नवाचार किसे कहते हैं?  नवाचार किसे कहते हैं, हम इसे कैसे पहचानते हैं और किस तरह दर्ज करते हैं? यह सवाल एक समस्या के रूप में मेरे दिमाग में आया जब मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से कस्बे डोंगरगाँव के बेसिक टीचर इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहा था। ये महज़ बारहवीं पास विद्यार्थी थे जो दो साल का डिप्लोमा कोर्स करके प्राइमरी स्कूल टीचर बनने की योग्यता पा लेते हैं। वे स्कूलों से शिक्षण का अभ्यास करके लौटे ही थे और काफी रोमांचित थे। एक लड़की ने बताया कि उसकी क्लास में दो विद्यार्थी बिलकुल चुप बैठे हुए थे और पढ़-लिख नहीं पा रहे थे। फिर उसने तय किया कि वह इन विद्यार्थियों के बारे में और जानने की व उन्हें कक्षा के भीतर सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश करेगी। उन बच्चों के घर जाने पर उसे किसी दुखद पारिवारिक स्थिति के बारे में पता चला। उनके घर जाने और उनकी मुसीबतों को देखने-समझने भर से उन विद्यार्थियों के साथ उसका सम्बन्ध बिलकुल बदल गया और वे विद्यार्थी अब क्लास में बढ़-चढ़कर भागीदारी करते हैं। शिक्षक-शिक्षण कोर्स के दौरान शिक्षण के अभ्यास में सूक्ष्म शिक्षण पद्धतियों की मदद से खास विषयवस्तुओं को पढ़ाने के लिए आदर्श पाठ-योजनाएँ बनानी पड़ती हैं। इस लड़की ने इस स्थापित साँचे को तोड़ दिया था और किसी पूर्वनियोजित योजना पर चलने की बजाय उसने दो बच्चों के सामने विशाल अटकाव बनी हुई एक बहुत ही खास समस्या का निवारण किया और इससे उसे बहुत सन्तोष मिला।
नवाचार किसे कहते हैं, हम इसे कैसे पहचानते हैं और किस तरह दर्ज करते हैं? यह सवाल एक समस्या के रूप में मेरे दिमाग में आया जब मैं छत्तीसगढ़ के एक छोटे-से कस्बे डोंगरगाँव के बेसिक टीचर इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों के साथ बातचीत कर रहा था। ये महज़ बारहवीं पास विद्यार्थी थे जो दो साल का डिप्लोमा कोर्स करके प्राइमरी स्कूल टीचर बनने की योग्यता पा लेते हैं। वे स्कूलों से शिक्षण का अभ्यास करके लौटे ही थे और काफी रोमांचित थे। एक लड़की ने बताया कि उसकी क्लास में दो विद्यार्थी बिलकुल चुप बैठे हुए थे और पढ़-लिख नहीं पा रहे थे। फिर उसने तय किया कि वह इन विद्यार्थियों के बारे में और जानने की व उन्हें कक्षा के भीतर सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने की कोशिश करेगी। उन बच्चों के घर जाने पर उसे किसी दुखद पारिवारिक स्थिति के बारे में पता चला। उनके घर जाने और उनकी मुसीबतों को देखने-समझने भर से उन विद्यार्थियों के साथ उसका सम्बन्ध बिलकुल बदल गया और वे विद्यार्थी अब क्लास में बढ़-चढ़कर भागीदारी करते हैं। शिक्षक-शिक्षण कोर्स के दौरान शिक्षण के अभ्यास में सूक्ष्म शिक्षण पद्धतियों की मदद से खास विषयवस्तुओं को पढ़ाने के लिए आदर्श पाठ-योजनाएँ बनानी पड़ती हैं। इस लड़की ने इस स्थापित साँचे को तोड़ दिया था और किसी पूर्वनियोजित योजना पर चलने की बजाय उसने दो बच्चों के सामने विशाल अटकाव बनी हुई एक बहुत ही खास समस्या का निवारण किया और इससे उसे बहुत सन्तोष मिला।
मुझे लगा कि शिक्षक-शिक्षण में हम जिस तरह का बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं उसके मूल में यही भावना तो है। बाद में मैंने उन सभी से स्कूल में किए गए कामों की रिपोर्ट और ‘डायरियाँ’ दिखाने को कहा। सबसे पहले मैंने इसी लड़की की रिपोर्ट देखी तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उसमें इस बात का कहीं भी ज़िक्र नहीं था जिसे लेकर वह इतनी उत्साहित थी। डायरी में पाठ के लक्ष्य, की गई गतिविधियों और बच्चों के सीखने के आकलन का एक सामान्य-सा विवरण था। इसलिए मैंने उससे पूछा कि इसमें वह सब क्यों नहीं लिखा जो उसने हमें बताया था। वह बोली, “हमारे शिक्षक ने हमसे कहा था कि अगर मैं वह सब लिख दूँगी तो मुझे नम्बर नहीं मिलेंगे और मुझे बस यही लिखना है कि मैंने अपने पाठ की योजना को कक्षा में कैसे लागू किया।” मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि अपने काम के दौरान बिलकुल साधारण शिक्षक भी लगातार नवाचार करता है लेकिन उसे मजबूर कर दिया जाता है कि वह उस नवाचार की स्मृति को मिटा दे या कम-से-कम उसे कहीं दर्ज न करे ताकि वह लोगों की स्मृति से भी ओझल हो जाए।
एक तरह से शिक्षकों या शैक्षिक प्रशासकों के रूप में हम सभी लगातार ‘नवाचार’ करते रहते हैं। दरअसल, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि हम उसे नहीं दोहराते जो पहले कर चुके होते हैं। हमारे विद्यार्थी बदलते रहते हैं, हम जिस ज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं, वह बदल जाता है। हमारी अपनी समझ और प्रवृत्ति भी बदलती रहती है। ये सारे बदलाव हमसे नवाचार कराते हैं। सीधी-सी बात है, नवाचार करने का मतलब है रचनात्मक होना, यानी कि मनुष्य होना।
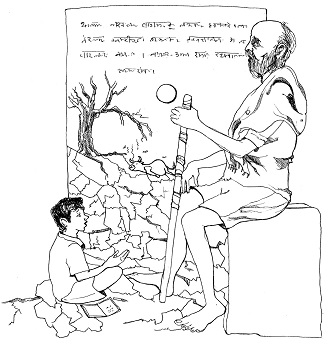 हालाँकि, हमारे द्वारा किए गए हर छोटे-से बदलाव या रचनात्मक समाधान को ‘नवाचार’ का दर्जा नहीं मिलता। किसी प्रयास को नवाचार कहलाने के लिए किन विशेषताओं की ज़रूरत होती है? सच कहूँ तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। पर मेरे पास इसका एक समाधान है जो युगों पुराने भाषा-बोली विवाद से उपजा है। यह चर्चा का एक पसन्दीदा विषय है और इससे आम तौर पर ‘भाषा’ की ये पहचान निकलकर आती है -- भाषा का एक व्याकरण होता है, उसकी एक लिपि होती है और इसके प्रभाव का क्षेत्र स्थानीय नहीं होता। अब हमारा बहुत सारा समय तो इन तीन मिथकों को तोड़ने और यह दिखाने में चला जाता है कि सभी भाषाओं या बोलियों का व्याकरण होता है (चाहे लिखित हो या अलिखित), कोई भी लिपि किसी एक भाषा विशेष की नहीं होती (किसी भी लिपि का उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जा सकता है) और किसी क्षेत्र में किसी भाषा का बोला जाना, उस भाषा की विशेषता न होकर एक सामाजिक प्रक्रिया का नतीजा होता है। अपनी इन ‘खासियतों’ से महरूम कर दिए जाने पर, ‘भाषा’ सिर्फ राजनैतिक प्रभावयुक्त बोली होती है। मेरा कहना है कि ठीक इसी तरह ‘नवाचारी’ शैक्षणिक व्यवहार भी राजनैतिक रूप से निर्धारित होता है।
हालाँकि, हमारे द्वारा किए गए हर छोटे-से बदलाव या रचनात्मक समाधान को ‘नवाचार’ का दर्जा नहीं मिलता। किसी प्रयास को नवाचार कहलाने के लिए किन विशेषताओं की ज़रूरत होती है? सच कहूँ तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है। पर मेरे पास इसका एक समाधान है जो युगों पुराने भाषा-बोली विवाद से उपजा है। यह चर्चा का एक पसन्दीदा विषय है और इससे आम तौर पर ‘भाषा’ की ये पहचान निकलकर आती है -- भाषा का एक व्याकरण होता है, उसकी एक लिपि होती है और इसके प्रभाव का क्षेत्र स्थानीय नहीं होता। अब हमारा बहुत सारा समय तो इन तीन मिथकों को तोड़ने और यह दिखाने में चला जाता है कि सभी भाषाओं या बोलियों का व्याकरण होता है (चाहे लिखित हो या अलिखित), कोई भी लिपि किसी एक भाषा विशेष की नहीं होती (किसी भी लिपि का उपयोग किसी भी भाषा को लिखने के लिए किया जा सकता है) और किसी क्षेत्र में किसी भाषा का बोला जाना, उस भाषा की विशेषता न होकर एक सामाजिक प्रक्रिया का नतीजा होता है। अपनी इन ‘खासियतों’ से महरूम कर दिए जाने पर, ‘भाषा’ सिर्फ राजनैतिक प्रभावयुक्त बोली होती है। मेरा कहना है कि ठीक इसी तरह ‘नवाचारी’ शैक्षणिक व्यवहार भी राजनैतिक रूप से निर्धारित होता है।
एक रचनात्मक शैक्षणिक विचार या व्यवहार तब ‘नवाचार’ बनता है जब वह एक खास साँचे में ढला हो और उसे एक सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति दी जाए जिसे इस पेशे से जुड़े वृहत समुदाय के साथ साझा किया जाए। तो इस तरह ‘व्याकरण, लिपि और क्षेत्र’ के तीन निर्णायक सिद्धान्त यहाँ भी लागू होते हैं।
हर शिक्षक और शैक्षिक प्रशासक को बदलती हकीकतों से लगातार दो-चार होना पड़ता है और रचनात्मक समाधान तलाशना पड़ते हैं। इसलिए वे हर वक्त नवाचार करते रहते हैं। लेकिन, इन्हें विरले ही नवाचार माना जाता है और आम तौर पर इन्हें, अगर बहुत खराब आकलन हुआ तो, शिक्षक की कामचोरी मान लिया जाता है, नहीं तो इनका ज़्यादा-से-ज़्यादा, शिक्षक की अच्छी कार्यविधि के रूप में ज़िक्र किया जाता है। बल्कि, शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले ज़्यादातर नवाचारों को या तो अपराध की तरह देखा जाता है या बिलकुल ही महत्वहीन करार दिया जाता है। ऐसा कभी-कभार ही होता है कि हम आलोचनात्मक या नकारात्मक हुए बगैर शिक्षकों द्वारा किए गए चुनावों के औचित्य को स्वीकार करें। न ही हम उनके इन चुनावों के पीछे के अर्थों और उद्देश्यों को समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षक और शैक्षिक प्रशासक भी, ढाँचागत और संस्थागत सीमाओं से बँधे रहकर उपलब्ध अत्यन्त सीमित माध्यमों एवं संसाधनों के आधार पर अपने चुनाव करते हैं और समाधान ढूँढ़ते हैं। फिर वैसी ही समस्याओं का सामना कर रहे शिक्षकों द्वारा जब इन चुनावों और समाधानों को व्यापक पैमाने पर अपनाया जाता है तो यह सब मिलकर एक प्रवृत्ति बना देते हैं। आम तौर पर शिक्षातंत्र द्वारा इन प्रवृत्तियों पर विलाप किया जाता है और इन्हें आदर्शों के साथ की गई अवांछित छेड़छाड़ मान लिया जाता है पर नवाचारों के रूप में इनकी प्रशंसा कभी नहीं की जाती। लेकिन इन ‘अतार्किक छेड़छाड़ों’ या नवाचारों में सफल होने की एक अजीब-सी क्षमता होती है, जबकि मान्य नवाचार आम तौर पर या तो असफल हो जाते हैं या उनका दुखदायी अन्त हो जाता है।
इसलिए मेरी यह बिनती है कि शिक्षक अपने रोज़मर्रा काम में जो चुनाव कर रहे हैं, उन्हें आलोचनात्मक रवैया अपनाए बिना दर्ज करना चाहिए और उनका अध्ययन होना चाहिए। एक प्रतिबद्ध पेशेवर की तरह मैं निश्चित ही अच्छे और अप्रिय नवाचार में भेद करता हूँ। मैं कुछ नवाचारों को मज़बूती देने के लिए काम करता हूँ, तो कुछ के विरुद्ध। लेकिन एक पेशेवर के रूप में मेरे लिए इस बात को देखना भी ज़रूरी है कि अन्य पेशेवर लोग क्यों अलग-अलग प्रकार के चुनाव करते हैं और इन सबका नतीजा क्या होता है।
स्मृति और विस्मृति
मैं जिस दूसरे मुद्दे को उठाना चाहता हूँ वह भी शिक्षक-शिक्षा पाठ्यक्रमों में सुधार करने के लिए विभिन्न एस.सी.ई.आर.टी. के साथ किए मेरे काम से निकला है। पाठ्यचर्या को तैयार करते वक्त इस बात पर ज़ोर दिया जाता कि शिक्षकों को प्रमुख नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रमों का अनुभव मिले। लेकिन, जब इस बात की विस्तृत चर्चा होने लगी कि किन कार्यक्रमों का अध्ययन किया जाना चाहिए, और उन पर सामग्री जुटाने की बात होने लगी तो हमारे बीच गतिरोध पैदा हो गया। असल में हमारे राज्य शिक्षा विभागों या एस.सी.ई.आर.टी. संस्थाओं को उनके ही राज्यों में चलाए गए प्रमुख नवाचारी कार्यक्रमों की कोई स्मृति नहीं है, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करना तो दूर की बात है। उदाहरण के लिए, जब हम लोग राजस्थान एस.आई.ई.आर.टी. के साथ काम कर रहे थे तो हमने पाया कि उनके पास शिक्षाकर्मी परियोजना की, या फिर लोक जुम्बिश परियोजना की भी लगभग कोई सामग्री नहीं थी। कुछ लोग ज़रूर ऐसे थे जिन्हें इन परियोजनाओं के बारे में थोड़ा-बहुत पता था पर इनके कोई दस्तावेज़ या कोई साहित्य मौजूद नहीं था। इन कार्यक्रमों से अनुभव और नवाचारी व्यवहारों की जो विशाल सम्पदा पैदा हुई थी, वह लगता है पूरी तरह से खो दी गई है। यह खास तौर से आश्चर्यजनक था क्योंकि ये सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र के ऐसे कार्यक्रम थे जिनका अच्छा-खासा दस्तावेज़ीकरण हुआ था और इन पर बहुत-से स्वतंत्र शैक्षिक अध्ययन किए गए थे। बल्कि, लोक जुम्बिश ने तो कार्यक्रम के शोध और दस्तावेज़ीकरण के लिए संधान नाम के एनजीओ में एक स्वतंत्र रिसर्च विंग भी स्थापित कर दिया था। पता चला कि जब सरकार ने इस कार्यक्रम को बन्द करने का निश्चय किया तो उसने संधान के पास मौजूद कार्यक्रम से जुड़े सभी कागज़ों और दस्तावेज़ों को जब्त कर लिया और उन्हें किसी अज्ञात सरकारी गोदाम में पटक दिया। तो हमारे पास अब ले-देकर कुछेक पुस्तकालयों में इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ प्रकाशन रह गए हैं और इससे जुड़े लोग हैं। यह ज़रूर है कि अगर कोई प्रभावशाली शोधकर्ता इस कार्यक्रम के इतिहास को खंगालने का निश्चय कर ले तो हो सकता है सरकार के पास मौजूद कुछ दस्तावेज़ों को देखा जा सके। लेकिन हकीकत तो यही है कि राजस्थान के स्कूली शिक्षा तंत्र से इस कार्यक्रम की स्मृति को मिटा दिया गया है।
मैं इससे भी ज़्यादा दुखद एक उदाहरण देता हूँ, नई तालीम का, जो निश्चित रूप से भारतीय शैक्षिक इतिहास के सबसे प्रभावशाली नवाचारों में से एक था, और इसे देशभर में 1945 से लेकर कम-से-कम 1965 तक आज़माया गया। यहाँ भी हम कार्यक्रम के वास्तविक अनुभवों को पूरी तरह से भूल चुके हैं। इस कार्यक्रम से भी बड़ी मात्रा में साहित्य तैयार हुआ था और आधिकारिक रिकॉर्ड व पत्रिकाएँ तैयार हुई थीं। लेकिन जब हम इनके बारे में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास या तो बस इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले गाँधी द्वारा कही गई बातें होती हैं या बहुत हुआ तो कुछ सरकारी रिपोर्ट मिल जाती हैं। नई तालीम पर जितना भी लिखा जाता है उसमें ज़्यादातर इस कार्यक्रम की अवधारणा पर ही बात की जाती है बजाय इस चर्चा के कि विभिन्न राज्यों में ज़मीनी स्तर पर इस कार्यक्रम ने क्या काम किए। जबकि अपने समय में इस कार्यक्रम पर खूब अध्ययन किए गए थे और खूब लिखा गया था। लेकिन सरकार के शिक्षा विभागों को उनकी तनिक भी याद नहीं है। और भी दुखद बात यह है कि सेवाग्राम तक में इस कार्यक्रम के कोई दस्तावेज़ नहीं बचे हैं जो इसका गढ़ हुआ करता था।
 हालाँकि, आज भी दूर-दराज़ के इलाकों में स्थित पुस्तकालयों में हमें इस कार्यक्रम से निकले बेहद दिलचस्प प्रकाशन देखने को मिल सकते हैं जिनमें समस्याओं को समझा गया है, अनुभवों की चर्चा की गई है और विचारों को साझा किया गया है। इन्हें तैयार करने में देश के दूर-दराज़ हिस्सों में रहने वाले शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों ने बड़े उत्साह से अपना योगदान दिया था। हो सकता है कि कुछ संस्थाओं के पास इस कार्यक्रम के कामों से जुड़े हुए पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध हों। लेकिन ये सभी दस्तावेज़, चाहे छपे हुए हों या फिर सस्ते कागज़ पर हाथ से लिखे गए, अब पुस्तकालयों के इस्तेमाल न होने वाले कोनों में या कचरों के ढेर पर सड़-गल रहे हैं और दीमकों का आहार बन रहे हैं।
हालाँकि, आज भी दूर-दराज़ के इलाकों में स्थित पुस्तकालयों में हमें इस कार्यक्रम से निकले बेहद दिलचस्प प्रकाशन देखने को मिल सकते हैं जिनमें समस्याओं को समझा गया है, अनुभवों की चर्चा की गई है और विचारों को साझा किया गया है। इन्हें तैयार करने में देश के दूर-दराज़ हिस्सों में रहने वाले शिक्षकों और शिक्षक-प्रशिक्षकों ने बड़े उत्साह से अपना योगदान दिया था। हो सकता है कि कुछ संस्थाओं के पास इस कार्यक्रम के कामों से जुड़े हुए पुराने रिकॉर्ड उपलब्ध हों। लेकिन ये सभी दस्तावेज़, चाहे छपे हुए हों या फिर सस्ते कागज़ पर हाथ से लिखे गए, अब पुस्तकालयों के इस्तेमाल न होने वाले कोनों में या कचरों के ढेर पर सड़-गल रहे हैं और दीमकों का आहार बन रहे हैं।
यह हमारी खुशकिस्मती है कि गुजरात विद्यापीठ ने बची-खुची गाँधीवादी संस्थाओं से इस तरह की सामग्री को इकट्ठा किया है और उसे डिजिटल रूप में परिवर्तित कर दिया है। मैंने इस सामग्री को देखा तो नहीं है पर उम्मीद करता हूँ कि यह काफी महत्वपूर्ण होगी।
इस पूरे मसले में एक-दूसरे से जुड़े हुए तीन मुद्दे हैं: पहला है शिक्षा तंत्र की अक्षमता कि वह अपने ही नवाचारी कार्यक्रमों की स्मृति को बनाए नहीं रखता और उनकी नींव पर नए निर्माण नहीं करता। दूसरी, हमारी सामूहिक अक्षमता कि हम इन कार्यक्रमों से निकले दस्तावेज़ों और साहित्य को सम्भालकर नहीं रखते और उनका अध्ययन नहीं करते। और आखिरी बात यह कि इन कार्यक्रमों पर बहुत ही कम आलोचनात्मक शैक्षिक अध्ययन हुए हैं। आम तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़े जो प्रकाशन हमारे पास होते हैं वे इन कार्यक्रमों की आत्म-प्रशंसात्मक रिपोर्टें होती हैं जो जटिल यथार्थ की बहुत ही सीमित झलक देती हैं।
किसी कार्यक्रम के रिकॉर्ड रखना, उनका प्रकाशन और छपाई उसकी स्मृति को बनाने के लिए तो ज़रूरी हो सकते हैं लेकिन ये पर्याप्त नहीं होते, और न ही इस बात का भरोसा होते हैं कि वह कार्यक्रम व्यवस्थागत स्मृति का हिस्सा बन जाएगा -- कुछ ऐसा जो नए कार्यक्रमों को हाथ में लेते समय हमारा मार्गदर्शन कर सके।
नतीजा यह होता है कि जब भी हम किसी नए नवाचारी कार्यक्रम की कल्पना करते हैं तो हम इस तरह के पिछले कार्यक्रमों की सीखों और सफलताओं पर आगे चलने की बजाय बिलकुल शुरू से शुरू करते हैं। दुर्भाग्य से, मेरे पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, पर ये बातें मैं आपके सामने इस आशा से रख रहा हूँ ताकि हम कम-से-कम इनकी बेहतर समझ तो बना सकें।
 इस लेख को निराशाजनक अन्त न देते हुए मैं आपको ‘स्मृति निर्माण’ के दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है, साकड़ नामक एक दूर-दराज़ के गाँव में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए खोले गए आधारशिला नाम के एक सादे-से रिहाइशी स्कूल का। लगभग 17 साल पहले गाँव में भयंकर सूखा पड़ा और स्कूल द्वारा बच्चों से कहा गया कि वे गाँव के बड़े-बूढ़ों से सूखे और भुखमरी के बारे में पता करें और जानें कि लोग इनसे कैसे निपटते हैं। बड़े-बूढ़ों ने जो बताया उससे बच्चों की कॉपियाँ भर गईं। फिर इस सब के आधार पर बच्चों ने स्कूल के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। जब अपनी एक यात्रा के दौरान मुझे यह रिपोर्ट देखने को मिली तो मुझे लगा कि इसे न सिर्फ सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने और सीखने सम्बन्धी दस्तावेज़ के रूप में प्रकाशित करना चाहिए बल्कि इसलिए भी प्रकाशित करना चाहिए क्योंकि इसमें इस बात से जुड़ी बहुत अनोखी बातें दर्ज थीं कि हाशियाग्रस्त समुदाय सूखे और भुखमरी जैसी आपदाओं से कैसे निपटते हैं। उस दौरान इस गाँव के लोगों ने क्या खाया, गाँव के पशु-पक्षियों और पौधों का क्या हुआ, अकाल व भुखमरी से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान, खुद को ज़िन्दा रखने के लिए किस तरह लोग पलायन, डकैती आदि करने लगे वगैरह वगैरह। इस रचना की पाण्डुलिपि कई सालों तक एकलव्य के पास पड़ी रही क्योंकि हमें ऐसा सही व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इस स्कूल के साथ मिलकर किताब की रूपरेखा तैयार करता, उसके चित्र तैयार करता। लेकिन आखिरकार, कुछ साल पहले यह किताब प्रकाशित हो गई।
इस लेख को निराशाजनक अन्त न देते हुए मैं आपको ‘स्मृति निर्माण’ के दो उदाहरण देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण है, साकड़ नामक एक दूर-दराज़ के गाँव में नर्मदा बचाओ आन्दोलन के कार्यकर्ताओं के बच्चों के लिए खोले गए आधारशिला नाम के एक सादे-से रिहाइशी स्कूल का। लगभग 17 साल पहले गाँव में भयंकर सूखा पड़ा और स्कूल द्वारा बच्चों से कहा गया कि वे गाँव के बड़े-बूढ़ों से सूखे और भुखमरी के बारे में पता करें और जानें कि लोग इनसे कैसे निपटते हैं। बड़े-बूढ़ों ने जो बताया उससे बच्चों की कॉपियाँ भर गईं। फिर इस सब के आधार पर बच्चों ने स्कूल के लिए एक रिपोर्ट तैयार की। जब अपनी एक यात्रा के दौरान मुझे यह रिपोर्ट देखने को मिली तो मुझे लगा कि इसे न सिर्फ सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने और सीखने सम्बन्धी दस्तावेज़ के रूप में प्रकाशित करना चाहिए बल्कि इसलिए भी प्रकाशित करना चाहिए क्योंकि इसमें इस बात से जुड़ी बहुत अनोखी बातें दर्ज थीं कि हाशियाग्रस्त समुदाय सूखे और भुखमरी जैसी आपदाओं से कैसे निपटते हैं। उस दौरान इस गाँव के लोगों ने क्या खाया, गाँव के पशु-पक्षियों और पौधों का क्या हुआ, अकाल व भुखमरी से किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान, खुद को ज़िन्दा रखने के लिए किस तरह लोग पलायन, डकैती आदि करने लगे वगैरह वगैरह। इस रचना की पाण्डुलिपि कई सालों तक एकलव्य के पास पड़ी रही क्योंकि हमें ऐसा सही व्यक्ति नहीं मिल रहा था जो इस स्कूल के साथ मिलकर किताब की रूपरेखा तैयार करता, उसके चित्र तैयार करता। लेकिन आखिरकार, कुछ साल पहले यह किताब प्रकाशित हो गई।
मेरे सामने बड़ा सवाल यह है कि इस तरह का काम सार्वजनिक स्मृति में कैसे आता है और सराहना करने वाले दोस्तों के दायरे से आगे बढ़कर शैक्षिक इतिहास का हिस्सा कैसे बनता है?
मैं इस सवाल पर वापस आऊँगा, लेकिन पहले हम इसी तरह के एक अन्य प्रयोग के बारे में बनाया गया एक छोटा-सा वीडियो देख लें (यंग हिस्टॉरियंस -- ईएसई और डीएसईआरटी द्वारा बनाई गई एक फिल्म, भाग-1)। इस प्रयोग का दस्तावेज़ीकरण सरकारी विभाग द्वारा की गई पहल पर किया गया।
इस सीरियल में एक ग्रामीण स्कूल के शिक्षक द्वारा अपने विद्यार्थियों को नए तरीके से इतिहास की खोज व अध्ययन सिखाने के प्रयोग दर्ज हैं।
स्मृति मानव समुदायों का साझा काम है, किताबों या कम्प्यूटरों का नहीं। इसलिए याद रखना और भुला देना, दोनों ही मनुष्य की सजग क्रियाएँ हैं। और यह अन्तत: हमारे चुनाव होते हैं, बल्कि सामाजिक समूहों के चुनाव होते हैं जिनसे ये बातें तय होती हैं। यह हमारा सजग प्रयास है कि कुछ यादों को ज़िन्दा रखा जाए, उनसे सीखा जाए, उन्हें और लोगों तक फैलाया जाए ताकि उस समूह को विस्तृत और समावेशी बनाया जा सके जिसके लिए नवाचारों की स्मृतियों को जीवित रखना सार्थक हो। किसी स्मृति को साझा करने वाले ऐसे समूहों का विस्तार करना, जो उस स्मृति से सीखते हुए, उसका उपयोग करते हुए उसे जीवित रखते हैं, एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें संवाद की आवश्यकता तो रहती ही है, साथ ही उस स्मृति में आलोचनात्मकता और विविधता लाने की ज़रूरत भी होती है। अगर हम किसी नवाचार के एक खास रूप को ही पकड़कर रखने पर आमादा रहेंगे तो फिर यह जोखिम ज़रूर रहेगा कि वह नवाचार सिर्फ एक छोटे-से समूह के दायरे में सिमटकर रह जाए और दूसरों को यह मौका मिल जाए कि वे उसे विस्मृत कर सकें। यहीं पर नवाचारों का तटस्थ शैक्षिक अध्ययन महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमें मौका मिलता है कि हम नवाचारों की पहुँच को उसी तरह विस्तृत कर सकें जिस तरह प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री के चार सिद्धान्तों को आधार बनाकर अन्य लोगों के साथ निरन्तर संवाद करने के प्रयास विस्तृत होते हैं, जैसा कि अम्बेडकर ने बुद्ध की शिक्षाओं को याद करते हुए कहा था।
सी.एन. सुब्रह्मण्यम: एकलव्य के सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं।
अँग्रेज़ी से अनुवाद: भरत त्रिपाठी: एकलव्य, भोपाल के प्रकाशन समूह के साथ कार्यरत हैं।
सभी चित्र: निहारिका शिनॉय: चित्रकार, लेखक और अनुवादक। WhatParentsAsk.com के साथ क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में जुड़ी हुई हैं। बैंग्लोर में रहती हैं।
यह लेख सी.एन. सुब्रह्मण्यम द्वारा सेंटर फॉर हिस्टॉरिकल स्टडीज़, जवाहरलाल नेह डिग्री विश्वविद्यालय, दिल्ली में दिए गए वक्तव्य पर आधारित है।

