भवानीप्रसाद मिश्र
अनुपम मिश्र
 संस्मरण
संस्मरण
थोड़ा - बहुत लिखना - पढ़ना पिताजी से ही सीखा पर उन पर कभी कुछ लिखा नहीं। उन्हें गए आज 27 बरस हो रहे हैं, लेकिन उनके बारे में कभी 27 शब्द भी नहीं लिखे।
कारण कई थे। पहला तो वे खुद थे। कुछ के लिए वे ज़रूर ‘गीतफरोश’ रहे होंगे, पर हमारे लिए तो वे बस पिता थे। हर पिता पर उसके बेटे-बेटी कुछ लिखें -- यह उन्हें पसन्द नहीं था। कुल मिलाकर हम सबके मन में भी यह बात ठीक उतर गई थी। मन्ना ने एकाध बार बहुत ही मज़े-मज़े में हमें बताया था कि कोई भी पिता अमर नहीं होता। पिता के मरते ही उसके बेटे-बेटी उनकी याद में कोई स्मारिका छाप बैठें, खुद लेख लिखें, दूसरों से लिखाते फिरें, उनकी स्मृति को स्थायी रूप देने हेतु उनके नाम से कोई संस्था, संगठन खड़ा कर दें -- यह सब बिलकुल ज़रूरी नहीं होता। उनकी मृत्यु के बाद हमने इस बात को पूरी तरह निभाया, न खुद लिखा, न लिखवाया।
दूसरा कारण उनकी एक कविता थी -- ‘कलम अपनी साध, मन की बात बिलकुल ठीक कह एकाध’। तो मन की बात ठीक एकाध कभी सूझी नहीं। सूझी भी तो मन्ना की शर्त ‘तेरी भर न हो’ लागू करने के बाद कभी कुछ ऐसा बचता नहीं था लिखने लायक।
हम सब उन्हें मन्ना कहते थे। भाषा को बिगाड़ने का कुछ पाप जिन संबोधनों से लगता हो, वैसे संबोधन पिता के लिए तब प्रचलित नहीं हुए थे। लेकिन तब के नाम बाबूजी, पिताजी, बाबा आदि से भी हम और वे बच गए थे। खूब बड़े भरे-पूरे परिवार में मँझले भाई थे। पिताजी के बड़े भाई उन्हें प्यार से सिर्फ ‘मँझले’ कहते और फिर दादा-दादी से लेकर सभी छोटे बहन-भाई, यानी हमारे चाचा, बुआ आदि भी उन्हें आदर से ‘मँझले भैया’ ही कहने लगे थे। मुझसे बड़े दो भाई सन् 1942 में जब पिताजी को पुकारने लायक उम्र में आ रहे थे कि वे जेल चले गए। जेल में लिखी उनकी कविता ‘घर की याद’ में इस भरे-पूरे परिवार का, उसके स्नेह का, आँखें गीली करने लायक वर्णन है। दो-तीन बरस बाद जब वे जेल से छूटकर लौटने वाले थे, तब ये दोनों बेटे अपने पिता को किस नाम से पुकारेंगे -- इस बारे में नरसिंहपुर (मध्य प्रदेश) के घर में बुआओं, चाचाओं में कुछ बहस चली थी। पर जब पिता सामने आकर अचानक खड़े हुए, संबोधन कूद के पार कर लिए थे और सहज ही ‘मँझले भैया’ कह कर उनकी तरफ दौड़ पड़े थे। दोनों बच्चों को कुछ सलाह, निर्देश भी दिए गए थे। बेटों के लिए भी वे ‘मँझले भैया’ बने रहे।
फिर जन्म हुआ मुझसे बड़ी बहन नंदिता का। जीजी से ‘मँझले भैया’ कहते बना नहीं, उनने उसे अपनी सुविधा के लिए ‘मन्ने भैया’ किया। फिर मन्ने भैया और थोड़ा घिसकर चमकते-चमकते ‘मन्ने’ और अन्त में ‘मन्ना’ हो गया। जब मेरा जन्म 1948 में वर्धा में हुआ तब तक पिताजी जगत मन्ना बन चुके थे -- सिर्फ हमारे ही नहीं, आस-पड़ोस और बाहर के छोटे-से लेकिन आत्मीय जगत के।
बचपन की यादें कोई खास नहीं। शायद घटनाएँ भी खास नहीं रही होंगी -- उस दौर में एक साधारण पिता के जो सम्बन्ध साधारण तौर पर अपने बच्चों से रहते हैं, ठीक वैसे ही सम्बन्ध हमारे परिवार में रहे होंगे।
मेरे जन्म के बाद हम सब वर्धा से हैदराबाद आ गए थे। वे दिन हमारे लिए यह सब जानने-समझने के थे नहीं कि मन्ना कहाँ क्या काम करते हैं। पर एक बार वे घर से कुछ ज़्यादा दिनों के लिए बाहर कहीं चले गए थे। तब शायद मैं पहली कक्षा में पढ़ता था। वे तब मद्रास गए थे। लौटे तो उनके साथ एक सुन्दर चमकीला चाकू आया था। मन्ना को सब्ज़ी काटने का खूब शौक था। सब्ज़ी खरीदने का भी यह शौक कभी-कभी अम्मा की परेशानी में बदल जाता। ढेर-के-ढेर उठा लाते क्योंकि बेचने वाली का बच्चा छोटा था, वह सब कुछ बेच जल्दी घर लौट सकती थी। बचपन में हमने उन्हें न तो कविता लिखते देखा, न पढ़ते-सुनाते। मद्रास के उस स्टील के चाकू से खूब मज़ा लेकर सब्ज़ी काटते थे -- इसकी हमें याद बराबर है।
यह दौर था जब वे मद्रास में ए.वी.एम. फिल्म कम्पनी के लिए कुछ गीत और संवाद लिखने गए थे। सब्ज़ी खरीदने में बहुत ही प्रेम से भाव-ताव करने वाले मन्ना ए.वी.एम. के मालिक चेट्टियार साहब से अपने गीत बेचते समय कोई भाव-ताव नहीं कर पाए थे। गीत बेचने की इस उतावली में उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि कुछ पैसा जुटा लेना भर था। बड़े परिवार में दो-तीन बुआओं का विवाह करना था। रजतपट के उस प्रसंग में उन पर कुछ कीचड़ भी उछला होगा। उसी दौर में उन्होंने ‘गीतफरोश’ कविता लिखी थी। हमने तब घर में रजतपट के चमकीले किस्से कभी सुने नहीं। किस्से सुने ए.वी.एम. के होटल के जहाँ रोज़ इतनी सब्ज़ी कटती थी कि अच्छे-से-अच्छे चाकू कुछ ही दिनों में घिस जाते थे, फिर फिंका जाते थे। रजतपट की सारी चमक हमारे घर में इसी चाकू में समा कर आई थी मद्रास से।
चेट्टियार साहब से किसी विवाद के बाद वे गीत बेचने की दुकान बढ़ा कर घर लौट आए। ‘गीतफरोश’ में किसिम-किसिम के गीतों में एक गीत ‘दुकान से घर जाने’ का भी है। शायद जब वे तरह-तरह के गीत बेच रहे थे, तब उनके मन में घर आने का गीत ‘ग्राहक’ की मर्ज़ी से बँधा नहीं था।
ए.वी.एम. की वे फिल्में, जिनमें मन्ना ने गीत और संवाद लिखे थे, डिब्बे में बन्द नहीं हुईं। वे हैदराबाद के सिनेमाघरों में भी आई होंगी, पर मन्ना ने उन्हें अपनी उपलब्धि नहीं माना। हम लोगों को, अम्मा को सज-धज कर उन्हें दिखा लाने का कभी प्रस्ताव नहीं रखा। शायद उनके लिए ये गीत ‘मरण’ के थे, फिल्मी दुनिया में रमने के नहीं, मरने के गीत थे।
साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए मन्ना का वह दौर प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका ‘कल्पना’ का दौर था। पर हम बच्चों की कल्पना कुछ और ही थी। घर में कभी शराब नहीं आई पर हैदराबाद में हम शराब के ही घर में, मुहल्ले में रहते थे। मुहल्ले का नाम था, टकेरवाड़ी। चारों तरफ अवैध शराब बनती थी। उसे चुआने की बड़ी-बड़ी नादें यहाँ-वहाँ रखी रहती थीं। यों हमारे मकान मालिक जिन्हें हम बच्चे शीतल भैया मानते थे, खुद इस धन्धे से एकदम अलग थे पर चारों तरफ इसी धन्धे में लगे लोग छापा पड़ने के डर से कभी-कभी कुछ सामान, नाद आदि हमारे घर के पिछवाड़े में पटक जाते। चार-पाँच बरस के हम भाई-बहनों की क्या ऊँचाई रही होगी तब। हम इन नादों में छिपकर तब की ताज़ा कहानी ‘अली बाबा और चालीस चोर’ का नाटक खेल डालते थे।
कभी-कभी मन्ना हमें बदरी चाचा (श्री बदरीविशाल पित्ती) के घर ले जाते। घर क्या, विशाल महल था। शतरंज के दो बित्ते के बोर्ड पर सफेद-काले रंग का जो सुन्दर मेल हमने कभी अपने घर में देखा, वह यहाँ बदरी चाचा के पूरे घर में, आँगन में, कमरों के फर्श में - सभी जगह पूरी भव्यता से फैला मिलता। बदरी चाचा के घर ऐसे मौकों पर बड़े-बड़े लोग जुटते थे, पर हम उन सबको उस रूप में पहचानते नहीं थे। बदरीचाचा सचमुच विशाल थे हम सब के लिए। कभी-कभी वे हम सबको हैदराबाद से थोड़ी दूर बसे शिवरामपल्ली गाँव ले जाते। वहाँ तब विनोबा का भूदान आन्दोलन शु डिग्री हुआ था। बदरी चाचा अच्छे फोटोग्राफर भी थे। उस दौर में उनके द्वारा खींचे गए चित्र आज भी हमारे मन पर ज्यों-के-त्यों अंकित हैं -- कागज़ वाले प्रिंट ज़रूर कुछ पीले-भूरे और धुँधले पड़ गए हैं।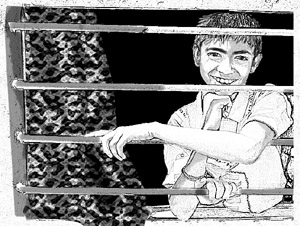 मन्ना कविता लिखते थे, पढ़ने भी लगे थे, शायद रेडियो पर भी। लेकिन हमें घर में कभी इसकी जानकारी मिली हो -- ऐसा याद नहीं आता। तब तक घर में रेडियो नहीं आया था। हैदराबाद रेडियो स्टेशन से हर इतवार सुबह बच्चों का एक कार्यक्रम प्रसारित होता था। हम एकाध बार वहाँ मन्ना के साथ गए थे। ऐसे ही किसी इतवार को नन्दी जीजी ने लकड़हारे की कहानी माइक के सामने सुना दी थी। जिस दिन उसे प्रसारित होना था, उसके एक दिन पहले मन्ना एक रेडियो खरीद लाए थे। रेडियो सेट मन्ना की कविता के लिए नहीं, जीजी की कहानी सुनाने के लिए घर में आया था -- इसे आज रेडियो में ही काम करने वाली नंदिता मिश्र भूली नहीं हैं।
मन्ना कविता लिखते थे, पढ़ने भी लगे थे, शायद रेडियो पर भी। लेकिन हमें घर में कभी इसकी जानकारी मिली हो -- ऐसा याद नहीं आता। तब तक घर में रेडियो नहीं आया था। हैदराबाद रेडियो स्टेशन से हर इतवार सुबह बच्चों का एक कार्यक्रम प्रसारित होता था। हम एकाध बार वहाँ मन्ना के साथ गए थे। ऐसे ही किसी इतवार को नन्दी जीजी ने लकड़हारे की कहानी माइक के सामने सुना दी थी। जिस दिन उसे प्रसारित होना था, उसके एक दिन पहले मन्ना एक रेडियो खरीद लाए थे। रेडियो सेट मन्ना की कविता के लिए नहीं, जीजी की कहानी सुनाने के लिए घर में आया था -- इसे आज रेडियो में ही काम करने वाली नंदिता मिश्र भूली नहीं हैं।
हैदराबाद से मन्ना आकाशवाणी के बम्बई केन्द्र में आ गए थे। तब मैं तीसरी कक्षा में भर्ती किया गया था। उस स्कूल में हमें दूसरों से, अध्यापकों के व्यवहार से पता चला था कि हमारे पिताजी को घर से बाहर के लोग भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वे कविताएँ लिखते हैं। हमारे मन्ना कवि हैं!
कवि कालदर्शी होता है? हमें नहीं मालूम था। कल क्या होगा बच्चों का, उनकी पढ़ाई-लिखाई कैसी करनी है -- बहुत ही बड़े माने गए ऐसे प्रश्न हमारे कवि पिता ने कभी सोचे नहीं होंगे। जब एक शाम मैं और नन्दी स्कूल से घर लौटे थे तो मन्ना ने हमें बताया कि अगले दिन हम सब बम्बई से बेमेतरा जाएँगे। बड़े भैया के पास। मन्ना के बड़े भैया मध्य प्रदेश के दुर्ग ज़िले की एक छोटी-सी तहसील बेमेतरा में तब तहसीलदार थे। हम सब बेमेतरा जा पहुँचे। दो-चार दिन बाद पता चला कि मन्ना और अम्मा वापस बम्बई लौट रहे हैं और अब हम यहीं बेमेतरा में बड़े भैया के पास रहकर पढ़ेंगे। हैदराबाद में एक बार सीढ़ियों से गिरने पर काफी चोट लगने से मैं खूब रोया था। तब के बाद अब की याद है -- बेमेतरा में खूब रोया, उनके साथ वापस बम्बई लौटने को। आँखें तो उनकी भी गीली हुई थीं पर हम वहीं रह गए, मन्ना-अम्मा लौट गए। ताऊजी यानी बड़े भैया का प्यार मन्ना से बड़ा ही निकला। यह तो हमें बहुत बाद में पता चला कि बड़े पिताजी के छह में से पाँच बेटे बड़े होकर कॉलेज हॉस्टल आदि में चले गए थे और उन्हें अपना घर सूना लगने लगा था, इसलिए उस सूने घर में रौनक लाने के लिए मँझले भाई मन्ना ने हम दोनों को उन्हें सौंप दिया था।
बम्बई से मन्ना दिल्ली आकाशवाणी आ गए। तब हम भी एक गर्मी में बेमेतरा से शायद चौथी-पाँचवीं की पढ़ाई पूरी कर दिल्ली बुला लिए गए। हैदराबाद, बम्बई की यादें धुँधली-सी ही थीं। बेमेतरा छोटा कस्बा था और बड़े भैया सरकार के बड़े अधिकारी थे, इसलिए बाज़ार आना-जाना, खरीददारी, डबलरोटी -- ऐसे विचित्र अनुभवों से हम गुज़रे नहीं थे। दिल्ली आने पर मन्ना के साथ घूमने, खुद चीज़ेें खरीदने के अनुभव भी जुड़े। एक साधारण, ठीक माने गए स्कूल रामजस में उन्होंने मुझे भरती किया। सातवीं-आठवीं-नौवीं में विज्ञान में नम्बर थे। इसी बीच उन्हें सरकारी मकान किसी और मुहल्ले में मिल गया। शुभचिन्तकों के समझाने पर भी मन्ना ने मेरा स्कूल फिर बदल दिया -- नए मुहल्ले सरोजनी नगर में टेंट में चलने वाले एक छोटे-से सरकारी स्कूल में। यह घर के ठीक पीछे था। पैदल दूरी। ‘बच्चा नाहक दिल्ली की ठण्ड-गर्मी में आठ-दस मील दूर के स्कूल में बसों में भागता फिरे’ यह उन्हें पसन्द नहीं था। यहाँ विज्ञान भी नहीं था। मैं कला की कक्षा में बैठा। मुझे खुद भी तब पता नहीं था कि विज्ञान मिलने-न-मिलने से जीवन में क्या खोते हैं-पाते हैं। यहीं नौवीं में हिन्दी पढ़ाते समय जब किसी एक सहपाठी ने हमारे हिन्दी के शिक्षक को बताया कि मैं भवानीप्रसाद मिश्र का बेटा हूँ तो उन्होंने उसे ‘झूठ बोलते हो’ कह दिया था। बाद में उनने मुझसे भी लगभग उसी तेज़ आवाज़ में पिता का नाम पूछा था। घर का पता पूछा था, फिर किसी शाम वे घर भी आए। अपनी कविताएँ भी मन्ना को सुनाईं। मन्ना ने भी कुछ सुनाया था। उस टेंट वाले स्कूल में ऐसे कवि का बेटा? मन्ना की प्रसिद्धि हमें इन्हीं मापदण्डों, प्रसंगों से जानने मिली थी।
 श्री मोहनलाल वाजपेयी यानी लालजी कक्कू मन्ना के पुराने मित्र थे। मन्ना ने उनके नाम एक पूरी पत्रनुमा कविता लिखी भी। बड़ा भव्य व्यक्तित्व। शान्तिनिकेतन में हिन्दी पढ़ाते थे। शायद सन् 1957 में वे रोम विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना करने बुलाए गए थे। वहाँ से जब वे दिल्ली आए, एक बार तो एक बहुत ही सुन्दर छोटा-सा टेप रिकॉर्डर लाए थे मन्ना के लिए। नाम था जैलेसी। जैलेसी यानी ईर्ष्या। उसमें छोटे स्पूल लगते थे। उन दिनों कैसेट वाले टेप चले नहीं थे। शहर का न सही, शायद मुहल्ले का तो यह पहला टेप रिकॉर्डर रहा ही होगा! इसका हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। विज्ञान के आगे मैंने तो माथा ही टेक दिया था। क्या गज़ब की मशीन थी। हर किसी की आवाज़ कैद कर ले, फिर उसे ज्यों-का-त्यों वापस सुना दे! शायद लालजी कक्कू ने यह यंत्र इसलिए दिया था कि मन्ना इस पर कभी-कभी अपना काव्य पाठ रिकॉर्ड करेंगे। पर वैसा कभी हो नहीं पाया। एक तो ऐसे यंत्र चलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, और फिर अपनी कविता खुद बटन दबाकर रिकॉर्ड करना, उसे खुद सुनना, दूसरों को सुनाना -- उन्हें पसन्द नहीं था। बाद में हमारे एक बड़े भाई बम्बई से वास्तुशास्त्र पढ़कर जब दिल्ली आए तो जैलेसी पर मुकेश, किशोर कुमार और लता के गाने ज़रूर जम गए थे। आज भी हमारे घर में मन्ना की एक भी कविता का पाठ रिकॉर्ड नहीं है। कभी-कभी नितान्त अपरिचित परिवार में परिचय होने के बाद सन्नाटा, गीतफरोश, घर की याद, सतपुड़ा के घने जंगल आदि कविताओं के पाठ की रिकॉर्डिंग हमें सुनने मिल जाती हैं। ये कविताएँ उन शहरों में मन्ना ने पढ़ी होंगी। वहीं वे रिकॉर्ड कर ली गईं। हमें ऐसे मौकों पर लालजी कक्कू के जैलेसी की याद ज़रूर आ जाती है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
श्री मोहनलाल वाजपेयी यानी लालजी कक्कू मन्ना के पुराने मित्र थे। मन्ना ने उनके नाम एक पूरी पत्रनुमा कविता लिखी भी। बड़ा भव्य व्यक्तित्व। शान्तिनिकेतन में हिन्दी पढ़ाते थे। शायद सन् 1957 में वे रोम विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग की स्थापना करने बुलाए गए थे। वहाँ से जब वे दिल्ली आए, एक बार तो एक बहुत ही सुन्दर छोटा-सा टेप रिकॉर्डर लाए थे मन्ना के लिए। नाम था जैलेसी। जैलेसी यानी ईर्ष्या। उसमें छोटे स्पूल लगते थे। उन दिनों कैसेट वाले टेप चले नहीं थे। शहर का न सही, शायद मुहल्ले का तो यह पहला टेप रिकॉर्डर रहा ही होगा! इसका हमारे मन पर बहुत गहरा असर पड़ा था। विज्ञान के आगे मैंने तो माथा ही टेक दिया था। क्या गज़ब की मशीन थी। हर किसी की आवाज़ कैद कर ले, फिर उसे ज्यों-का-त्यों वापस सुना दे! शायद लालजी कक्कू ने यह यंत्र इसलिए दिया था कि मन्ना इस पर कभी-कभी अपना काव्य पाठ रिकॉर्ड करेंगे। पर वैसा कभी हो नहीं पाया। एक तो ऐसे यंत्र चलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं थी, और फिर अपनी कविता खुद बटन दबाकर रिकॉर्ड करना, उसे खुद सुनना, दूसरों को सुनाना -- उन्हें पसन्द नहीं था। बाद में हमारे एक बड़े भाई बम्बई से वास्तुशास्त्र पढ़कर जब दिल्ली आए तो जैलेसी पर मुकेश, किशोर कुमार और लता के गाने ज़रूर जम गए थे। आज भी हमारे घर में मन्ना की एक भी कविता का पाठ रिकॉर्ड नहीं है। कभी-कभी नितान्त अपरिचित परिवार में परिचय होने के बाद सन्नाटा, गीतफरोश, घर की याद, सतपुड़ा के घने जंगल आदि कविताओं के पाठ की रिकॉर्डिंग हमें सुनने मिल जाती हैं। ये कविताएँ उन शहरों में मन्ना ने पढ़ी होंगी। वहीं वे रिकॉर्ड कर ली गईं। हमें ऐसे मौकों पर लालजी कक्कू के जैलेसी की याद ज़रूर आ जाती है, पर ईर्ष्या नहीं होती।
कवि कर्म जैसे शब्दों से हम घर में कभी कहीं टकराए नहीं। मन्ना कब कहाँ बैठकर कविता लिख लेंगे -- यह तय नहीं था। अक्सर अपने बिस्तरे पर, किसी भी कुर्सी पर एक तख्ती के सहारे उन्होंने साधारण-से-साधारण चिट्ठों पर, पीठ कोरे (एक तरफ छपे) कागज़ों पर कविताएँ लिखीं थीं। उनके मित्र और कुछ रिश्तेदार उन्हें हर वर्ष नए साल पर सुन्दर, महँगी डायरी भी भेंट करते थे। पर प्राय: उनके दो-चार पन्ने भरकर वे उन्हें कहीं रख बैठते थे। बाद में उनमें कविताओं के बदले दूध का, सब्ज़ी का हिसाब भी दर्ज हो जाता, कविता छूट जाती। भेंट मिले कविता संग्रह उन्हें खाली नई डायरी से शायद ज़्यादा खींचते थे। हमें थोड़ा अटपटा भी लगता था पर उनकी कई कविताएँ दूसरों के कविता संग्रहों के पन्नों की खाली जगह पर मिलती थीं। पीठ कोरे पन्नों से मन्ना का मोह इतना था कि कभी बाज़ार से कागज़ खरीद कर घर में आया हो -- इसकी हमें याद नहीं। फिर यह हम सबने भी सीख लिया था। आज भी हमारे घर में कोरा कागज़ नहीं आता।
परिचित-अपरिचित, पाठक, श्रोता, रिश्तेदार -- उनकी दुनिया बड़ी थी। इस दुनिया से वे छोटे-से पोस्टकार्ड से जुड़े रहते। पत्र आते ही उसका उत्तर देते। कार्ड पूरा होते ही उसे डाक के डिब्बे में डल जाना चाहिए। हम आसपास नहीं होते तो वे खुद उसे डालने चल देते। फोन घर में बहुत ही बाद में आया। शायद सन् 1968 में। इन्हीं पोस्टकार्डों पर वे सम्पादकों को कविताएँ तक भेज देते।
बचपन से लेकर बड़े होने तक मन्ना को किसी से भी अँग्रेज़ी में बात करते नहीं देखा, सुना। जबलपुर में शायद किसी अँग्रेज़ प्रिंसिपल वाले तब के प्रसिद्ध कॉलेज रॉबर्टसन से उन्होंने बी.ए. किया था। फिर आगे पढ़े नहीं। लेकिन अँग्रेज़ी खूब अच्छी थी। घर में अँग्रेज़ी साहित्य, अँग्रेज़ी कविताओं की पुस्तकें भी उनके छोटे-से संग्रह में मिल जाती थीं। पर अँग्रेज़ी का उपयोग हमें याद नहीं आता। बस एक बार सम्पूर्ण गांधी वांङ्मय के मुख्य सम्पादक किसी प्रसंग में घर आए। वे दक्षिण के थे और हिन्दी बिलकुल नहीं आती थी उन्हें। मन्ना उनसे काफी देर तक अँग्रेज़ी में बात कर रहे थे -- हमारे लिए यह बिलकुल नया अनुभव था। दस्तखत, खत-किताब -- सब कुछ बिना किसी नारेबाज़ी के, आन्दोलन के -- उनका हिन्दी में ही था और हम सब पर इसका खूब असर पड़ा। घर में, परिवार में प्राय: बुन्देलखण्डी और बाहर हिन्दी -- हमें भी इसके अलावा कभी कुछ सूझा भी नहीं। हमने कभी कहीं भी हचक कर, उचक कर अँग्रेज़ी नहीं बोली, अँग्रेज़ी नहीं लिखी।
कोई भी पतन, गड्ढा इतना गहरा नहीं होता, जिसमें गिरे हुए को स्नेह की उँगली से उठाया न जा सके -- एक कविता में कुछ ऐसा ही मन्ना ने लिखा था। उन्हें क्रोध करते, कड़वी बात करते हमने सुना नहीं। हिन्दी साहित्य में मन्ना की कविता छोटी है कि बड़ी है, टिकेगी या पिटेगी -- इसमें उन्हें बहुत फँसते हमने देखा नहीं। हाँ, अन्तिम वर्षों में कुछ वक्तव्य वगैरह लोग माँगने लगे थे। तब मन्ना इन वक्तव्यों में कहीं-कहीं कुछ कटु भी हुए थे। एक बार मैं चाय देने उनके कमरे में गया था तो सुना कि वे किसी से कह रहे थे, “मूर्ति तो समाज में साहित्यकार की ही खड़ी होती है, आलोचक की नहीं!”
हम उनके स्नेह की उँगली पकड़कर पले-बढ़े थे। इसलिए ऐसे प्रसंग में हमें उन्हीं की सीख से खासी कड़वाहट दिखी थी। पर उन्हें एक दौर में गांधी का कवि तक तो ठीक, बनिए का कवि भी कहा गया तो ऐसे अप्रिय प्रसंग उनके संग जुड़ ही गए एकाध। फिर अपनी एक कविता में उन्होंने लिखा है कि ‘दूध किसी का धोबी नहीं है। किसी की भी ज़िन्दगी दूध की धोई नहीं है। आदमकद कोई नहीं है।’ कवि के नाते उनका कद क्या था -- यह तो उनके पाठक, आलोचक ही जानें। हम बच्चों के लिए तो वे एक ठीक आदमकद पिता थे। उनकी स्नेह भरी उँगली हमें आज भी गिरने से बचाती हैं।
सभी चित्र: कनक शशि: एकलव्य, भोपाल के प्रकाशन समूह के साथ काम करती हैं।
यह लेख गांधी मार्ग पत्रिका के मई-जून, 2012 के अंक से साभार।

