लेखक : शोभा सिन्हा
अनुवाद: भरत त्रिपाठी [Hindi PDF, 317 kB]
 साक्षरता और विकास के रिश्ते की प्रकृति बड़ी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों शब्दों में से किसी को भी परिभाषित करना आसान नहीं है। लेकिन, शुरुआती दौर से ही दोनों के बीच एक सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध मान लिया गया है। यही धारणा तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उन जन साक्षरता अभियानों की बुनियाद थी जो इस आशा से शु डिग्री किए गए कि इनसे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस धारणा के पीछे शायद यह कारण रहा हो कि विकसित देशों में साक्षरता दरें बहुत ऊँची थीं इसलिए दोनों के बीच एक सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध मान लिया गया (दासवानी, 1994)। लेकिन नज़दीकी परीक्षण से पता चलता है कि यह धारणा कुछ ज़्यादा ही सतही है। दासवानी इस धारणा को ‘भ्रामक’ बताते हैं और साक्षरता तथा विकास के जटिल स्वरूपों को उदाहरणों द्वारा समझाते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी प्रतिरूप का भी पुनर्मूल्यांकन किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि पश्चिमी देशों में जन साक्षरता से पहले ही आर्थिक विकास हो चुका था, वह जन साक्षरता का परिणाम नहीं था। कुछ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश, जैसे कि थाईलैंड में साक्षरता दर ऊँची है, पर उसके मुताबिक वहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ है।
साक्षरता और विकास के रिश्ते की प्रकृति बड़ी पेचीदा और चुनौतीपूर्ण है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दोनों शब्दों में से किसी को भी परिभाषित करना आसान नहीं है। लेकिन, शुरुआती दौर से ही दोनों के बीच एक सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध मान लिया गया है। यही धारणा तीसरी दुनिया के देशों द्वारा उन जन साक्षरता अभियानों की बुनियाद थी जो इस आशा से शु डिग्री किए गए कि इनसे देश के आर्थिक विकास में मदद मिलेगी। इस धारणा के पीछे शायद यह कारण रहा हो कि विकसित देशों में साक्षरता दरें बहुत ऊँची थीं इसलिए दोनों के बीच एक सीधा कार्य-कारण सम्बन्ध मान लिया गया (दासवानी, 1994)। लेकिन नज़दीकी परीक्षण से पता चलता है कि यह धारणा कुछ ज़्यादा ही सतही है। दासवानी इस धारणा को ‘भ्रामक’ बताते हैं और साक्षरता तथा विकास के जटिल स्वरूपों को उदाहरणों द्वारा समझाते हैं। उदाहरण के लिए, पश्चिमी प्रतिरूप का भी पुनर्मूल्यांकन किए जाने की ज़रूरत है क्योंकि पश्चिमी देशों में जन साक्षरता से पहले ही आर्थिक विकास हो चुका था, वह जन साक्षरता का परिणाम नहीं था। कुछ दक्षिण-पूर्वी एशियाई देश, जैसे कि थाईलैंड में साक्षरता दर ऊँची है, पर उसके मुताबिक वहाँ आर्थिक विकास नहीं हुआ है।
सैद्धान्तिक रूप से भी, साक्षरता के परिणामों और उसकी बदलावकारी क्षमताओं की शुरुआती धारणाओं को संज्ञानात्मक, सामाजिक, और अन्य अर्थों से चुनौतियाँ मिली थीं। शुरू- शु डिग्री में, साक्षरता को इन बदलावों के कारण के रूप में देखा जाता था। पर, बहुत ज़्यादा नियतात्मक या सीमित (deterministic) होने और साक्षरता के उपयोगों के सन्दर्भ की अनदेखी करने के कारण बाद में इस दृष्टिकोण की आलोचना हुई। इसलिए, अब साक्षरता के परिणामों की बजाय उसके उपयोगों पर ध्यान केन्द्रित करने की, और इस प्रकार साक्षरता की कार्य-कारण व उपयोगितावादी धारणाओं में अन्तर करने की ज़रूरत है। इसके बाद, जैसा कि ऑॅल्सन और टॉरेन्स (2001) कहते हैं, साक्षरता और सामाजिक विकास के बीच के सम्बन्ध को समझने के लिए हमें साक्षरता को, उसके स्वरूपों और कार्यों की दृष्टि से, ज़्यादा व्यापक सन्दर्भों में देखना होगा।
फिलहाल, साक्षरता के परिणामों के मामले में प्रचलित अक्षम धारणा की जगह उसकी पेचीदगियों के बारे में पनपी एक गहरी समझ ने ले ली है। जैसा कि दासवानी बताते हैं, साक्षरता सम्बन्धी कार्यक्रम अब सिर्फ साधारण साक्षरता कार्यक्रम न रहकर साक्षरता की बृहत धारणा को शामिल करने लगे हैं। ये बदलाव विभिन्न अभियानों को मिली अपर्याप्त सफलता, भागीदारों को प्रेरित करने की ज़रूरतों को अनदेखा करने वाली नीतियों, और साक्षरता मुहिम को बरकरार रखने की असमर्थता के परिणाम-स्वरूप हुए। इससे साक्षरता कार्यक्रमों की गुणवत्ता और उनके सन्दर्भों पर प्रश्न खड़े होते हैं। एक मुद्दा जिससे नीति-निर्माताओं और विद्वानों, दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ा है, वह साक्षरता की परिभाषा है। यह स्पष्ट है कि साक्षरता कोई स्थिर या सर्वत्र एकरूप ऐसी दशा नहीं है जो कि अपने आप किसी व्यक्ति की ज़िन्दगी या कि समाज को रूपान्तरित कर दे। बाकी चीज़ों के साथ इसे भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है कि कोई किस स्तर की साक्षरता की बात कर रहा है। ‘सामाजिक क्रियाकलापों और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं की व्यवस्था में घुली-मिली साक्षरता, और वर्णमाला में पारंगत होना, जो कि सिर्फ एक तकनीकी योग्यता है’ (ट्राइबेल, 2001) के बीच फर्क किया जाना बहुत ज़रूरी है। यह एक महत्वपूर्ण भेद है क्योंकि कई साक्षरता अभियानों में साक्षरता को बहुत ही सरलीकृत ढंग से देखा गया, क्योंकि उनका उद्देश्य पढ़ने-लिखने की न्यूनतम योग्यता पैदा करना था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसका उपयोग क्या होगा या कि किसी व्यक्ति की ज़िन्दगी में उसका क्या अर्थ होगा।
इस तथ्य के बावजूद कि अब साक्षरता को आर्थिक व सामाजिक विकास की मंज़िल के सुनिश्चित मार्ग के रूप में नहीं देखा जाता, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि अभी इसमें बहुत-सी सम्भावनाएँ और छिपी हैं और यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह ज़रूरी है कि शिक्षा में काम करने वाले लोग इन सम्भावनाओं को तलाशें क्योंकि महज़ कूटलेखन (भावों, आशयों को शब्दों में व्यक्त करना) और कूटानुवाद/संकेतानुवाद (शब्दों की पहचान कर पाना) का थोड़ा-सा कौशल भर हासिल होने से सामाजिक यथार्थ को नहीं बदला जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में फ्रेरे का योगदान महत्वपूर्ण था क्योंकि उन्होंने साक्षरता को कोई यांत्रिक कौशल न मानते हुए उसे ‘मुक्ति’ के एक साधन के रूप में देखा। उन्होंने सिर्फ शब्द मात्र को पढ़ने की बजाय दुनिया को पढ़ने पर ज़ोर दिया।
यहाँ पर हम साक्षरता को केवल मात्रात्मक रूप में ही नहीं बल्कि गुणात्मक रूप में भी देखेंगे। इस तरह, साक्षरता सिर्फ एक तकनीकी, यांत्रिक कौशल नहीं है बल्कि वह ऐसा आचरण है जो कि किसी व्यक्ति को समर्थ व सशक्त बना सकता है। पहले, मैं भारत के साक्षरता-सम्बन्धी प्रचलनों का एक व्यापक विवरण सामने रखूँगी। उसके बाद, मैं स्कूली शिक्षा की भूमिका की चर्चा करूँगी, और उसके बाद भारत में स्कूली साक्षरता से सम्बन्धित मुद्दों और समस्याओं की बात करूँगी।
भारत में साक्षरता भारत में साक्षरता दर में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है - 1951 से लेकर 2001 की जनगणना में यह 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 64.8 प्रतिशत हो गई है। लेकिन, यह बढ़ती हुई दर कुछ निराशाजनक तथ्यों को छिपा देती है। एक तथ्य तो यह है कि इस बढ़ती साक्षरता दर के साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते निरक्षर लोगों की कुल संख्या में कमी नहीं आई है। इसके अलावा, अलग-अलग क्षेत्रों व लिंग की दृष्टि से तथा शहरी व ग्रामीण आबादियों के बीच साक्षरता दरों में अच्छा-खासा अन्तर है। इस दुखद कहानी का एक और पहलू यह है कि जो लोग साक्षर हो भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास साक्षरता का वह स्तर हो जो कि व्यक्ति द्वारा स्वयं को समझने के अर्थ में या एक स्तर तक विवेचनात्मक चेतना को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी माना जाता है। कुमार के अनुसार भारत में साक्षरता का एक ‘सीमित, बल्कि निर्बल’ अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पर साक्षरता को न्यूनतम दायरे में परिभाषित करने की प्रवृत्ति है। साक्षरता के दायरे की सीमा में बस लिखे हुए का आशय समझ पाना और थोड़ा-बहुत लिख सकना, जैसे कि किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने की, कुछ बुनियादी क्षमता दर्शा पाना ही शामिल है (अग्निहोत्री, 1997)। इसलिए, अगर साक्षरता को ‘ऐसी बातों को समझने तथा लिखने की क्षमता’ के रूप में परिभाषित किया जाए ‘जो किन्हीं अर्थों में व्यक्ति को सशक्त बनाती हो और अन्वेषण के नए रास्ते खोलती हो, तो साक्षरता दर नाटकीय ढंग से गिर जाएगी, सात वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी का सम्भवत: चौथाई से भी कम भाग साक्षर कहला पाएगा’। यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे देश में साक्षरता दर में हुए इज़ाफे का कारण दरअसल, साक्षरता का अत्यन्त उदार (सतही) मानदण्ड है।
भारत में साक्षरता दर में लगातार बढ़ोत्तरी हुई है - 1951 से लेकर 2001 की जनगणना में यह 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 64.8 प्रतिशत हो गई है। लेकिन, यह बढ़ती हुई दर कुछ निराशाजनक तथ्यों को छिपा देती है। एक तथ्य तो यह है कि इस बढ़ती साक्षरता दर के साथ ही साथ बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते निरक्षर लोगों की कुल संख्या में कमी नहीं आई है। इसके अलावा, अलग-अलग क्षेत्रों व लिंग की दृष्टि से तथा शहरी व ग्रामीण आबादियों के बीच साक्षरता दरों में अच्छा-खासा अन्तर है। इस दुखद कहानी का एक और पहलू यह है कि जो लोग साक्षर हो भी जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास साक्षरता का वह स्तर हो जो कि व्यक्ति द्वारा स्वयं को समझने के अर्थ में या एक स्तर तक विवेचनात्मक चेतना को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी माना जाता है। कुमार के अनुसार भारत में साक्षरता का एक ‘सीमित, बल्कि निर्बल’ अर्थ निकाला जाता है। यहाँ पर साक्षरता को न्यूनतम दायरे में परिभाषित करने की प्रवृत्ति है। साक्षरता के दायरे की सीमा में बस लिखे हुए का आशय समझ पाना और थोड़ा-बहुत लिख सकना, जैसे कि किसी दस्तावेज़ पर दस्तखत करने की, कुछ बुनियादी क्षमता दर्शा पाना ही शामिल है (अग्निहोत्री, 1997)। इसलिए, अगर साक्षरता को ‘ऐसी बातों को समझने तथा लिखने की क्षमता’ के रूप में परिभाषित किया जाए ‘जो किन्हीं अर्थों में व्यक्ति को सशक्त बनाती हो और अन्वेषण के नए रास्ते खोलती हो, तो साक्षरता दर नाटकीय ढंग से गिर जाएगी, सात वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों की आबादी का सम्भवत: चौथाई से भी कम भाग साक्षर कहला पाएगा’। यह बिलकुल स्पष्ट है कि हमारे देश में साक्षरता दर में हुए इज़ाफे का कारण दरअसल, साक्षरता का अत्यन्त उदार (सतही) मानदण्ड है।
अग्निहोत्री ने भारत में साक्षरता शिक्षा के इतिहास को सिलसिलेवार दर्शाया है। साक्षरता का मुद्दा, कई समाज सुधार आन्दोलनों के एजेंडे का और फिर बाद में स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा रहा। कई राष्ट्रीय नेताओं ने, जिसमें गांधी और टैगोर भी शामिल थे, राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए साक्षरता के महत्व को पहचाना। लेकिन, बाद में, स्वतंत्रता संघर्ष के साथ जुड़ा जोश जब ठण्डा पड़ा तो वयस्कों के साक्षरता कार्यक्रमों का चरित्र बहुत ही सीमित कामकाजी किस्म का हो गया। स्वतंत्रता के पश्चात साक्षरता कार्यक्रम को सरकार व गैर-सरकारी संगठनों ने अपने हाथों में ले लिया। दुर्भाग्यवश, अर्थहीन और उबाऊ सामग्री, साक्षरता का संकुचित अर्थ (जैसे कि अपना नाम-पता लिख-पढ़ लेना मात्र) लगा लेने, अपर्याप्त वित्तीय संसाधनों, और दूरदर्शिता की कमी के कारण ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सके।
भारत में साक्षरता पर होने वाली चर्चाओं में किसी व्यक्ति को साक्षर बनाने में स्कूलों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका को तकरीबन पूरी तरह से बाहर ही रखा जाता है। सबसे प्रमुख समस्या निरक्षरों की विशाल संख्या है और जिसका हल प्रमुखत: वयस्क साक्षरता अभियानों के रूप में देखा जाता है। कुमार (2004) दर्शाते हैं कि भारत में ‘साक्षरता’ शब्द को वयस्क शिक्षा द्वारा पूरी तरह से हथिया लिया गया है, क्योंकि नीति-दस्तावेज़ और शैक्षणिक शोध पत्रिकाएँ साक्षरता को लेकर स्कूल और बच्चों की शिक्षा के सन्दर्भ में, मौन हैं। हालाँकि वयस्क साक्षरता कार्यक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर आश्चर्य होता है कि आखिर क्यों बच्चों के साक्षर होने के बहुत ज़ाहिर-से सन्दर्भ को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जाता है। बहुत थोड़े-से अपवादों को यदि छोड़ दें तो इस बात का ज़िक्र ही नहीं किया जाता कि बच्चों को स्कूलों में किस प्रकार के साक्षरता अनुभव मिलते हैं।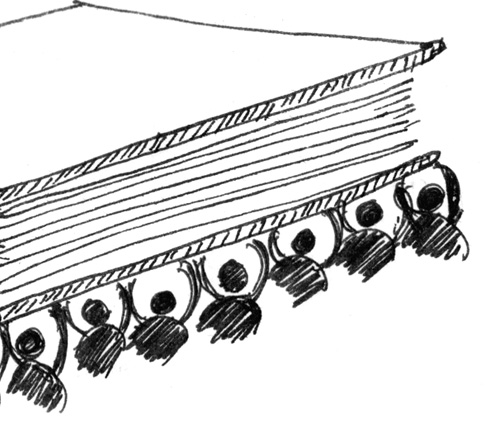 भारत जैसे देश में साक्षरता हासिल करने में स्कूलों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए यह ‘लोप’ वाकई समझ से परे है। टील और सल्ज़बी (1986) द्वारा ऊँची साक्षरता दरों वाले देशों में बच्चों की शुरुआती साक्षरता प्रगति पर किए गए शोध अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे ऐसे अनौपचारिक परिवेशों में भी साक्षर बनते हैं जहाँ उन्हें सार्थक तरीकों से साक्षर बनने के और उसकी प्रकृति के बारे में अनुमान लगा पाने के मौके मिलते हैं। लेकिन, भारत में निम्न सामाजिक-आर्थिक दर्ज़े वाले, खास तौर पर निरक्षर परिवारों वाले, अधिकांश बच्चे अनौपचारिक ढंग से अक्षर ज्ञान हासिल करने के मौकों से वंचित ही रह जाते हैं। इसके अलावा, यह भी बहुत सम्भव है कि उनमें से कइयों को कोचिंग व ट्यूशनों के लिए अपने घरों से औपचारिक सहयोग न मिले, हालाँकि, इन ट्यूशनों और कोचिंगों की शैक्षणिक गुणवत्ता भी सन्देह के घेरे में ही रहती है। इसलिए, ये बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से स्कूलों पर आश्रित रहते हैं। अत: भारत में साक्षरता के प्रसार में स्कूलों की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बच्चों को स्कूल में पर्याप्त मदद प्राप्त नहीं होगी तो वे बड़े होने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सीखने तक निरक्षर बने रहने के लिए बाध्य हैं। अगर वे शुरुआती कक्षाओं में ढंग से साक्षरता हासिल नहीं करते तो उनका स्कूल में बने रह पाना बेहद मुश्किल होता चला जाता है। उन्हें न सिर्फ भाषा की कक्षाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि लगभग सभी स्कूली विषयों, जैसे सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में भी। हो सकता है कि उन्हें मजबूर होकर स्कूल भी छोड़ना पड़ जाए क्योंकि स्कूली शिक्षा के आगे के वर्षों में टिके रहने के लिए और ज़्यादा- से-ज़्यादा साक्षरता ज्ञान की ज़रूरत होती है। इससे यह स्पष्ट है कि स्कूल में बने रहने के लिए साक्षरता बुनियादी ज़रूरत है। दरअसल, एन. कुमार ने बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ देने की ऊँची दर और स्कूल में साक्षरता के साथ बच्चों के अनुभवों के बीच के सम्बन्ध की पड़ताल की है।
भारत जैसे देश में साक्षरता हासिल करने में स्कूलों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका को मद्देनज़र रखते हुए यह ‘लोप’ वाकई समझ से परे है। टील और सल्ज़बी (1986) द्वारा ऊँची साक्षरता दरों वाले देशों में बच्चों की शुरुआती साक्षरता प्रगति पर किए गए शोध अध्ययनों से पता चलता है कि बच्चे ऐसे अनौपचारिक परिवेशों में भी साक्षर बनते हैं जहाँ उन्हें सार्थक तरीकों से साक्षर बनने के और उसकी प्रकृति के बारे में अनुमान लगा पाने के मौके मिलते हैं। लेकिन, भारत में निम्न सामाजिक-आर्थिक दर्ज़े वाले, खास तौर पर निरक्षर परिवारों वाले, अधिकांश बच्चे अनौपचारिक ढंग से अक्षर ज्ञान हासिल करने के मौकों से वंचित ही रह जाते हैं। इसके अलावा, यह भी बहुत सम्भव है कि उनमें से कइयों को कोचिंग व ट्यूशनों के लिए अपने घरों से औपचारिक सहयोग न मिले, हालाँकि, इन ट्यूशनों और कोचिंगों की शैक्षणिक गुणवत्ता भी सन्देह के घेरे में ही रहती है। इसलिए, ये बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए पूर्ण रूप से स्कूलों पर आश्रित रहते हैं। अत: भारत में साक्षरता के प्रसार में स्कूलों की भूमिका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि बच्चों को स्कूल में पर्याप्त मदद प्राप्त नहीं होगी तो वे बड़े होने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में सीखने तक निरक्षर बने रहने के लिए बाध्य हैं। अगर वे शुरुआती कक्षाओं में ढंग से साक्षरता हासिल नहीं करते तो उनका स्कूल में बने रह पाना बेहद मुश्किल होता चला जाता है। उन्हें न सिर्फ भाषा की कक्षाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा बल्कि लगभग सभी स्कूली विषयों, जैसे सामाजिक अध्ययन और विज्ञान में भी। हो सकता है कि उन्हें मजबूर होकर स्कूल भी छोड़ना पड़ जाए क्योंकि स्कूली शिक्षा के आगे के वर्षों में टिके रहने के लिए और ज़्यादा- से-ज़्यादा साक्षरता ज्ञान की ज़रूरत होती है। इससे यह स्पष्ट है कि स्कूल में बने रहने के लिए साक्षरता बुनियादी ज़रूरत है। दरअसल, एन. कुमार ने बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ देने की ऊँची दर और स्कूल में साक्षरता के साथ बच्चों के अनुभवों के बीच के सम्बन्ध की पड़ताल की है।
ऑल्सन और टॉरेंस (2001) के अनुसार ‘आधुनिक समाज में स्कूली शिक्षा और साक्षरता बुनियादी रूप से एक साथ चलने वाली बातें हैं’ और ‘किसी देश के साक्षरता स्तर का स्कूली शिक्षा के वर्षों से बहुत निकट का सम्बन्ध होता है’। भारतीय स्कूलों में पढ़ने के निर्देशों की प्रकृति की और उसके सम्भावित कारण की पड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। यह मुश्किल काम है क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया है, इस बाबत बहुत कम अध्ययन-आधारित सामग्री उपलब्ध है।
स्कूली सन्दर्भ में साक्षरता
बच्चों द्वारा बीच में ही स्कूल छोड़ देने की समस्या ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को एक चुनौती बना दिया है। कई शोधकर्ताओं द्वारा इस समस्या की पड़ताल की गई है। अतीत में, मुख्य रूप से बच्चों की पृष्ठभूमि को उनके स्कूल छोड़ देने का प्रमुख कारण माना गया। कृष्ण कुमार (1992) ने स्कूल छोड़ देने की समस्या को पूरी तरह से समझने के लिए स्कूल-सम्बन्धी कारकों की पड़ताल करने की ज़रूरत को चिन्हांकित किया है। वे दावा करते हैं कि कमज़ोर साक्षरता शिक्षण पद्धति इसका कारण हो सकता है। एनजीओज़ द्वारा तैयार की गई हालिया वार्षिक शिक्षा स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) बताती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर कम है। लेकिन, वाचन क्षमता सम्बन्धी आँकड़े कतई उत्साहवर्धक नहीं हैं। इस राष्ट्रीय स्तर के सर्वे के मुताबिक, पढ़ने के लिए दिए गए कार्यों को पैराग्राफ स्तर (पढ़ने की कठिनाई का पहला स्तर), सरल कहानी पढ़ना (पढ़ने की कठिनाई का दूसरा स्तर), शब्द पढ़ने, और अक्षर पढ़ने की श्रेणियों में विभक्त किया गया। जो जानकारियाँ सामने आईं, उनके अनुसार 35 प्रतिशत बच्चे एक सरल-सा पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए, जबकि 52 प्रतिशत बच्चे कहानी नहीं पढ़ पाए। छोटी आयु वर्ग (7 - 10 वर्ष) वाले बच्चों में ये आँकड़े और भी ज़्यादा थे : उनमें 48.2 प्रतिशत पहले स्तर का पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए और 68 प्रतिशत स्तर-2 की कहानियाँ पढ़ पाने में सक्षम नहीं थे। 44 प्रतिशत बच्चे स्तर-2 के सरल पैराग्राफ नहीं पढ़ पाए। क्षेत्रीय आधार पर देखें तो इन आँकड़ों में व्यापक भिन्नताएँ हैं। ये आँकड़े केवल बच्चों की संकेतानुवाद करने (अक्षरों को पहचानने) की योग्यता पर आधारित हैं और उनकी समझने की क्षमता को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिर भी बच्चों ने बहुत कमतर प्रदर्शन किया। बच्चों की समझने-बूझने की क्षमता के बारे में व्यवस्थित अध्ययन बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन, कुछ अध्ययन जो उपलब्ध हैं, दर्शाते हैं कि बच्चों की पढ़कर समझ पाने की क्षमता भी बहुत कमज़ोर है। थॉर्नडाइक को (1973) 15 देशों पर किए गए अपने अध्ययन से पता चला कि भारतीय विद्यार्थी पढ़कर समझ पाने में बहुत कमज़ोर हैं। हालाँकि, यह अध्ययन कुछ पहले का है, फिर भी यह मान लेने का कोई कारण नहीं है कि अब स्थिति बदल गई होगी। हालिया अध्ययनों से भी बहुत सुधार ज़ाहिर नहीं होता। उदाहरण के लिए, नरसिम्हन (2004) ने मुम्बई के सम्भ्रान्त स्कूलों में बच्चों की भाषाई समझ को जानने हेतु परीक्षा का आयोजन किया। परीक्षा में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और शैक्षणिक गद्य शामिल किए गए। नतीजे उन्हें ‘अनपेक्षित’ लगे क्योंकि बच्चे मुम्बई के सम्भ्रान्त स्कूलों के थे, पर उनके प्रदर्शन में भी इस समस्या की व्यापकता उजागर हुई और उनका औसत प्रदर्शन सार्वजनिक परीक्षाओं में उनकी उपलब्धियों से कमतर था। नरसिम्हन ने समझाया कि उन पब्लिक स्कूलों में बच्चों को परीक्षाओं में सफल होना सिखाया गया पर वे उन्हें अपरिचित गद्यों और कार्यों को कर पाने के लिए तैयार नहीं कर पाए।
भारत में साक्षरता शिक्षण भारतीय विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार के प्रदर्शन को समझने के लिए कक्षा में होने वाली साक्षरता शिक्षण पद्धति की पड़ताल करना ज़रूरी है, खास तौर पर शुरुआती कक्षाओं में होने वाला शिक्षण। शिक्षण की प्रकृति के बारे में अन्दाज़ा लगाने के लिए हमें मुख्यत: पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षक पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों पर ही बहुत अधिक निर्भर करते हैं, अत: पाठ्य पुस्तकें कक्षाओं में होने वाले कामों की अच्छी संकेतक हैं।
भारतीय विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार के प्रदर्शन को समझने के लिए कक्षा में होने वाली साक्षरता शिक्षण पद्धति की पड़ताल करना ज़रूरी है, खास तौर पर शुरुआती कक्षाओं में होने वाला शिक्षण। शिक्षण की प्रकृति के बारे में अन्दाज़ा लगाने के लिए हमें मुख्यत: पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। शिक्षक पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकों पर ही बहुत अधिक निर्भर करते हैं, अत: पाठ्य पुस्तकें कक्षाओं में होने वाले कामों की अच्छी संकेतक हैं।
भारत में, साक्षरता शिक्षण की प्रकृति मुख्यत: पारम्परिक है। इसमें लगभग पूरा ज़ोर अर्थ की बजाय ध्वनियों पर ही दिया जाता है। हालाँकि, यहाँ भी, कक्षाओं के बारे में बहुत ज़्यादा विवरणात्मक जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी, शुरुआती पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण करके साक्षरता शिक्षण के बारे में कुछ निष्कर्ष तो निकाले ही जा सकते हैं क्योंकि भारत में शिक्षण बहुत कुछ पाठ्य पुस्तकों पर ही निर्भर करता है। ऐसे एक अध्ययन में प्रारम्भिक वाचन शिक्षण की प्रकृति को समझने के लिए 10 शुरुआती हिन्दी पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण किया गया (सिन्हा, 2000)। इस अध्ययन से पता चला कि बच्चों का पूरा ध्यान ग्राफोफोनिक्स (भाषा के अक्षरों और उनकी ध्वनियों के सम्बन्ध) पर होता है। अभ्यासों व पाठों को विषय-प्रसंगों की बजाय किन्हीं ध्वनियों के इर्द-गिर्द रचा गया था। अत: सामान्यतया उनमें किसी लक्षित ध्वनि वाले शब्दों की सूची के साथ शुरुआत की गई। उदाहरण के लिए, एक पाठ में निम्नलिखित शब्द सूचीबद्ध थे: कार, भात, सागर, सरकार, दमा, शाम, तलवार, साल और काला। शब्दों का यह बेबूझ संग्रह इसलिए बनाया गया क्योंकि हिन्दी में इन सभी शब्दों में एक साझी आवाज़ ‘आ’ आती है (जिसकी ‘कार’ में आने वाले ‘आ’ से तुक मिल जाती है)। विषयसूत्र की दृष्टि से असम्बद्ध शब्दों की इस सूची के बाद ऐसे वाक्य दिए गए हैं जहाँ अधिकतम शब्दों में लक्षित ध्वनि का इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, ‘ओ’ ध्वनि वाले एक पाठ में इस तरह के वाक्य दिए गए:
ढोल बजाओ। चोर भगाओ। शोर न मचाओ। पाठशाला चलो। किताब खोलो। बोलकर पढ़ो। देखकर लिखो। तोते को राम-राम रटने दो।
बाकी सब बातों को छोड़कर सिर्फ ध्वनियों के आधार पर सिखाने की अपनी सनक के चलते पाठ बिखरे हुए, असम्बद्ध और कई दफा बिलकुल ही असंगत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आम पर चढ़, गिलास सिर पर मत रख।
ये पाठ दरअसल, पढ़ते वक्त अर्थ ‘न’ तलाशना सिखाते हैं। यदि कोई समझने के लिए इन पाठों को पढ़े तो उसका अनुभव बिलकुल ही विचित्र होगा क्योंकि समझने के लिए कोई सुसंगत गद्य होता ही नहीं। यदि बच्चा पढ़ना सीखने के लिए पूरी तरह से सिर्फ इन्हीं पाठों पर निर्भर करे तो उसे यह सन्देश मिलेगा कि पढ़ना बिलकुल निरर्थक, गूढ़ और काफी बेहूदी प्रक्रिया है। यदा-कदा, जब कभी पाठों में विषय की एकसूत्रता पर ध्यान दिया भी गया तो उसकी शैली ज़्यादा पठनीय या रोचक नहीं थी। उसमें प्रवाह नहीं था और उनकी विषयवस्तु सुसंगत होते हुए भी रोचक नहीं थी।
एक अन्य अध्ययन में कौशिक शुरुआती साक्षरता के बारे में पहली कक्षा के शिक्षकों की मान्यताओं की पड़ताल करती हैं। उन्हें मालूम पड़ा कि शिक्षक के दृष्टिकोण पाठ्य पुस्तकों में प्रदर्शित दृष्टिकोणों के अनुरूप हैं। पाठ्य पुस्तकों में ध्यान सिलसिलेवार ढंग से अक्षरों के ज्ञान, और अक्षरों को मिलाकर शब्द बनाने के अध्ययन पर केन्द्रित किया गया है। पढ़ने की अवधारणा का मुख्य लक्ष्य अक्षरों को पहचान लेना माना गया और हर पाठ का उद्देश्य प्रत्येक ध्वनि का अभ्यास करना था। शिक्षकगण साक्षरता की सिलसिलेवार प्रकृति को लेकर अपनी मान्यताओं के प्रति बहुत आग्रही थे। उनकी मुख्य चिन्ता सही उच्चारण और लिखते समय अक्षरों की सही बनावट को लेकर थी। छपे हुए से ज़रा-से भी फर्क को त्रुटि माना जाता था।
वाचन के सिद्धान्त और शोध
पारम्परिक रूप से, वाचन को संकीर्ण रूप से सिर्फ संकेतानुवाद (अक्षरों को पहचानना) की प्रक्रिया माना गया, यानी लिखी हुई भाषा का मौखिक समरूप तलाशना। इसलिए साक्षरता शिक्षा में वाचन के ग्राफोफोनिक्स (अक्षर-ध्वनि सम्बन्ध) पहलू पर ज़ोर दिया गया। प्रारम्भिक साक्षरता शिक्षा में बच्चों को वाचन के उप-कौशलों पर सिलसिलेवार ढंग से अधिकार करना सिखाया गया। इसलिए, बच्चों से यह अपेक्षा की गई कि वे अक्षर-ध्वनि सम्बन्ध पर पूरा अधिकार कर लें और शब्दों का संकेतानुवाद करने के लिए अक्षरों का मिश्रण करना सीखें। जैसा कि टील और सल्ज़बी (1986) बताते हैं, एक प्रवृत्ति यह भी थी कि पढ़ना सीखते समय भाषा के कामकाजी पहलुओं की बजाय उसके औपचारिक पहलुओं पर ध्यान देना।
 पढ़ने से जुड़ी इस पद्धति की कई आधार पर आलोचना की गई। उप-योग्यताओं में सिलसिलेवार प्रवीणता हासिल कराने और बार-बार अभ्यास कराने की पद्धति पर ज़ोर देने वाले, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने भाषा को कई अर्थहीन इकाइयों में बाँट दिया। परिणामस्वरूप, पढ़ना सीखना एक उबाऊ और यांत्रिक प्रक्रिया बन गई जो बच्चों के लिए अरुचिकर और अप्रासंगिक थी। इस पद्धति की एक अन्य समस्या यह थी कि इसमें भाषा के किसी व्यावहारिक उपयोग को सम्मिलित नहीं किया गया था। मौखिक भाषा के विकास के विपरीत, जहाँ कि बच्चों द्वारा शब्दों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना एक साथ घटता है, यहाँ उनसे भाषा का उपयोग करने से पहले लिखी हुई भाषा के औपचारिक पहलुओं पर पूरी तरह से पकड़ जमा लेने की अपेक्षा की गई।
पढ़ने से जुड़ी इस पद्धति की कई आधार पर आलोचना की गई। उप-योग्यताओं में सिलसिलेवार प्रवीणता हासिल कराने और बार-बार अभ्यास कराने की पद्धति पर ज़ोर देने वाले, सीखने के व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने भाषा को कई अर्थहीन इकाइयों में बाँट दिया। परिणामस्वरूप, पढ़ना सीखना एक उबाऊ और यांत्रिक प्रक्रिया बन गई जो बच्चों के लिए अरुचिकर और अप्रासंगिक थी। इस पद्धति की एक अन्य समस्या यह थी कि इसमें भाषा के किसी व्यावहारिक उपयोग को सम्मिलित नहीं किया गया था। मौखिक भाषा के विकास के विपरीत, जहाँ कि बच्चों द्वारा शब्दों को ग्रहण करना और उनका उपयोग करना एक साथ घटता है, यहाँ उनसे भाषा का उपयोग करने से पहले लिखी हुई भाषा के औपचारिक पहलुओं पर पूरी तरह से पकड़ जमा लेने की अपेक्षा की गई।
1960 के दशक के दौरान और उसके बाद के दशकों में भी, वाचन पर महत्वपूर्ण काम किया गया जिसमें इस मान्यता को चुनौती दी गई कि वाचन सिर्फ संकेतानुवाद है (पिअर्सन और स्टीवेन्स, 1994)। भाषा पर नोम चोम्सकी के सशक्त प्रभाव ने वाचन के क्षेत्र पर भी प्रभाव छोड़ा। शुरुआत में, भाषाई मनोगतिकी (साइको-लिंग्विस्टिक्स) और बाद में दूसरे विषयों जैसे संज्ञानात्मक (cognitive) मनोविज्ञान ने वाचन की इस उलटी पद्धति पर प्रश्न खड़े किए जिसमें अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाना, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाना इत्यादि शामिल था। वाचन को केवल संकेतानुवाद की यांत्रिक गतिविधि के रूप में न देखने की बजाय उसे समझ पैदा करने वाली गतिविधि के रूप में देखा जाने लगा। साक्षरता केवल ध्वनियों तक सीमित नहीं रह गई बल्कि उसमें पढ़ने का पूरा कृत्य समाहित हो गया जिसमें समझना भी शामिल था। स्मिथ (1971) के अनुसार, अक्षरों पर अत्यधिक ध्यान दिए जाने को समझने की प्रक्रिया के लिए हानिकारक माना गया।
पढ़ना सीखने के सम्बन्ध में, वाचन की एक भिन्न और व्यापक अवधारणा पर आधारित एक विकासात्मक दृष्टिकोण, उद्गामी साक्षरता (emergent literacy), ने प्रमुखता हासिल कर ली। शुरुआत से ही वाचन को समझ पैदा करने वाली गतिविधि के रूप में देखा गया। बच्चे अपनी आस-पास की छपी हुई चीज़ों के बारे में सक्रिय रूप से परिकल्पनाएँ निर्मित करके साक्षर बनने लगे। पढ़ने और लिखने को लेकर किसी बच्चे के प्रारम्भिक प्रयास, उदाहरण के लिए, घसीटा लेखन, मनगढ़न्त हिज्जे, या स्वांग-वाचन करने को साक्षरता सिखाने के वैध तरीकों के रूप में देखा गया और पारम्परिक वाचन से भिन्न होने के कारण इन्हें अस्वीकृत नहीं किया गया (टील और सल्ज़बी, 1986)। इस पद्धति का शैक्षणिक निहितार्थ बार-बार अभ्यास करना और ध्वनियों में महारत हासिल करना नहीं था बल्कि एक अर्थपूर्ण और समग्र ढंग से साक्षरता सीखना था। बच्चों में साक्षरता के विकास को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक जीवन के कार्य सुझाए गए। हेबर्ट के अनुसार ऐसे वास्तविक कार्यों में ‘बच्चे आनन्द व सम्प्रेषण के लिए साक्षरता का तुरन्त उपयोग कर पाते हैं। इन कार्यों की प्रकृति स्कूली साक्षरता जैसी नहीं होती, जिसमें साक्षरता का टुकड़ों-टुकड़ों में... भविष्य के किसी अनिश्चित उपयोग के लिए अभ्यास किया जाता है।’ इसके अलावा, गुडमैन कहते हैं कि साक्षरता शिक्षा को ज़्यादा सरल माना जाएगा अगर वह तर्कसंगत, रोचक और बच्चों के जीवन के लिए प्रासंगिक होगी।
इस प्रकार के सिद्धान्त निर्माण और शोध मुख्य रूप से साक्षरता में समृद्धता रखने वाले परिवेशों जैसे उत्तरी अमरीका और न्यूज़ीलैंड में विकसित हुए। विभिन्न देशों में हुए एक हालिया शोध में बच्चों के सीखने की प्रक्रिया के बारे में एक सतत चिन्ता उजागर होती है। यदि हम इस प्रकार के शोध को देखें, तो हम भारत में शिक्षण के सन्दर्भ में जो कुछ भी देखते हैं वह काफी निराशाजनक लगता है। यह स्पष्ट है कि प्रारम्भिक वाचन शिक्षा के नाम पर भारत में जो कुछ भी होता है वह पढ़ना सिखाने के ज़्यादा पारम्परिक प्रतिरूप के करीब है और वाचन की रचनात्मक पद्धतियों पर आधारित शोध का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अर्थहीनता के अलावा, साक्षरता के साथ बच्चों के शुरुआती प्रयासों को मान्यता न देना भी इस साक्षरता शिक्षा की कमी है। बच्चों की गतिविधियों, जैसे स्वांग-वाचन और कल्पित हिज्जे बनाना, में सुधार की गुंजाइश रहती है। समस्या यह है कि शिक्षकों के पास बच्चों की साक्षरता की विकासात्मक प्रकृति का आकलन करने के सैद्धान्तिक उपकरण नहीं होते। यह समस्या शिक्षकों तक ही सीमित नहीं है। भारत में एक बड़े साक्षरता कार्यक्रम का वर्णन करते हुए बच्चों के लिखने के शुरुआती प्रयासों को स्वीकार तो किया गया पर उन पर ‘अपरिष्कृत’ होने का ठप्पा लगा दिया गया (बनर्जी और अन्य, 2004)। इन शैक्षणिक दस्तूरों की एक अन्य समस्या यह है कि ये पूरी तरह से लेखन के औपचारिक पहलुओं पर आधारित हैं और साक्षरता के व्यावहारिक पहलुओं को पूर्णत: नजरन्दाज़ कर देते हैं। ऐसे बच्चे जिनके घरों में साक्षर लोग होते हैं, देख पाते हैं कि किस तरह साक्षरता लगातार जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और उस पर गहरा असर रखती है। लेकिन, निरक्षर परिवार के बच्चे को इसके व्यावहारिक पहलू देखने का मौका नहीं मिल पाता। हो सकता है कि उसने सुना हो कि भविष्य में कभी साक्षरता उनके काम आएगी पर वर्तमान में तो स्कूल उन्हें यह समझा पाने में असफल हो जाता है कि इन्सान साक्षरता के साथ क्या-क्या कर सकता है।
यह इत्मीनान से कहा जा सकता है कि स्कूली परिस्थिति में साक्षरता से बच्चों का सम्पर्क बेरौनक और उबाऊ होता है। अभ्यास बिलकुल नीरस होते हैं। वे बच्चे जो साक्षरता हासिल करने के लिए पूर्णत: स्कूलों पर निर्भर करते हैं उनके लिए इसके परिणाम घातक होते हैं। स्कूली दायरे में बने रहने के लिए उनमें साक्षरता और उसके महत्व से जुड़े अविश्वास को परे रखने के लिए बहुत इच्छाशक्ति होना ज़रूरी है। बच्चों को घर पर साक्षरता अनुभव न मिल पाने के लिए अधिकांशत: बच्चे व उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमियों को दोष दिया जाता है। लेकिन, निरक्षर पालकों पर दोषारोपण करने की बजाय स्कूलों के लिए यह ज़रूरी है कि वे इन बच्चों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और उन्हें उनके मुताबिक किताबों व लेखन से भरा परिवेश प्रदान करें, साक्षरता के साथ सार्थक प्रयास करने की छूट दें, और प्रेरणादायी तौर-तरीकों में साक्षरता का उपयोग करने के मौके दें। यह पता लगाना ज़रूरी है कि भारतीय कक्षाओं में इन उद्देश्यों की पूर्ति किस तरह हो सकती है।
भारत में साक्षरता शोध
अकसर यह कहा जाता है कि विकसित देशों के सिद्धान्तों और शैक्षणिक पद्धतियों को उठाकर सीधे किन्हीं अन्य देशों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह वाकई सही है। क्योंकि आसानी से यह तर्क दिया जा सकता है कि इन देशों में बहुत ऊँचे साक्षरता स्तर हैं और बच्चों को खोजबीन करने के लिए आसानी से बहुत सारी छपी हुई सामग्री उपलब्ध रहती है। पर इन तर्कों के बावजूद इन शोध को खारिज कर देना उचित नहीं होगा, खास तौर पर जबकि शैक्षणिक साहित्य में इस क्षेत्र की बिलकुल भी खोजबीन नहीं की गई है।
भारत में, समस्या का एक बड़ा पक्ष यह है कि वाचन की प्रक्रियाओं और उसके शिक्षण पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता। इस स्थिति का एक कारण भारतीय शिक्षा की आम समस्या को माना जा सकता है। एन. कुमार बनारस के शैक्षणिक प्रॉजेक्टों का वर्णन करते हुए दावा करती हैं कि अधिकांश प्रॉजेक्ट ‘शैक्षणिक अक्षमता’ के कारण असफल हुए। वे आगे कहती हैं:
“बच्चों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पूर्वाग्रह और उनकी निष्क्रियता के सम्बन्ध में मान्यताएँ बना लेने से वयस्कों को बहुत नुकसान हुआ है। शिक्षकों ने यह मान लिया कि उनके इरादों को एक बारगी व्यक्त कर देने के बाद उनका अपने आप कार्यरूप में पालन कर दिया जाएगा। ये इरादे बच्चों के अनुभवों में किस प्रकार समझे गए और इससे भी ज़्यादा कि सीखने के दृष्टिकोण से बच्चों के लिए इनका क्या महत्व था, इसके प्रति किसी भी शिक्षक को रुचि नहीं थी...।”
ऐसा लगता है कि कुछ विशेष अपवादों, जैसे कि होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम, को छोड़कर, भारत में वास्तविक शैक्षणिक प्रक्रियाओं के बारे में परवाह की कमी कोई नई बात नहीं है। शिक्षकों या संस्थाओं द्वारा साक्षरता शिक्षा की तरफ किसी भी सार्थक ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है। विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम ढाँचों पर एक निगाह डालने से इस उपेक्षा का अन्दाज़ा लग जाता है।
यहाँ, यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि हालिया हैंडबुक ऑॅफ रीडिंग रिसर्च, खण्ड-3 से पता चलता है कि वाचन की प्रक्रिया और शिक्षण पर ध्यान देने का अमरीका, इंग्लैंड, ऑॅस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों का तरीका लातिनी अमरीकी देशों के तरीके से भिन्न है। पहले समूह के देशों में प्रक्रियाओं और संस्थागत नीतियों पर शोध चर्चाएँ की गईं जबकि बाद के समूह के देशों में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। सन्ताना बताते हैं कि विकासशील देशों में शैक्षणिक शोध की प्रकृति औद्योगीकृत देशों की शोध से सैद्धान्तिक रूप से भिन्न है क्योंकि शोध भी सामाजिक व्यवहार का एक रूप है और इसलिए वह अपने सन्दर्भ के प्रति संवेदनशील होती है। दरअसल, जब कोई शोध किसी औद्योगीकृत मुल्क से ज़रूरत से ज़्यादा सामग्री लेती है तो ऐसे में उसके द्वारा अपने देश के वास्तविक परिदृश्य की अवहेलना भी हो सकती है। भारत में लैटिन अमरीका से कुछ दिलचस्प समानताएँ हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ भी शोध को कोई खास तरजीह नहीं दी जाती। लेकिन, शैक्षणिक शोध की कमी को इन आधारों पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है कि हमारी स्थिति औद्योगीकृत मुल्कों से बिलकुल अलग है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि भारतीय सन्दर्भ में बच्चे किस प्रकार पढ़ते हैं, कक्षाओं में किस प्रकार का शिक्षण होता है, कक्षाओं की गतिविधियों के सन्दर्भ में अभिनव विचारों का क्या अर्थ हो सकता है, इत्यादि। ये वे मुद्दे हैं जिनका शिक्षकों को रोज़ सामना करना पड़ता है। सन्दर्भ-सम्बन्धी अन्तर के आधार पर इन मुद्दों को अनदेखा कर देना ठीक बात नहीं है।
इस सन्दर्भ में, विश्वविद्यालयों के भीतर शिक्षा विभाग की भूमिका की चर्चा करना उपयुक्त होगा। दुर्भाग्यवश, वे शिक्षक-शिक्षण में ही इतने तल्लीन हैं कि वे शैक्षणिक शोध में योगदान देना ज़रूरी नहीं समझते। बल्कि कुछ हद तक तो शोध के प्रति प्रतिबद्धता शिक्षण के लिए हानिकारक मानी जाती है। नीति-अध्ययनों और पाठ्य पुस्तक विश्लेषण में कुछ गुणवत्तापूर्ण कार्य किया जा रहा है पर कक्षाई शोध-अध्ययन और शैक्षणिक शोध-अध्ययन या तो न के बराबर हैं या फिर उनका स्तर काफी निम्न है। समस्या यह है कि ज़रूरी सन्दर्भ सामग्री के अभाव के चलते शिक्षक-शिक्षण भी प्रभावित होता है। इस स्थिति के पीछे कई समस्याएँ हैं - ऐसी सोच जो शिक्षक प्रशिक्षकों को शोध का महत्व समझने की सुविधा नहीं देती, इन कार्यक्रमों का कमज़ोर ढाँचा जहाँ फैकल्टी को स्कूलों में चल रहे शोधकार्यों में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती। यह एक गहरी दरार है क्योंकि इस क्षेत्र में ज्ञान-निर्माण करने में विश्वविद्यालयों की अहम भूमिका है।
शिक्षक शिक्षण - साक्षरता शिक्षण
हाल में, इस धारणा को चुनौती मिली है कि बच्चे प्रेरणा की कमी और पालकों के सहयोग की कमी के चलते स्कूल छोड़ देते हैं और बुरा प्रदर्शन करते हैं। अब बच्चों के स्कूल में न टिक पाने के कारण के तौर पर स्कूली कारकों की पड़ताल हो रही है। यह बदलाव स्वागत योग्य है क्योंकि यह शिक्षा में बच्चों के प्रदर्शन के लिए ज़िम्मेदार एक बेहद महत्वपूर्ण कारक की पहचान करता है। लेकिन, हो सकता है कि यह माना जाए कि इस परिवर्तन का निहितार्थ शिक्षकों पर दोषारोपण करना है। यह उचित नहीं होगा क्योंकि वाचन के क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा प्रदान किए गए विशेष ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करना ज़रूरी है। भारत में स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ पढ़ना सिखाने के लिए बमुश्किल ही कोई पृथक पाठ्यक्रम है और बैचलर ऑॅफ ऐलीमेन्ट्री ऐजुकेशन (बी.ईएल.एड.) जैसा अभिनव कार्यक्रम भी इन ज़रूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं करता। ऐसे विचारों व योजनाओं को न आज़माने के लिए शिक्षकों की भी आलोचना नहीं की जा सकती जिनसे वे खुद ही अपरिचित हैं।
इसके अलावा, जैसी कि पहले भी चर्चा की गई है, हमारे यहाँ शैक्षणिक सिद्धान्त-निर्माण और शोध नहीं हो रहे हैं। विद्यार्थी सिद्धान्तों का व्यापक दृष्टि से अध्ययन करते हैं और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं ही उनका कक्षाई उपयोग तलाशें। इस दरार को भर पाना आसान नहीं है, अत: अधिकांशत: वे परिचित पारम्परिक प्रचलनों पर ही निर्भर हो जाते हैं। यह अच्छी तरह से तलाशना ज़रूरी है कि कक्षा के सन्दर्भ में इन सिद्धान्तों का क्या अर्थ है। अत: शिक्षक प्रशिक्षण द्वारा शिक्षकों को हासिल होने वाले ज्ञान को लेकर और ज़्यादा चर्चाएँ किए जाने की ज़रूरत है। इस तरह की चर्चा अभी शु डिग्री ही नहीं हुई है।
निष्कर्ष
इस पूरी चर्चा से यह स्पष्ट है कि भारत में साक्षरता शिक्षण की स्थिति बहुत निराशाजनक है जिसके पीछे अन्य कारणों के अलावा कमज़ोर शैक्षणिक पद्धतियाँ और शोध की कमी प्रमुख कारण हैं। इन क्षेत्रों की लम्बे समय से अनदेखी की गई है, भले ही भारत में साक्षरता के बारे में काफी परवाह की जाती हो।
इस लेख की शुरुआत में हुई चर्चा से यह स्पष्ट है कि साक्षरता के बारे में यांत्रिकी ज्ञान सशक्तिकरण या विकास की शक्ल अख्तियार नहीं करता। जैसा कि नरसिम्हन ने बताया है, साक्षरता को सामाजिक सेवा से परे जाने की ज़रूरत है और उसे मूल्यवान पेशेवर ज्ञान का संग्रह विकसित करने की आवश्यकता है। इसलिए, साक्षरता हासिल करने-कराने की प्रक्रिया में सार्थक ढंग से लगे रहने की और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तथा सुविज्ञ शैक्षणिक प्रक्रियाएँ विकसित करने की बेहद ज़रूरत है।
शोभा सिन्हा: दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग में रीडर हैं। इनकी रुचि के शोध-विषय हैं: बढ़ती साक्षरता, साहित्य के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया, कक्षा के सन्दर्भ में साक्षरता का अर्थ और निम्न सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का साक्षरता-सम्बन्धी विकास।
अँग्रेज़ी से अनुवाद: भरत त्रिपाठी: पत्रकारिता की पढ़ाई। स्वतंत्र लेखन और द्विभाषिक अनुवाद करते हैं। होशंगाबाद में निवास।
सभी चित्र: बोस्की जैन: सिम्बायोसिस ग्राफिक्स एण्ड डिज़ाइन कॉलेज, पुणे से ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में स्नातक। मध्य भारत के गोंड क्षेत्र की आदिवासी कला के अध्ययन में विशेष रुचि। भोपाल में निवास।
मूल लेख सेज प्रकाशन, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2002 में प्रकाशित पुस्तक ‘एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट’ से साभार।
लेख में उपयोग किए गए सन्दर्भों के लिए कृपया मूल पुस्तक देंखें।

