उदयन वाजपेयी
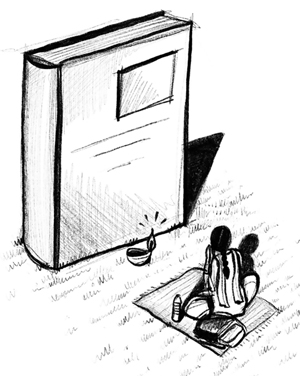 एक छोटी-सी स्वीकारोक्ति से अपनी बात शुरु करना चाहता हूँ। यह विषय कई दिनों से मेरे दिमाग में था। इसके बड़े ही निजी कारण थे। मैं जब भी अपने आसपास के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के कारण घरवालों के हाथों प्रताड़ित होते देखता तो रह-रह एक प्रश्न मेरे मन में घूमने लगता : आखिर इन्हें किस अपराध के लिए सताया जा रहा है? और इसी रास्ते मैं पाठ्यपुस्तक पर विचार करने तक आया। आम तौर पर हम अपनी बेहद आत्मीय समस्या को समझते-समझते किन्हीं सामाजिक संकटों को समझने तक पहुँच जाते हैं। पाठ्यपुस्तक पर मैं कई दिनों से सोच रहा था और मैंने बड़े उत्साह से खुद यह विषय चुना था। मैं सोचता था, सब सोचा हुआ है, यहाँ मैं बैठा और लेख तैयार हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जैसे ही कुछ लिखना शुरु करता, मुझे इस विषय के भीतर से मेरे प्रवेश के विरुद्ध कुछ प्रतिरोध महसूस होता और मैं ठहर जाता।
एक छोटी-सी स्वीकारोक्ति से अपनी बात शुरु करना चाहता हूँ। यह विषय कई दिनों से मेरे दिमाग में था। इसके बड़े ही निजी कारण थे। मैं जब भी अपने आसपास के बच्चों को स्कूल की पढ़ाई के कारण घरवालों के हाथों प्रताड़ित होते देखता तो रह-रह एक प्रश्न मेरे मन में घूमने लगता : आखिर इन्हें किस अपराध के लिए सताया जा रहा है? और इसी रास्ते मैं पाठ्यपुस्तक पर विचार करने तक आया। आम तौर पर हम अपनी बेहद आत्मीय समस्या को समझते-समझते किन्हीं सामाजिक संकटों को समझने तक पहुँच जाते हैं। पाठ्यपुस्तक पर मैं कई दिनों से सोच रहा था और मैंने बड़े उत्साह से खुद यह विषय चुना था। मैं सोचता था, सब सोचा हुआ है, यहाँ मैं बैठा और लेख तैयार हुआ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं जैसे ही कुछ लिखना शुरु करता, मुझे इस विषय के भीतर से मेरे प्रवेश के विरुद्ध कुछ प्रतिरोध महसूस होता और मैं ठहर जाता।
वैसे तो हर किताब दूसरी किताब से अलग होती है, लेकिन तब भी आखिर किताब होती तो किताब ही है। मुझे प्रवेश क्यों नहीं मिल रहा? पाठ्यपुस्तक में ऐसी क्या बात है कि उस पर बात शुरु करना इतना मुश्किल जान पड़ रहा है? अगर उपन्यास होता तो मैं उसके पात्रों के वर्णन से शुरु करता या किसी एक संवाद पर विचार करना शुरु करता और धीरे-धीरे सारा उपन्यास इस एक सूत्र के सहारे खुलने लगता। जब मैंने और ध्यान लगाया तब मुझे लगा कि मुझे अन्दर से कुछ भय-सा मालूम दे रहा है : इस भय का एक कारण तो मैं जानता हूँ कि मैं इस विषय का स्कॉलर नहीं हूँ। लेकिन आखिर मैंने इतने दिनों इस पर सोचा है, तब मुझे यह भय क्यों? मुझे कुछ विचित्र-सा ज़रूर लगा लेकिन तभी मुझे लगा कि यह भय उस भय से मिलता-जुलता है, जो मुझे तब होता था जब मैं रसोईघर में चप्पल पहनकर घुस जाता था। कुछ वैसा डर जो कुछ अपवित्र करने से होता है। क्या पाठ्यपुस्तक पर सोचना कुछ अपवित्र करना है? इसलिए मैंने सोचा कि पवित्र और अपवित्र की श्रेणियों को समझने से ही पाठ्यपुस्तक को समझने की शुरुआत करनी चाहिए।
एक भारतीय विचारक का मानना है कि यह विभाजन पश्चिम के इसी तरह के विभाजन का अनुवाद है। उनका कहना है कि पवित्र और अपवित्र, जैसा कि उन्हें हम बरतने लगे हैं, ‘सेक्रेड’ और ‘प्रोफेन’ के अनुवाद हैं। प्राचीनकाल में हमारे देश में ईशनिन्दा जैसी कोई अवधारणा ही नहीं थी। ईश्वर की निन्दा करना और उनकी प्रार्थना करना एक-दूसरे के विपरीत कर्म नहीं माने जाते। वेद पवित्र है न अपवित्र। इसका सबसे बढ़िया साक्ष्य यह है कि वेदों को न मानने वाले नास्तिक बौद्धों पर प्रश्न तो कई उठाए गए हैं लेकिन उन्हें नेस्तनाबूद नहीं कर दिया गया। यह नहीं कि उनका नास्तिक होना सहज स्वीकार कर लिया गया हो, लेकिन उनके इस अविश्वास को किन्हीं ‘एब्सोल्यूट’ सन्दर्भों में नहीं देखा गया। ‘एब्सोल्यूट’ सन्दर्भों का अर्थ यह है कि उन्हें हमेशा के लिए तिरस्कृत नहीं कर दिया गया। हालाँकि, यह कहा गया कि वे भटक गए हैं, जैसे कि जैन मत के लोगों के विषय में भी शुरू-शुरु में समझा गया होगा, लेकिन उन्हें अपराधी नहीं ठहराया गया, काफिर नहीं कहा गया या अगर कहा भी गया तो किन्हीं भी ‘एब्सोल्यूट टर्म्स’ में ऐसा नहीं किया गया, वरना आज बौद्ध और जैन मतावलम्बियों को इस देश में ऐसा सम्मानजनक स्थान प्राप्त न होता।
इससे हम अपनी खोज की कम-से-कम एक दिशा तो पा ही सकते हैं कि अगर कोई पुस्तक अपने होने को, अपने अस्तित्व को पवित्र और अपवित्र के सन्दर्भ में परिभाषित करती हो तो हमें उसके स्रोत पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। हमारे पास यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि वह इस देश में कहीं बाहर से आई होगी। और तब हमें यह निश्चय ही सोचना चाहिए कि यह पुस्तक आई कहाँ से है। कम-से-कम तब तो अवश्य ही जब हम यह मान रहे हों कि वह हमेशा से नहीं थी। हमारे पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसके आधार पर हम कह सकें कि पाठ्यपुस्तक हमेशा से थी। इस तरह के किसी शब्द का प्रयोग हमारे प्राचीन शास्त्र में आया हो, ऐसा मेरी जानकारी में नहीं। अगर पाठ्यपुस्तक हमेशा से ही अस्तित्व में नहीं थी तो वह अस्तित्व में कहाँ से आई?
पवित्र और अपवित्र की ‘एब्सोल्यूट’ श्रेणियाँ ईसाई धार्मिक विश्वास से आई हैं। ‘सेक्रेड’ और ‘प्रोफेन’ शब्दों का ईसाई धार्मिक विश्वास से गहरा सम्बन्ध है। इसीलिए ईसाइयत के इस लक्षण को समझकर ही हम पाठ्यपुस्तक की उससे निकटता को समझ सकेंगे। इन्हीं श्रेणियों के होने के कारण ईसाइयत में बाइबिल एक ‘पवित्र’ ग्रन्थ माना जाता है जैसे इस्लाम में कुरान को। ये पवित्र ग्रन्थ पवित्र स्थानों की शोभा बनते थे और बनते हैं। गिरजों या मस्जिदों में इनका पाठ होता था और होता है। पुनर्जागरण का पहला लक्षण यह था कि (सोलहवीं शती में आकर) पश्चिम के मनुष्य ने पवित्र के विरुद्ध ‘धर्म निरपेक्ष’ को स्थापित करने की शुरुआत की; ‘सेक्रेड’ का स्थान ‘सेक्युलर’ ने लेना शुरु किया।
‘पवित्र’ का स्थान ‘धर्म निरपेक्ष’ ने लिया ज़रूर लेकिन यह विस्थापन चूँकि अनिवार्यत: द्वन्द्व पर आश्रित था, याने ‘सेक्रेड’ के विरुद्ध ‘सेक्युलर’ को रखा गया था इसलिए ‘सेक्युलर’ चिन्तन में ‘सेक्रेड’ चिन्तन के बहुत सारे लक्षण अपने उलटे रूप में सुरक्षित रहे आए। आप चाहें तो कह सकते हैं कि ‘सेक्युलर’ चिन्तन ‘सेक्रेड’ चिन्तन की प्रति-कृति की तरह अस्तित्व में आया। यह प्रति-कृति ठीक-ठीक अपनी कृति की तरह नहीं थी; उसमें कुछ महत्वपूर्ण अन्तर भी थे लेकिन इन अन्तरों के साथ, उसमें कुछ समानताएँ भी निश्चय ही थीं। समकालीन ग्रीक कवि तासोस डेनिग्रीस की कुछ पंक्तियाँ इस स्थिति पर सटीक टिप्पणी हो सकती हैं : तुम किसी से नफरत करते हो और उसकी नकल करना तुम्हारा हश्र होता है, “यू हेट समथिंग एण्ड यू एण्ड अप इमिटेटिंग इट”। लगभग ऐसी ही स्थिति पुनर्जागरण के बाद पश्चिम में बनी होगी। पुनर्जागरण ने कुछ हद तक पुनर्जागरण के पहले के चिन्तन का अनुकरण किया। धर्म निरपेक्ष चिन्तन पर पश्चिमी धार्मिक चिन्तन की गहरी छाया मौजूद थी। पवित्र पुस्तक का अब वह स्थान नहीं रह गया जो पहले था और चूँकि पवित्रता का केन्द्र यही पवित्र पुस्तक थी, बल्कि यूँ कहें कि इस पुस्तक के आधार पर ही पवित्रता और अपवित्रता की श्रेणियाँ तैयार की जाती थीं, इसलिए इसे किसी धर्म निरपेक्ष पुस्तक से विस्थापित करना अनिवार्य मालूम दिया। जो पुस्तक इस विस्थापन के नतीजे में आई, वह थी पाठ्यपुस्तक।
इन दोनों पुस्तकों में जो भेद हैं, उनकी बात हम बाद में करेंगे लेकिन एक बुनियादी साम्य हम स्पष्टत: देख सकते हैं : बाइबिल हर ईसाई के लिए ज़रूरी है और पाठ्यपुस्तक प्रत्यय में ही यह निहित है कि यह वह पुस्तक है जिसे पढ़ा ही जाना चाहिए। हम इस तरह की बात किसी उपन्यास या कहानियों की या कविताओं की किताब के सन्दर्भ में नहीं कर सकते, कम-से-कम तब तक तो नहीं ही, जब तक वह किताब ‘पाठ्यपुस्तक’ की उपाधि प्राप्त नहीं कर लेती। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी अन्तिम व्याख्या पवित्र पुस्तक में मिलती थी, न्यू टेस्टामेण्ट के ‘दस कमांडमेंट्स’ इसका उदाहरण हैं। पुनर्जागरण के बाद यह बताने का काम पाठ्यपुस्तक को सौंपा गया कि जीवन कैसे अस्तित्व में आया, क्या विकास हुआ और इस सबके नतीजे के तौर पर नागरिकों को क्या करना चाहिए, उनके क्या दायित्व हैं। यह उसमें एक बार में बाइबिल की तरह अन्तिम रूप से आ गया हो, ऐसा नहीं है। इस मायने में पाठ्यपुस्तक पवित्र-पुस्तक से भिन्न है। पवित्र-पुस्तक में जो एक बार आया, सो आया। पवित्र-पुस्तक ज्ञान के विस्तार की अवधारणा पर या तो विश्वास नहीं करती और अगर करती है तो इस तरह कि सारे ज्ञान का सारा विस्तार अन्तत: जहाँ ले जाता है, वह ज्ञान पवित्र-पुस्तक में पहले से ही सुरक्षित है। लेकिन पाठ्यपुस्तक के संस्करण होते हैं। उसमें हर साल परिवर्तन होते हैं, कुछ नया जुड़ता है, कुछ पुराना हटाया जाता है लेकिन अपने हर संस्करण में पाठ्यपुस्तक ठीक वैसे ही बरताव करती है जैसे वह पवित्र-पुस्तक हो। उसके हर संस्करण को इस तरह पढ़ा जाता है जैसे वह अन्तिम हो। इसी बात को हम और भी विस्तार से कहें तो कह सकते हैं कि अगर एक शिक्षक किसी पाठ्यपुस्तक का छठा संस्करण पढ़ा रहा हो तो उसे वह इस तरह पढ़ाएगा, या पाठ्यपुस्तक पढ़ाए जाने की शर्त ही यह है कि उसे ऐसा पढ़ाया जाए, जैसे वह अपने में पूर्ण है, अन्तिम है। यह बात हम अलग से क्यों न जानते हों कि इसके इस संस्करण के आगे भी कई संस्करण आएँगे इसलिए इसमें जो भी लिखा है वह अपने में अस्थायी है, परिवर्तनशील है और अन्तिम नहीं है। लेकिन पाठ्यपुस्तक की अपनी बनावट के कारण उसे पढ़ाते वक्त यह भुलावा शिक्षक और विद्यार्थी में उत्पन्न हो जाता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। इसका कारण शिक्षक का अच्छा-बुरा होना उतना नहीं है जितना पाठ्यपुस्तक की अपनी अवधारणा है। उसे प्रस्तुत ही इस तरह किया जाता है कि वह पवित्र-पुस्तक की तरह पढ़ाई जा सके।
यह उसमें एक बार में बाइबिल की तरह अन्तिम रूप से आ गया हो, ऐसा नहीं है। इस मायने में पाठ्यपुस्तक पवित्र-पुस्तक से भिन्न है। पवित्र-पुस्तक में जो एक बार आया, सो आया। पवित्र-पुस्तक ज्ञान के विस्तार की अवधारणा पर या तो विश्वास नहीं करती और अगर करती है तो इस तरह कि सारे ज्ञान का सारा विस्तार अन्तत: जहाँ ले जाता है, वह ज्ञान पवित्र-पुस्तक में पहले से ही सुरक्षित है। लेकिन पाठ्यपुस्तक के संस्करण होते हैं। उसमें हर साल परिवर्तन होते हैं, कुछ नया जुड़ता है, कुछ पुराना हटाया जाता है लेकिन अपने हर संस्करण में पाठ्यपुस्तक ठीक वैसे ही बरताव करती है जैसे वह पवित्र-पुस्तक हो। उसके हर संस्करण को इस तरह पढ़ा जाता है जैसे वह अन्तिम हो। इसी बात को हम और भी विस्तार से कहें तो कह सकते हैं कि अगर एक शिक्षक किसी पाठ्यपुस्तक का छठा संस्करण पढ़ा रहा हो तो उसे वह इस तरह पढ़ाएगा, या पाठ्यपुस्तक पढ़ाए जाने की शर्त ही यह है कि उसे ऐसा पढ़ाया जाए, जैसे वह अपने में पूर्ण है, अन्तिम है। यह बात हम अलग से क्यों न जानते हों कि इसके इस संस्करण के आगे भी कई संस्करण आएँगे इसलिए इसमें जो भी लिखा है वह अपने में अस्थायी है, परिवर्तनशील है और अन्तिम नहीं है। लेकिन पाठ्यपुस्तक की अपनी बनावट के कारण उसे पढ़ाते वक्त यह भुलावा शिक्षक और विद्यार्थी में उत्पन्न हो जाता है कि इसके आगे कुछ नहीं है। इसका कारण शिक्षक का अच्छा-बुरा होना उतना नहीं है जितना पाठ्यपुस्तक की अपनी अवधारणा है। उसे प्रस्तुत ही इस तरह किया जाता है कि वह पवित्र-पुस्तक की तरह पढ़ाई जा सके।
लेकिन संस्करणों के भेद के कारण हम जानते हैं कि वह असली पवित्र-पुस्तक नहीं है, सिर्फ पवित्र-पुस्तक होने का स्वाँग कर रही है। क्या हम पाठ्यपुस्तक को एक ‘मिथ्या पवित्र-पुस्तक’ कह सकते हैं? अगर हम इसी फर्क का कुछ और देर पीछा करें तो कुछ और बातें भी शायद सामने आएँ।
पवित्र-पुस्तक का कोई लेखक नहीं होता। उसे इस तरह नहीं पढ़ा जाता कि इसे किसी मनुष्य ने लिखा होगा। पवित्र-पुस्तक के विषय में यह माना जाता है कि यह प्रकट होती है, किसी देवता की तरह। स्वर्ग में या अर्श पर लिखी कुरान ही फर्श पर या ज़मीन पर पैगम्बर के माध्यम से प्रकट होती है। उसका ‘द्रष्टा’ होता है, ‘लेखक’ नहीं। लेखक तो ईश्वर है। ऐसा कैसे होता है, यह तो मान्यता का प्रश्न है इसलिए इसे हम छोड़ दें, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पढ़ा इस तरह जाता है जैसे वह ईश्वर की कृति हो। उसका एक-एक शब्द उसके पाठक के मन में ईश्वर की ओर से आई अमृत की बूँद की तरह टपकता है। पवित्र-पुस्तक का कोई भी लेखक अगर रहा भी हो तो वह अपने कृतित्व को इस तरह बरतता है जैसे वह कृतित्व उसका नहीं, वह तो उसे ईश्वर से पाठक तक बल्कि भक्त तक ले जाने का माध्यम-भर बना है। पवित्र-पुस्तक के लेखक का अपने को इस तरह बरतना और उसके पाठक का उसे इस तरह पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है। हम यह कह सकते हैं कि पवित्र-पुस्तक को इस तरह पढ़ा और लिखा जाता है जैसे वह किसी अलौकिक आकांक्षा या ‘कॉस्मिक इंटेन्शन’ का परिणाम हो।
अब हम अपनी इस मिथ्या-पवित्र-पुस्तक या पाठ्यपुस्तक को देखें। क्या हम कह सकते हैं कि बावजूद इसके कि इसे पवित्र-पुस्तक की तरह बरता जाता है, इसका लेखक यह मानकर लिखता है कि वह ईश्वर की आकांक्षा को या ईश्वर के कृतित्व को मनुष्यों के लिए पृथ्वी पर उतार रहा है? हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। वह यह मानकर बिलकुल नहीं लिखता कि वह ईश्वर का माध्यम है। पाठ्यपुस्तक की तो बाकायदा योजना और नीति बनती है, उसे लिखने वाले का नाम भी उस पर छापा जाता है लेकिन उसे पढ़ते वक्त हम उसमें लिखे पाठ को इस तरह पढ़ते हैं जैसे वह किसी लेखक के मानस से उपजे न होकर किसी आलौकिक आकांक्षा के वाहक हों। हम यह भुला देते हैं कि उसका जो भी लेखक है, उसका एक सीमित विवेक है जो इन पुस्तकों को तैयार करता है।
पवित्र-पुस्तक की तरह का कोई केन्द्रीय ग्रन्थ प्राचीन भारत में कभी नहीं रहा। आप औपनिषदिक ग्रन्थों, भगवद्गीता, रामायण -- किसी को भी उन अर्थों में पवित्र-ग्रन्थ नहीं कह सकते जिन अर्थों में आप, मसलन, बाइबिल को पवित्र-ग्रन्थ कहते हैं। पवित्र-ग्रन्थ वह ग्रन्थ है जिसके साथ ‘कौतुक’ सम्भव नहीं, जिसके साथ आप खेल का रिश्ता नहीं बना सकते। लेकिन प्राचीन भारत के असंख्य पुराण इन ग्रन्थों से कौतुक के रिश्ते के कारण ही लिखे गए हैं। और यहीं से हम पाठ्यपुस्तक के हमारे देश की शिक्षा पर पड़े प्रभाव को देख सकते हैं। पाठ्यपुस्तक इस देश की परम्परा का उत्पाद मालूम नहीं देती। हमारे देश में कभी भी किसी एक ग्रन्थ को केन्द्र में रखकर शिक्षा नहीं दी गई। जब अँग्रेज़ हमारे देश में आए तो वे हमें शिक्षित करना चाहते थे और शिक्षा का अर्थ उनके लिए किसी एक ग्रन्थ को या कुछ ग्रन्थों को केन्द्र में रखकर शिक्षा देने का था। वे जहाँ से आए थे, वहाँ पुस्तक ‘एक’ ही थी और उसे जानना ही ज्ञान हासिल करना था। एक किताब और एक ईश्वर के देश से वे आए थे। यहाँ आकर जब उन्होंने तैंतीस करोड़ देवी-देवता देखे तो उन्हें एक पुस्तक को केन्द्र में रखकर शिक्षा देने की ज़रूरत और भी शिद्दत से महसूस हुई होगी। और इसलिए उन्होंने हमारे ऊपर पाठ्यपुस्तक को आरोपित किया।
ऐसा करने के पीछे उनके पास कुछ दूसरे कारण भी थे। वे जिस तरह के लोग अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और अन्य व्यापार चलाने के लिए चाहते थे, उसके लिए उन्हें एक तरह की पाठ्यपुस्तक बनाना ज़रूरी लगा, वह योजना आज तक चली आ रही है क्योंकि उस पर विस्तार से शिक्षाविदों तक ने विचार नहीं किया। वह योजना थी हमारे देश की मनीषा को, हमारे देश के ज्ञान-व्यापार को हमारे लिए ही अजनबी बना देना। उसे इस हद तक अजनबी बना देना कि यह ज्ञान स्वयं हमें ही अवास्तविक लगने लगे। जैसे-जैसे हमारी शिक्षा पाठ्यपुस्तक के चारों ओर बसती चली गई वैसे-वैसे हमारी अपनी मनीषा खुद हमारे लिए ही अवास्तविक होती गई। पाठ्यपुस्तक काल में इस मनीषा का तिरस्कार करना भी शिक्षित होने का एक अर्थ हो गया। इसका एक बड़ा सीधा-सा उदाहरण यह है कि वे सारे पौराणिक ग्रन्थ या वे सारे ग्रन्थ जिन्हें पौराणिक शैली में आज के उन भारतीय विद्वानों ने लिखा है जो शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रहकर काम करते हैं, उन्हें हम और हमारे विद्यार्थी अज्ञानपूर्ण पाएँ या न पाएँ लेकिन हमें वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। और चूँकि हम इन ग्रन्थों को वास्तविक नहीं मानते इसलिए इन ग्रन्थों के विषय में सोचना-समझना हमें ज़रूरी नहीं लगता। भारत के सन्दर्भ में पाठ्यपुस्तक एक ऐसा चौकोर लक्ष्मण घेरा है जिसके अन्दर जो भी गया, वह वास्तविक और जो छूट गया, वह अवास्तविक। साहित्य के अध्यापन में यह भेद और अधिक तीखा हो जाता है। कुछ लेखकों की कुछ कृतियाँ पाठ्यपुस्तकों में हैं, उन्हें विद्यार्थी बचपन से पढ़ते हैं और मानने लगते हैं कि वास्तविक कृतियाँ यही हैं, फिर अगर वे किन्हीं अन्य लेखकों की कृतियाँ अन्य पुस्तकों में पढ़ भी लें और वे उनसे आनन्दित भी हों, तब भी चूँकि ये दूसरी पुस्तकें पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं इसलिए छात्रों को वे कम या बिलकुल अवास्तविक जान पड़ती हैं। वे उन किताबों को पराई मानकर पढ़ते हैं और धीरे-धीरे इन अद्भुत किताबों के लिए स्वयं पराए हो जाते हैं।
इसका एक बड़ा सीधा-सा उदाहरण यह है कि वे सारे पौराणिक ग्रन्थ या वे सारे ग्रन्थ जिन्हें पौराणिक शैली में आज के उन भारतीय विद्वानों ने लिखा है जो शैक्षणिक संस्थानों से बाहर रहकर काम करते हैं, उन्हें हम और हमारे विद्यार्थी अज्ञानपूर्ण पाएँ या न पाएँ लेकिन हमें वे वास्तविक नहीं जान पड़ते। और चूँकि हम इन ग्रन्थों को वास्तविक नहीं मानते इसलिए इन ग्रन्थों के विषय में सोचना-समझना हमें ज़रूरी नहीं लगता। भारत के सन्दर्भ में पाठ्यपुस्तक एक ऐसा चौकोर लक्ष्मण घेरा है जिसके अन्दर जो भी गया, वह वास्तविक और जो छूट गया, वह अवास्तविक। साहित्य के अध्यापन में यह भेद और अधिक तीखा हो जाता है। कुछ लेखकों की कुछ कृतियाँ पाठ्यपुस्तकों में हैं, उन्हें विद्यार्थी बचपन से पढ़ते हैं और मानने लगते हैं कि वास्तविक कृतियाँ यही हैं, फिर अगर वे किन्हीं अन्य लेखकों की कृतियाँ अन्य पुस्तकों में पढ़ भी लें और वे उनसे आनन्दित भी हों, तब भी चूँकि ये दूसरी पुस्तकें पाठ्यपुस्तकें नहीं हैं इसलिए छात्रों को वे कम या बिलकुल अवास्तविक जान पड़ती हैं। वे उन किताबों को पराई मानकर पढ़ते हैं और धीरे-धीरे इन अद्भुत किताबों के लिए स्वयं पराए हो जाते हैं।
किसी भी पुस्तक की बनावट उसके पठन के नियमों पर भी निर्भर होती है। यह पुस्तक की बनावट का ही हिस्सा है कि उसे किस तरह पढ़ा जाए। हम किसी भी पुस्तक को अपनी शर्तों पर नहीं, उस पुस्तक की शर्तों पर पढ़ते हैं। प्रश्न है कि पाठ्यपुस्तक को क्या वैसे ही पढ़ा जा सकता है जैसे मसलन दोस्तोएव्स्की के उपन्यासों को? अगर नहीं तो फिर इनके पढ़ने में क्या फर्क है और उस फर्क का क्या आधार है? जब हम दोस्तोएव्स्की का उपन्यास ‘अपराध और दण्ड’ पढ़ते हैं तो हम लगातार उपन्यास से संवाद या बहस करते चलते हैं। कई बार हमें उपन्यास सन्तुष्ट करता है, कई बार नहीं कर पाता। लेकिन उपन्यास को पढ़ने की शर्त ही यह है कि आप उसमें शामिल हों। वह एक ऐसा खेल रचता है जो पाठक के शामिल हुए बिना पूरा नहीं हो सकता। उसे आप लेन-देन के सम्बन्ध में नहीं घटा सकते। उपन्यास में हमेशा ही पाठक का स्थान सुरक्षित रहता है। यही बात महाभारत जैसे ग्रन्थों के विषय में भी कही जा सकती है। इससे ठीक उलटा पाठ्यपुस्तक का पठन है। पाठ्यपुस्तक पढ़ने की यह शर्त है कि आप उससे संवाद न करें। वह उपदेशात्मक पुस्तक है जो पाठक को अपने होने के खेल में शामिल नहीं करती। उसका पाठक पाठ्यपुस्तक के बाहर खड़ा ठिठुरता रहता है, सिर्फ बीच-बीच में कुछ बनी-बनाई अवधारणाएँ उसकी झोली में गिरती रहती हैं। उससे संवाद सम्भव नहीं। वह अपने एकालाप में ही जीवित रहती है। उसे पढ़ने का ढंग यह है कि आप उसे ‘याद’ कर लें। पाठ्यपुस्तक के विषय में इसीलिए कोई भी राय उस तरह नहीं हो सकती जैसी कि उपन्यासों के बारे में होती है। आप यह नहीं कह पाते कि पाठ्यपुस्तक की यह धारणा गलत है, तर्कहीन है जैसा कि आप अन्य पुस्तकों के विषय में कहने को स्वतंत्र हैं। पाठ्यपुस्तक अपने पाठक को उपदेशात्मक एकालाप में ही बताती है कि सृष्टि, जीवन, प्रकृति आदि को कैसे देखा जाए। उसमें पाठक की एक स्वतंत्र विचार-सृष्टि की कल्पना नहीं है। इसीलिए पाठ्यपुस्तक में उसे पढ़ते हुए असहमति या बहस का कोई स्थान नहीं है।
काफी हद तक इसका कारण हमारे शैक्षणिक संस्थान हैं जिन्हें हम आधुनिक गिरजे कह सकते हैं, जहाँ पाठ्यपुस्तकों को अन्तिम साक्ष्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इन गिरजों का इस तरह होना भी पाठ्यपुस्तक की बनावट का एक अंग है क्योंकि पाठ्यपुस्तक तभी तक पाठ्यपुस्तक है जब तक इस तरह के शैक्षणिक संस्थान हों। शैक्षणिक संस्थाएँ हैं ही इस तरह कि उनमें पाठ्यपुस्तक को पाठ्यपुस्तक की शर्तों पर पढ़ाया जा सके। पाठ्यपुस्तक तभी तक असामान्य पुस्तक है जब तक उस पर अलग से विचार नहीं किया जाता, और जब तक वह इन संस्थानों की चहारदीवारियों में अपने एकालापों में सुरक्षित बनी है।
आज की शिक्षा का आधार संस्थानिक आकांक्षा है, शिष्य की जिज्ञासा नहीं। इसलिए जीवन-मृत्यु से जुड़े, अस्तित्व से जुड़े प्रश्नों की इन पाठ्यपुस्तकों में कोई अनुगूंज नहीं है। कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी आबादी को सम्भालने को ज्ञान की नहीं, कौशल की आवश्यकता है इसलिए संस्थानों को ऐसा होना ज़रूरी है। लेकिन क्या जो भी शिक्षा इन कारणों से छात्रों को दी जाती है, उसे ज्ञान कहकर नहीं दिया जाता? यहाँ अनैतिक यह नहीं कि संस्थाओं की आकांक्षा शिक्षा का आधार है, अनैतिक यह है कि इसे लगातार छिपाकर रखा जाता है। जैसे ही शिष्य की जिज्ञासा उसके ज्ञान का आधार बनेगी, तमाम पाठ्यपुस्तकें अपने-आप विलुप्त हो जाएँगी क्योंकि पाठ्यपुस्तक की बनावट की एक शर्त यह भी है कि वह अपने पाठक की जिज्ञासाओं को नियंत्रित करे। लेकिन जैसे ही शिष्य की आकांक्षाएँ अनियंत्रित होंगी, बँधी-बँधाई न होंगी, वैसे ही उसके समाधान की यह पोटली, पाठ्यपुस्तक, निस्सार हो जाएगी। पाठ्यपुस्तक तब तक बनी रहेगी जब तक छात्र की अपनी जिज्ञासाओं को हमारी शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं मिल जाता। हमें इस बात से शायद दुखी हो सकना चाहिए कि पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों को इतनी कम उम्र से ही पढ़ाई जाना आरम्भ कर दी जाती हैं कि वह अपनी जिज्ञासाओं को अन्त तक पहचान नहीं पाता। उसकी जगह वह अपने भीतर उन मिथ्या प्रश्नों को जगह दे देता है जिसके बँध-बँधाए उत्तर पाठ्यपुस्तकों में पहले से ही उपलब्ध रहते हैं।
इसी के बरअक्स आप औपनिषदिक शिक्षा का मॉडल देखें तो आधुनिक शिक्षा-पद्धति का आध्यात्मिक खोखला-पन बुरी तरह उजागर हो जाएगा। औपनिषदिक शिक्षा-व्यवस्था में सारा ज्ञान व्यापार शिष्य के प्रश्न पर टिका होता है। यहाँ गुरु किसी पुस्तक का एजेण्ट नहीं है, न कोई ग्रन्थ उसे यह बन जाने की अनुमति ही देता है। शिष्य का प्रश्न गुरु को जहाँ-जहाँ ले जाता है, वहाँ-वहाँ गुरु जाता है। दोनों के जाने में फर्क सिर्फ इतना है कि वहाँ जो कुछ अनुभव हो रहा है, उसे गुरु कह पा रहा है। दोनों मिलकर ज्ञान की खोज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि शिष्य को लगातार लग रहा है कि एक ऐसा वक्त आएगा जब उसकी खोज खत्म हो सकेगी लेकिन गुरु जानता है कि चलना या भटकना ही अपने में ज्ञान की बुनावट का हिस्सा है। जैसे ही शिष्य को यह अनुभव होगा कि ज्ञान की खोज ही ज्ञान का मिलना है, उसे ‘ज्ञान’ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह वहाँ गुरु शिष्य को प्रश्न सुलझाना नहीं, प्रश्न सहना सिखाता है। क्योंकि जैसे कि हाइडेगर मानते थे, मनुष्य के सत्व का स्वरूप प्रश्न ही है, द एसेन्स ऑव मेन इज़ द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। इसलिए सवाल इसे सुलझाने का नहीं, इसे सहने का है। इसे निरन्तर आविष्कृत करने का है।
उदयन वाजपेयी: हिन्दी के कवि, निबन्धकार, उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं। आपके कविता संग्रह, लघु कहानियों का संग्रह व कई निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी रचनाओं का बांग्ला, तमिल, उड़िया, कन्नड़, अँग्रेज़ी, फ्रेंच, स्वीडिश, पोलिश और बल्गेरियन भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। रज़ा फाउण्डेशन पुरस्कार, कृष्ण बलदेव वैद पुरस्कार से सम्मानित। साथ ही, आप गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में फिज़ियोलॉजी पढ़ाते हैं।
सभी चित्र: अंकिता ठाकुर: राष्ट्रीय डिज़ाइन संस्थान, अहमदाबाद से ग्राफिक डिज़ाइन में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रही हैं। बाल साहित्य और चित्रों में दिलचस्पी रखती हैं।
यह लेख राजकमल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उदयन वाजपेयी के निबन्ध संग्रह चरखे पर बढ़त और अन्य निबन्ध से लिया गया है।
यह डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर में दिए गए व्याख्यान का संशोधित रूप है।

