साक्षात्कार
हमसे बातचीत के दौरान प्रोफेसर अमन मदान उस बौद्धिक यात्रा की चर्चा करते हैं जिससे वे गुज़रे हैं। इस दौरान हमें शिक्षक के रूप में उनकी भूमिका के महत्व का अन्दाज़ा होता है। आलोचनात्मक शिक्षा और उसके ज्ञान-शास्त्र की जड़ों के बारे में उनका चिन्तन, नव-उदारवादी दुनिया के बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य के कारण उभरती चुनौतियों के बारे में उनकी गहरी समझ, डिजिटल दुनिया में पढ़ने और सीखने की प्रकृति पर उनके अवलोकन, और सबसे बड़ी बात, उनके द्वारा नियतिवाद को स्वीकार न करना हमें सम्भावनाओं और आशाओं के संसार में ले जाता है।
 प्रश्न - कृपया हमें अपनी शैक्षिक/बौद्धिक यात्रा के बारे में बताएँ। आज आप अपने आप को एक शिक्षाशास्त्री - यानी शिक्षाशास्त्र के एक प्राध्यापक जो शिक्षकों और शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को विकसित कर रहा है - के रूप में किस प्रकार देखते हैं?
प्रश्न - कृपया हमें अपनी शैक्षिक/बौद्धिक यात्रा के बारे में बताएँ। आज आप अपने आप को एक शिक्षाशास्त्री - यानी शिक्षाशास्त्र के एक प्राध्यापक जो शिक्षकों और शोधकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को विकसित कर रहा है - के रूप में किस प्रकार देखते हैं?
मुझे अक्सर इस बात में बड़ा आश्चर्य लगता है कि मेरी यात्रा की शुरुआत अपने अधिकांश शिक्षकों और उनके यांत्रिक पढ़ाने के तरीकों से दूर भागने से हुई थी। इसके चलते मैं उन शिक्षकों, मित्रों और संगठनों की तरफ खिंचा जिनमें कहीं अधिक प्रामाणिकता दिखाई देती थी और हमारे समय के ज्वलन्त मुद्दों के साथ जूझने की, उन्हें समझने की कहीं अधिक प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। पहले तो मैंने जीवविज्ञान में बी.एससी. किया था और मुझे पौधों और पशुओं का अध्ययन करना अद्भुत चीज़ लगती थी, और मेरे लिए वह बड़े आनन्द का स्रोत था। लेकिन प्रयोगशालाओं में और विराट अकादमिक नौकरशाही में बहुत ज़्यादा बारीक निरीक्षण तले काम करने का विचार बहुत निराशा पैदा करने वाला था। तो इसलिए मैंने सामाजिक विज्ञानों का रुख कर लिया, इस आशा से कि वहाँ मैं अपने चारों ओर फैली हिंसा और साम्प्रदायिक द्वेष की चिन्ताजनक समस्याओं को गहराई से समझ सकूँगा, और यह भी आशा थी कि यह एक ऐसा अध्ययन होगा जिसमें मैं आज़ादी से साँस ले सकूँगा। पंजाब विश्वविद्यालय में मानव शास्त्र का अध्ययन करते वक्त मैं भाग्यशाली रहा कि मुझे स्वर्गीय दिव्यदर्शी कपूर जैसे शिक्षक मिले जिन्होंने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि, शैक्षिक दृढ़ता और मूर्तिभंजन की प्रकृति से हमें बहुत प्रेरित किया। फिर जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय में सौभाग्य से मुझे अविजित पाठक जैसे शिक्षक मिले जो ईमानदारी और सच्चाई में पगी विद्वता का उदाहरण थे।
स्नातक-पूर्व वर्षों से मैं भाग्यशाली था कि मुझे बलराम बोधी और गुरिन्दर सिंह ‘डिम्पी’ जैसे दोस्त मिले जो सार्वजनिक मसलों पर अपना मत रखते थे और उसके लिए खड़े होते थे, और उन मुद्दों के लिए जो उनके दिल के बहुत करीब थे, वे अपने जीवन सहित कुछ भी दाँव पर लगाने के लिए तैयार रहते थे। उस समय जब हम भविष्य के जीवन के बारे में सोचते थे तो हम ऐसे समूहों के साथ काम करने के बारे में ही सोचते थे जो एक बेहतर भारत और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, न कि शिक्षक बनने के बारे में। धीरे-धीरे हममें से कई लोगों को यह महसूस होना शु डिग्री हुआ कि दुनिया को बदलने में शिक्षा का केन्द्रीय महत्व है। जब हम लोगों की निराशा और अज्ञानता से भरी प्रतिक्रियाएँ देखते थे तो हमें लगता था कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में संघर्ष करके कुछ स्थाई बदलाव लाए जा सकते हैं। बड़ी मासूमियत के साथ हम सोचते थे कि अगर आप बच्चों में तब्दीली ले आएँ तो दुनिया तब्दील हो जाएगी। अब तो खैर हमें भी एहसास होता है कि हमारी वह सोच ज़्यादा ही सरलता और भोलेपन से भरी थी।
कल्याणी डिके, जिनसे बाद में मैंने शादी की, ने मुझे एकलव्य के स्याग भाई से मिलवाया। उनके माध्यम से हम कई और लोगों से मिले जैसे अरविंद सरदाना, अनु गुप्ता, सी.एन. सुब्रह्मण्यम, रश्मि पालीवाल, यमुना सनी, सुशील जोशी और कई अन्य लोग जिन्हें देखकर लगता था कि वे बहुत बढ़िया ज़िन्दगी जी रहे थे और भारतीय सामाजिक विज्ञान के बारे में अपने बहुत गहरे विचारों को छोटे-छोटे कस्बों में काम करते हुए लागू कर रहे थे ताकि स्कूल में बच्चों द्वारा सीखी जाने वाली चीज़ों में बदलाव लाया जा सके। कल्याणी और मैंने सोचा कि हमें भी ऐसा ही जीवन जीना है। इसमें अकादमिक समुदाय के आडम्बरों और दिखावों से दूर जाने का लाभ तो था ही, साथ ही सबसे बुनियादी सवालों के साथ जुड़ने की गुंजाइश और स्वतंत्रता भी थी, और शिक्षा जगत के पदानुक्रम पर बैठे लोगों को सन्तुष्ट रखने के लिए किए जाने वाले कार्यों की मजबूरी भी नहीं थी। 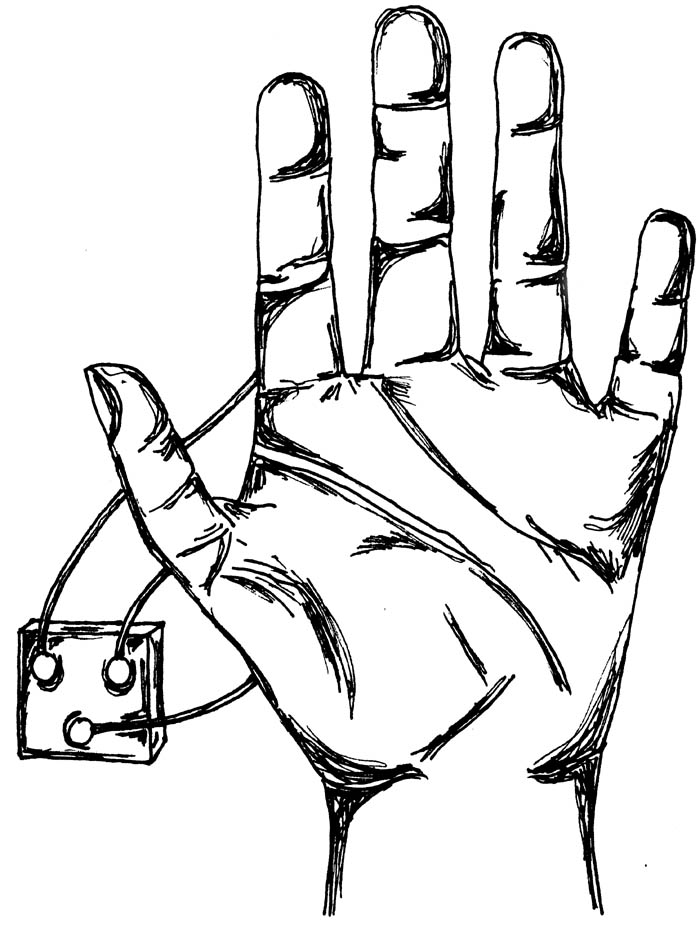 सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जुड़ने में मेरी रुचि के कारण मैं स्कूलों के भीतर ऐसे अनिवार्य स्थान के रूप में नागरिक शास्त्र की तरफ आकृष्ट हुआ जहाँ हमारे देश की कई समस्याओं से नज़रें मिलाई जा सकती थीं। लेकिन समस्या यह थी कि अधिकांश लोगों को नागरिक शास्त्र बहुत उबाऊ और अरुचिकर लगता था। एकलव्य ने अपने खास तरीके से यह सवाल किया कि आखिर क्यों बच्चों को नागरिक शास्त्र उबाऊ लगता था। होशंगाबाद में रहकर, एकलव्य में काम करते हुए इस बारे में मैं सामूहिक जीवन में विभिन्न संस्कृतियों के बीच के संघर्ष की तरफ इशारा करता रहा। तीन सालों तक लोगों से बात करके, पुस्तकालयों को चलाते, कार्यशालाओं का आयोजन करते, गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों से बात करके मैंने यह दलील देनी शुरु की कि यह एक ऐसी संस्कृति थी जो जातीय समाज की सत्ता के संवादों से उपजती थी। जो एक तरफ तो किसी जातीय समूह के भीतर सभी पुरुषों के बीच समानता की बात करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके और महिलाओं के तथा अन्य जातीय समूहों के बीच ऊँच-नीच का क्रम मौजूद था। इस स्थिति के विरोध में वह संस्कृति खड़ी थी जिसे स्कूली पाठ्यपुस्तकें व्यक्त करने की कोशिश कर रही थीं, और जिसमें संविधान के सभी मूल्यों -- सार्वभौमिक समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ इत्यादि -- की बात की जाती थी। इन दोनों संस्कृतियों के बीच का तनाव इतना गहरा था कि नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम एक सम्भावित युद्धभूमि बन गया था। इसलिए पाठ्यपुस्तक के लेखकों ने उनमें से वह सब कुछ हटा दिया जो विवाद का विषय हो सकता था, और सिर्फ भारतीय राज्य के कानूनों और नियमों को, तथा कुछ पाखण्ड से लगने वाले आदेशों को रहने दिया, जिसका अर्थ था कि हम कुछ भी बुरा नहीं देखते, कुछ बुरा नहीं सुनते और कुछ बुरा नहीं करते। इन दो संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसलिए, विलर्ड वॉलर के अमर कथन को थोड़ा-सा बिगाड़कर यह कह सकते थे कि नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें नैतिक गुणों के उजाड़ संग्रहालयों में तब्दील हो गई थीं, प्राण रहित और शरीर रहित।
सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया से जुड़ने में मेरी रुचि के कारण मैं स्कूलों के भीतर ऐसे अनिवार्य स्थान के रूप में नागरिक शास्त्र की तरफ आकृष्ट हुआ जहाँ हमारे देश की कई समस्याओं से नज़रें मिलाई जा सकती थीं। लेकिन समस्या यह थी कि अधिकांश लोगों को नागरिक शास्त्र बहुत उबाऊ और अरुचिकर लगता था। एकलव्य ने अपने खास तरीके से यह सवाल किया कि आखिर क्यों बच्चों को नागरिक शास्त्र उबाऊ लगता था। होशंगाबाद में रहकर, एकलव्य में काम करते हुए इस बारे में मैं सामूहिक जीवन में विभिन्न संस्कृतियों के बीच के संघर्ष की तरफ इशारा करता रहा। तीन सालों तक लोगों से बात करके, पुस्तकालयों को चलाते, कार्यशालाओं का आयोजन करते, गहरी समझ रखने वाले व्यक्तियों से बात करके मैंने यह दलील देनी शुरु की कि यह एक ऐसी संस्कृति थी जो जातीय समाज की सत्ता के संवादों से उपजती थी। जो एक तरफ तो किसी जातीय समूह के भीतर सभी पुरुषों के बीच समानता की बात करती थी, लेकिन दूसरी तरफ उनके और महिलाओं के तथा अन्य जातीय समूहों के बीच ऊँच-नीच का क्रम मौजूद था। इस स्थिति के विरोध में वह संस्कृति खड़ी थी जिसे स्कूली पाठ्यपुस्तकें व्यक्त करने की कोशिश कर रही थीं, और जिसमें संविधान के सभी मूल्यों -- सार्वभौमिक समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएँ इत्यादि -- की बात की जाती थी। इन दोनों संस्कृतियों के बीच का तनाव इतना गहरा था कि नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम एक सम्भावित युद्धभूमि बन गया था। इसलिए पाठ्यपुस्तक के लेखकों ने उनमें से वह सब कुछ हटा दिया जो विवाद का विषय हो सकता था, और सिर्फ भारतीय राज्य के कानूनों और नियमों को, तथा कुछ पाखण्ड से लगने वाले आदेशों को रहने दिया, जिसका अर्थ था कि हम कुछ भी बुरा नहीं देखते, कुछ बुरा नहीं सुनते और कुछ बुरा नहीं करते। इन दो संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित करने की कोई कोशिश नहीं की गई। इसलिए, विलर्ड वॉलर के अमर कथन को थोड़ा-सा बिगाड़कर यह कह सकते थे कि नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकें नैतिक गुणों के उजाड़ संग्रहालयों में तब्दील हो गई थीं, प्राण रहित और शरीर रहित।
बाद में, आई.आई.टी., कानपुर में काम करते हुए मेरी दिलचस्पी शिक्षा में असमानता से जुड़ी विचारधाराओं में हुई। शोध के इस विषय में मेरी दिलचस्पी मण्डल के दूसरे दौर के कारण हुई। वहाँ पर मेरे कई साथी गैर-अगड़ी जातियों के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे थे उनसे मैं बहुत दुखी और आहत हो गया था। उन लोगों की बातों में ऐतिहासिकीकरण की कमी से, सामाजिक विषमताओं को न्यायोचित ठहराने के ढंग से, और सामाजिक ढाँचे किस प्रकार लोगों को शिक्षा में कमतर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करते हैं इसके बारे में उनके भोलेपन से मुझे बहुत अचम्भा हुआ। हालाँकि, मेरे ही साथियों में इसके कई अपवाद भी मौजूद थे, लेकिन मुझे एहसास होना शु डिग्री हो गया था कि शिक्षित भारतीय उच्च वर्गों की व्यापक संस्कृति यही है। बहुत बाद में मैंने लोकप्रिय अर्थशास्त्र की एक किताब पढ़ी जिसका नाम था द विनर टेक ऑल सोसायटी। मुझे लगा कि यह शीर्षक इस तरह की नैतिकता का उचित वर्णन करता है जहाँ सबसे ऊपर बैठे लोग किसी भी चुनौती का विरोध करते हैं और अपने माल पर किसी और के दावे को खारिज करने के लाखों तरीके ढूँढ़ लेते हैं लेकिन खुद अपने दावों की मनमानी प्रकृति और अवैधता की तरफ आँखें मीच लेते हैं। इस अनुभव ने मुझे योग्यता के चरित्र, और फिर आरक्षण की व्यवस्था से जुड़ी चर्चा की तरफ खींचा। मैं बहुत भाग्यशाली रहा कि मुझे अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में इस तरह के कुछ विचारों को अमल में लाने के लिए बहुत सहयोगपूर्ण माहौल मिला। यहाँ हमने ऐतिहासिक असुविधा भोगे हुए लोगों के प्रवेश को तौलने के लिए न सिर्फ जाति बल्कि आठ अलग-अलग मानदण्डों का इस्तेमाल करके एक सामाजिक-आर्थिक असुविधा सूची बनाने की कोशिश की है।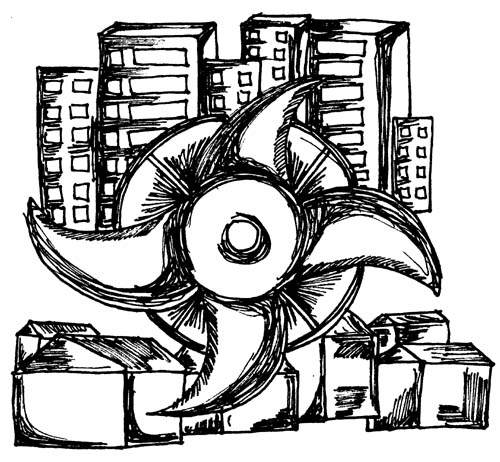 एकलव्य, ए.पी.एफ. और कई अन्य लोगों के साथ ही मैं भी अक्सर यह सोचता रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्थाओं को अधिक न्यायोचित और समतावादी किस तरह बनाया जा सकता है। आखिरकार, आरक्षण तो एक वृहत सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था के घावों पर लगाई गई एक सांकेतिक मरहम पट्टी भर था। आजकल मैं उन विभिन्न ताकतों के बारे में सोचता रहता हूँ जो किन्हीं शिक्षा व्यवस्थाओं को रूपान्तरित करने में सहायक होती हैं। एक ताकत जिसे कम तवज्जो मिलती रही है वह है किसी समाज और उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में राजनीति, सामाजिक आन्दोलनों और सम्भ्रान्त वर्गों की विचारधाराओं की भूमिका। संवेदनशील और विचारवान राम शास्त्री और बी. रामदास, जो एकॉर्ड और आदिवासी मुन्नेत्र संगम के सदस्य हैं, ने मुझे इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। एन.जी.ओ., सी.एस.आर. और राज्य की नौकरशाही की प्रवृत्ति तकनीकी समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने की होती है। हमें खुद को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारे जीवन और समाज का एक राजनैतिक पहलू भी होता है। और इसका हमारी प्राथमिकताओं को तय करने, हम क्या देखते हैं और किसे अनदेखा करते हैं इसे तय करने में और ऐसे समूहों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बाद में कुछ खास रुख अपनाते हैं, दूसरे नहीं।
एकलव्य, ए.पी.एफ. और कई अन्य लोगों के साथ ही मैं भी अक्सर यह सोचता रहा हूँ कि शिक्षा व्यवस्थाओं को अधिक न्यायोचित और समतावादी किस तरह बनाया जा सकता है। आखिरकार, आरक्षण तो एक वृहत सामाजिक और शैक्षणिक व्यवस्था के घावों पर लगाई गई एक सांकेतिक मरहम पट्टी भर था। आजकल मैं उन विभिन्न ताकतों के बारे में सोचता रहता हूँ जो किन्हीं शिक्षा व्यवस्थाओं को रूपान्तरित करने में सहायक होती हैं। एक ताकत जिसे कम तवज्जो मिलती रही है वह है किसी समाज और उसकी शिक्षा व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित करने में राजनीति, सामाजिक आन्दोलनों और सम्भ्रान्त वर्गों की विचारधाराओं की भूमिका। संवेदनशील और विचारवान राम शास्त्री और बी. रामदास, जो एकॉर्ड और आदिवासी मुन्नेत्र संगम के सदस्य हैं, ने मुझे इस स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद की है। एन.जी.ओ., सी.एस.आर. और राज्य की नौकरशाही की प्रवृत्ति तकनीकी समाधानों पर ध्यान केन्द्रित करने की होती है। हमें खुद को यह याद दिलाते रहना चाहिए कि हमारे जीवन और समाज का एक राजनैतिक पहलू भी होता है। और इसका हमारी प्राथमिकताओं को तय करने, हम क्या देखते हैं और किसे अनदेखा करते हैं इसे तय करने में और ऐसे समूहों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है जो बाद में कुछ खास रुख अपनाते हैं, दूसरे नहीं।
मैं शिक्षक के रूप में अपने कार्य को इसी नज़रिये से देखता हूँ। यह भारतीय समाज में एक सांस्कृतिक राजनीति का हिस्सा है। विद्यार्थियों और साथियों को जब हम उत्पीड़ित लोगों के अनुभवों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं तब हम बलवानों के आधिपत्य के खिलाफ काम करते हैं। सिद्धान्तों से निकलने वाली गहरी समझ का उत्सव हम तकनीकी-यांत्रिकीय ज्ञानहितों की संकीर्णता और समझ की आँखों पर बाँध दी जाने वाली पट्टी के विरोध में खड़े होकर मनाते हैं। इस बात पर ज़ोर देकर कि मनुष्यों और उनके सम्बन्धों का अध्ययन करके भी हम एक कैरियर और सार्थक जीवन हासिल कर सकते हैं, हम तकनीकी विशेषज्ञों वाली नौकरशाही के कठोर पिंजरों से आज़ाद होने में विद्यार्थियों की मदद करते हैं। यह कहकर कि सुधारवादी आलोचना, शोध, शिक्षण और सृजनात्मक कार्यों के कोई बँधे-बँधाए ढाँचे नहीं होते, बल्कि सब एक साथ चल सकते हैं, दरअसल हम उस निराशा के खिलाफ खड़े होते हैं जो हमें हार मानने को और जीवन के प्रभुत्व विचारों और जीवन शैलियों को अपनाने पर मजबूर करती है।
हो सकता है कि मेरी अपनी ज़िन्दगी में एक शिक्षक के रूप में मैं यह सब बहुत अच्छे से न कर पाया होऊँ। लेकिन मुझे यह ज़रूर लगता है कि इन दिशाओं में उठाया गया एक छोटा-सा कदम भी किसी बड़े बदलाव की नींव साबित हो सकता है।
प्रश्न - अगर हम शिक्षा के विषय को एक वृहत सामाजिक-राजनैतिक/दार्शनिक चर्चा के एक अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं तो आप आलोचनात्मक/मुक्तिदाई शिक्षण के ज्ञान-शास्त्र की जड़ें कहाँ देखते हैं?
भारत में जिस तरह हम आलोचनात्मक और मुक्तिदायी शिक्षण की बात करते हैं वह सम्भवत: ज्ञान-शास्त्र के कई स्रोतों से बनता है। एक स्रोत तो निश्चित ही उन्नीसवीं सदी में हुए मानव शास्त्र के विकास के ढंग में मौजूद है, खास तौर पर जैसा कि कार्ल मार्क्स की रचनाओं में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मार्क्स की रचनाओं में हम पाते हैं कि मनुष्यों ने वास्तविक दुनिया के साथ अपनी अन्तर्क्रिया और संघर्ष के द्वारा खुद का निर्माण किया। वे अस्तित्व में बने बनाए नहीं आए थे बल्कि उन्होंने खुद को हर तरह से ‘बनाया।’ हमारी मानवता को इस निर्माण में बहुत-सी निराशाओं और अवरोधों का सामना करना पड़ा। सामन्ती काल में मनुष्यों की रचना और उनकी पूर्ण अभिव्यक्ति को प्रभुत्व और वर्चस्व के उन सामन्ती सम्बन्धों ने बाधित कर दिया जिन्होंने अधिकांश आबादी को बन्धनों और दरिद्रता में घेर कर रखा था। पूंजीवाद में इसे चालाकी भरे बाज़ारवादी सम्बन्धों के द्वारा और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं द्वारा बाधित कर दिया जाता है, और इस तरह हम अपनी क्रियाशीलता को त्याग देते हैं। मनुष्य की क्रियाशीलता और उसके कृत्यों की दृढ़ता आलोचनात्मक शिक्षण का केन्द्र हैं। इसे अपनी अभिव्यक्ति के लिए उत्पीड़न की एक वृहत सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष करना पड़ता है। ये वे विचार हैं जो पाउलो फ्रेयर की रचनाओं से भी निकलते हैं।
यहाँ हमें एक ‘झूठी चेतना’ की अवधारणा मिलती है और चेतावनी मिलती है कि संस्कृति और समझ को सतर्कता के साथ देखना चाहिए, और उन्हें उनके प्रत्यक्ष मूल्य के हिसाब से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हमारी समझ की संरचना हमारे क्रियान्वयन के द्वारा आकार लेती है, और जब उसे ही विकृत किया जा रहा हो तो हमारी समझ और हमारी कल्पनाशीलता भी उससे अछूती नहीं रह सकती। ज्ञान और उसका प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वे किसी पर प्रभुत्व स्थापित करने के काम न आएँ, शायद मुक्त होने का अर्थ यही है।
एक और स्रोत है अमरीकी व्यवहारवाद, खास तौर पर ड्यूई और उनके अनुयायियों का काम। भारत में ऐसे बहुत-से लोग हैं जो मार्क्स को पढ़ने में कतराते हैं लेकिन जॉन ड्यूई, हर्बर्ट ब्लमर और जॉर्ज हर्बर्ट मीड को पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इन लेखकों में भी हम यही धारणा देखते हैं कि मनुष्य के कृत्य ही उसकी समझ को बनाते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचनात्मक शिक्षण वह है जो शिक्षक व विद्यार्थी के बीच स्वैच्छिक संवाद और अन्तर्क्रिया को प्रेरित करता हो जिससे कहीं ज़्यादा पूर्ण और गहरी समझ विकसित होती है। इसमें मार्क्स से समानताएँ स्पष्ट दिखती हैं। लेकिन इनके बीच का अन्तर शिक्षक-विद्यार्थियों के बीच के संवाद को सीमित करने में सामाजिक संरचनाओं की भूमिकाओं में देखा जा सकता है। जहाँ ड्यूई हमारे कृत्यों पर सर्वांगीण बाधाओं के सवालों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, वहीं इस परम्परा के अन्य लोगों में ज़्यादा संशय दिखाई देता है।
भारत में अंबेडकरवादियों और महिलावादी आन्दोलनों ने हाल में आलोचनात्मक शिक्षण की तरफ ज़ोरदार प्रयास किया है। इन दोनों ही आन्दोलनों ने -- और कभी-कभी वे एक ही आवाज़ में बात करते हैं -- इस ओर इशारा किया है कि सांस्कृतिक अर्थ प्रभुत्व व आधिपत्य के रंगों में रंगे हो सकते हैं। पितृसत्ता और जातिवाद ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के अपने बारे में, और जिस तरह स्कूली ज्ञान बनता है उस बारे में, दृष्टिकोणों को तय किया है। प्रभुत्व के इन स्वरूपों पर सवाल खड़े करना भारत में शैक्षणिक चर्चाओं से जुड़े आन्दोलनों का एक अहम तत्व रहा है।
शिक्षण से सम्बन्धित दूसरे विचार भी हैं, लेकिन आलोचनात्मक शिक्षण का स्वरूप तय करने के लिए गाँधीवादी जड़ों का उल्लेख करना अभी के लिए काफी होगा। गाँधी और उनसे प्रेरित हुए कई लोग पाश्चात्य तथा औद्योगिकीकरण के हिमायती विमर्शों पर गहरे सवाल खड़े करते हैं। ये विमर्श सोचने, और अपने शरीर को पूरी तरह इस्तेमाल करने की हमारी क्षमताओं को दरिद्र बनाकर हमें कैद कर लेते हैं। ये हमें ऐसी तकनीकों की तरफ खींच लेते हैं जो हमें सबल बनाने की बजाय अपना गुलाम बना लेती हैं। विकास के इस रूप की गाँधीवादी आलोचना, और स्कूली ज्ञान पर प्रभुत्व रखने वाली प्रवृत्तियों ने हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित किया है कि हमें वाकई में स्वतंत्र बनाने के लिए और स्वराज प्राप्त करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है।
प्रश्न - द न्यू लीम के इस अंक में हमने कार्ल मार्क्स, इवान इलिच और मोहनदास गाँधी का आह्वान किया है क्योंकि हम मानते हैं कि इन विचारकों/दृष्टाओं ने हमें शिक्षा और जीवन को एक बिलकुल अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित किया। लेकिन, हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ हम नव-उदारवादी बाज़ार और सामाजिक रूढ़िवाद का अपवित्र गठबन्धन देख रहे हैं। इन परिस्थितियों में, क्या सम्भव है कि हम सिर्फ बाज़ारोन्मुख/कौशल-आधारित सीखने की बजाय जीवन को महत्व देने वाली शिक्षा में फिर से भरोसा दिखा सकें?
जिसे आपने जीवन को महत्व देने वाली शिक्षा कहा है वह आसानी से समाप्त नहीं हो जाएगी, वह बार-बार प्रकट होती रहेगी। स्वतंत्रता संघर्ष के सालों में यह नई तालीम की ज़ुबान बोलती थी, 1970 के बाद के कुछ सालों में यह सशक्तिकरण और विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की भाषा बोलती थी, आज के वक्त में यह उन सभी आवाज़ों के माध्यम से बोलती है जो सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है और जो कक्षा के भीतर चुके हुए और निराश महसूस करते हैं। इनमें वे बहुत सारे विद्यार्थी और शिक्षक शामिल हैं जो बेतरतीब ढंग से तकनीकी और प्रबन्धन की शिक्षा में फँस गए थे। प्रबन्धन जगत के सम्भ्रान्त लोगों की एक पसन्दीदा तकनीक है जिसका वे बार-बार प्रयोग करते हैं -- जीत का गीत गाना, यह बताना कि उनकी संस्थाएँ कितनी श्रेष्ठ हैं और उनका ज्ञान कितना अद्भुत है और यह राष्ट्र कितना महान बन जाएगा। लेकिन विद्यार्थी जिन्हें खाली-खाली महसूस होता है, और शिक्षक जिन्हें अपनी कक्षाओं में नियंत्रण बनाए रखने के लिए ‘पेशेवराना रुख’ अपनाना पड़ता है, अपने दिलों में जानते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है।
संस्कृति और शिक्षा को लेकर तकनीकी-यांत्रिकीय पद्धतियों की बुनियादी समस्या है कि वे लोगों की मनुष्यता तक पहुँचने और उसके साथ जुड़ने में नाकाम हैं। इस वजह से बराबर ये सवाल उठता रहेगा कि हो क्या रहा है।
पर इतिहास को सामाजिक ताकतों की कुल गणना के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम अपना इतिहास खुद बनाते हैं और बार-बार हम समूहों, संगठनों, आवाज़ों और आन्दोलनों का उभार देखते हैं जो उस मौजूदा दौर की आम समझ को चौंका देते हैं। विकल्प तैयार करना और बनाना हमारे ऊपर है। हम नियतिवाद की सोच नहीं अपना सकते, कि या तो हार मान लें या इतिहास का इन्तज़ार करें कि वह खुद किसी तरह मुश्किलों से उबरकर चीज़ों को बदल देगा। एक साथ मिलकर कई आवाज़ें जीवित रह सकती हैं, अपने समय आने का इन्तज़ार कर सकती हैं, गहरी समझ विकसित कर सकती हैं।
प्रश्न - सूचना की क्रान्ति में एक विरोधाभास भी है। यह ठीक है कि नई तकनीकों के कारण हम अपने आपको सूचनाओं से घिरा हुआ पाते हैं। फिर भी यह डर तो है कि पढ़ने की संस्कृति -- सिर्फ मज़े के लिए पढ़ना, पाठ्यक्रम से इतर अच्छी किताबें पढ़ना, श्रेष्ठ साहित्य और दर्शन पढ़ना -- समाप्त हो रही है। इसके अलावा, परीक्षाओं का दबाव और कोचिंग संस्थानों द्वारा प्रचारित की जाने वाली गाइड किताबें किशोर व युवा विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता को बाँध देने का काम करती हैं। आप इस विरोधाभास को किस तरह देखते हैं? या आप इससे सहमत नहीं हैं?
इस बारे में मेरी राय थोड़ी अस्पष्ट है। एक तरफ तो यह सच है कि अँग्रेज़ी में पढ़ी और बेची जा रही अधिकांश किताबें परीक्षाओं से या फिर ‘सफल कैसे बनें’ से सम्बद्ध हैं। लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि सामाजिक विज्ञानों और मानविकी के विषयों के बाहर के बहुत सारे लोग अन्य तरह की किताबें पढ़ रहे हैं। कथा साहित्य अभी भी खूब बिकता है और इतिहास तथा अन्य प्रकार के गैर-कथा लेखन में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। भले ही हम इन लेखकों की गुणवत्ता के बारे में कुछ भी सोचें लेकिन जिस तरह चेतन भगत और देवदत्त पटनायक की किताबें अँग्रेज़ी में बड़ी संख्याओं में बिक रही हैं वह दिखाता है कि लोग ऐसी पौराणिक कथाएँ और वर्णन पढ़ना चाहते हैं जो संकुचित यांत्रिकीय ज्ञान के बाहर हैं। यह याद रखना भी प्रासंगिक होगा कि पिछले कुछ दशकों में ऐसे बहुत सारे लोग पाठकों की दुनिया में शामिल हो गए हैं जिनके माता-पिता ने न तो कभी कोई किताब खरीदी होगी न ही कभी पढ़ी होगी। शायद हमें संवाद करने की शैलियों और स्वरूपों को नई शक्ल देने की ज़रूरत है ताकि ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों तक उनकी पहुँच हो सके। शायद पुराने समय के लिखने के तरीकों को नए ज़माने के लोगों के मुताबिक ढालना होगा। समय गुज़रने के साथ संवाद की शैलियों में हुआ बदलाव कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अगर आज मैं टॉल्सटॉय और हरमन मैलविल जैसे महान लेखकों को पढ़ने की कोशिश करूँ तो आज के लेखकों के वर्णनों के मुकाबले में मुझे उनका लेखन बहुत ज़्यादा फैलाव वाला और असम्बद्ध लगेगा। वाकई समय के साथ शैलियों में बदलाव होना चाहिए।
जब मैं युवाओं को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए देखता हूँ तो मैं इसकी सम्भावनाओं के बारे में सोचने लगता हूँ। वे अपने मोबाइल, टेबलेट और लैपटॉप पर सिर्फ तकनीकी सामग्री नहीं पढ़ रहे होते। बल्कि उनका ज़्यादातर समय ब्लॉग, समाचार पढ़ने या सोशल मीडिया पर जाता है। यह मनुष्यों से जुड़े मामलों में, और जीती-जागती दुनिया में रुचि होने का उदाहरण है। मैं देखता हूँ कि युवा एक-दूसरे के साथ वीडियो और तस्वीरें साझा करते रहते हैं और उन पर काफी भावनात्मक व सुरुचिपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया देते हैं, और अपने दोस्तों के साथ घण्टों तक टिप्पणियों का आदान-प्रदान करते रहते हैं। कभी किताब न खोलने वाले लोगों के बीच भी टेड टॉक और ऐसे ही बहुत-से अन्य वीडियो, जो बेसिरपैर का मनोरंजन नहीं हैं, की आश्चर्यजनक लोकप्रियता निश्चित रूप से कुछ बताती है। इसके पीछे शायद यह वजह भी हो सकती है कि तकनीक ने चलती-फिरती तस्वीर को बनाना और देखना बहुत सस्ता कर दिया है। और इसकी ताकत और प्रभाव ऐसा हो गया है कि लोग जब अपने जीवन में या रिश्तों में अर्थ तलाशने की कोशिश करते हैं तो शब्द की बजाय चित्र को अपना साधन बनाते हैं।
इतिहास में एक समय, तकनीक की एक खास व्यवस्था के चलते, पुस्तक वह जगह थी जहाँ बुद्धिजीवी अपने काल की पड़ताल करते थे। यू.आर. अनंतमूर्ति जैसे महान विचारक साहित्य प्रेमी विद्वान लोगों में व्यापक रूप से पढ़े जाते थे और उनके लिए ये किताबें कभी प्रेरणा का स्रोत होती थीं तो कभी क्रोध और अस्वीकृति का। इंटरनेट की राजनीति को, और उसमें जिस तरह कुछ खास तरह के संवाद को तरजीह मिलती है, उसे कम करके न आँकते हुए शायद हम आज ऐसा समय देख रहे हैं जहाँ छपी हुई किताबों के अलावा और भी स्थान हो गए हैं और जो लोग विचारों के मन्थन का हिस्सा बनना चाहते हैं उन्हें इन स्थानों पर संवाद करना भी सीखना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग फेसबुक और यूट्यूब पर अपने विचारों को और आज के समय के बारे में अपनी आलोचनाओं को साझा कर रहे हैं तो वे लोग जो दूसरों तक पहुँचना चाहते हैं, उन्हें भी इन स्थानों पर संवाद करने की कला को सीखने की कोशिश करना चाहिए।
प्रश्न - हम आपके पढ़ाने के प्रयास के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि किस प्रकार आप अच्छी किताबों की दुनिया से, गहरे शैक्षणिक फलसफों और नूतन शैक्षणिक पद्धतियों से विद्यार्थियों का परिचय कराते हैं। और फिर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया क्या होती है? क्या यह सम्मिलन का क्षण होता है या द्वन्द्व से भरे संवाद का?
दुर्भाग्यवश, मैं ऐसा शिक्षक नहीं हूँ जो वह क्या कर रहा है उसके बारे में बहुत सोचे-विचारे या सजग रहे। मेरे ऐसे मित्र और साथी भी हैं जो, वे जो कर रहे होते हैं उसे बहुत अच्छे से सिद्धान्त रूप में व्यक्त कर सकते हैं और फिर अपने सिद्धान्तों के बिलकुल अनुरूप विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं जो भी करता हूँ उसका वर्णन करना या उसे सही ठहराना मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। आइए मैं ज़रा दो पहलुओं के बारे में बात कर लूँ -- मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ उसकी विषयवस्तु का अर्थ और उसकी अपील तथा विद्यार्थियों को दी जाने वाली जगह और गुंजाइश की ज़रूरत।
शायद एक चीज़ जो मैं बहुत करता हूँ वह है कि मैं अवधारणाओं और सिद्धान्तों को जीते-जागते, भावनात्मक, जीवन्त उदाहरणों में बदल देता हूँ। रोज़मर्रा का जो जीने का संघर्ष रहता है, मैं उसी से प्रेरित होकर सवालों का जवाब ढूँढ़ता हूँ। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्होंने पूर्णत: औपचारिक आधार पर कुछ निश्चित सवालों के उत्तर तलाशने के लिए खुद को प्रशिक्षित कर लिया है या फिर उन्हें ऐसा करने से कुछ बाहरी लाभ मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता और विद्यार्थियों को भी ऐसा करते नहीं देख सकता। किसी मुद्दे का अध्ययन करने या उसके बारे में गहराई से सोचने का कारण उसकी व्यक्तिगत या भावनात्मक अपील, उसके द्वारा उठाई जाने वाली व्यावहारिक चुनौतियाँ, और ऐतिहासिक अर्थ में तथा दैनिक गतिविधियों में उसके द्वारा सामने लाई जाने वाली गहरी नैतिक दुविधाएँ होना चाहिए। तो मैं जब भी पढ़ाता हूँ तब मैं कक्षा के भीतर इन्हीं सरोकारों को लाने की कोशिश करता हूँ। किसी कक्षा के लिए तैयारी का ज़्यादा सृजनशील और समय लेने वाला भाग होता है किसी विषय की अपील और उसके विभिन्न पहलुओं के अर्थ को तय करने का सही ढंग तलाश करना। कभी-कभी यह तरीका असफल हो जाता है तो कभी सफल भी हो जाता है। जिस समय यह तरीका काम कर जाता है तो ऐसा लगता है कि इससे विद्यार्थियों में अपने से सोचने और पढ़ने की प्रेरणा पैदा होती है और उन मुद्दों से उनका भी जुड़ाव बन जाता है। कक्षा में अपनी चर्चाओं में मैं एक पहलू दिमाग में रखने की कोशिश करता हूँ कि किसी समस्या के बारे में ‘हम क्या कर सकते हैं’। सिर्फ किसी चीज़ का विश्लेषण करना व्यर्थ और आत्म-आसक्ति जैसा लगता है। लोगों ने इस बारे में जो कुछ किया है या इस क्षेत्र में कार्य करने की क्या सम्भावनाएँ हो सकती हैं, इसके बारे में कम-से-कम कुछ दखल रखने से ऐसा लगता है कि कक्षा को सही गति और उद्देश्य मिल जाते हैं।
मैं आम तौर पर खुद भी एक सन्देही छात्र था इसलिए अभी भी मैं इस बात को नहीं मानता कि आधिकारिक रूप से शिक्षक नियुक्त हो जाने पर मैं अपने आप विद्यार्थियों से सार्थक बातें करने लगूँगा। हाँ, मेरे पास ऐसा कुछ कहने को होगा जो मेरे लिए तो सार्थक हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके लिए भी हो। एक कोर्स के समाप्त होने पर मैं आम तौर पर मेरी तरफ ध्यान देने के लिए विद्यार्थियों का आभार व्यक्त करता हूँ। कोर्स के दौरान अगर इन मसलों के बारे में वे भी चिन्तित महसूस करने लगें तो मुझे लगेगा कि मेरा प्रयास सफल हुआ। लेकिन, ज़ाहिर है, मैं यह नहीं मान सकता कि यह सिर्फ मेरे प्रयास का नतीजा होगा, उसमें बहुत-से दूसरे कारकों का हाथ हो सकता है। लेकिन ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिन्हें लगता है कि मेरी बातें इस लायक नहीं हैं कि उनके लिए वे अपनी ऊर्जा या दिमाग का इस्तेमाल करें। या फिर ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिन्हें मेरे दिए हुए कार्य उनकी बाकी रुचियों की तुलना में कम महत्व के लग सकते हैं। उनके साथ दण्ड देने का तरीका अपनाना निरर्थक है। आप ही सोचें, कोई किसी को डाँटकर या दबाव डालकर किसी चीज़ को पसन्द करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता है! इसकी बजाय मैं ऐसे प्रश्न और उदाहरण ढूँढ़ने की कोशिश करता हूँ जिससे उनका ध्यान खींचा जा सके। कभी-कभी यह तरीका काम करता है, कभी नहीं करता है। शायद किसी भी अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुति की तरह शिक्षण भी सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विशिष्ट कार्य है। कभी-कभी हमें पूरी तरह एक-से सांस्कृतिक आधारों के साये में बातचीत करने का खुशगवार मौका मिलता है। लेकिन कभी-कभी हम दूसरी संस्कृति के साथ भी बात करते हैं और ऐसी स्थिति में बातचीत की एक धीमी प्रक्रिया विकसित होती है जो, ज़ाहिर है, दोनों को रूपान्तरित करती है। हर समय व्यक्ति को सामने वाले के दृष्टिकोण का सम्मान करना चाहिए और इस बात पर तुले नहीं रहना चाहिए कि मेरी संस्कृति ही बुनियादी रूप से सही और श्रेष्ठ है। जिस क्षण व्यक्ति ऐसा करना शुरु करता है तो फिर वह संवाद न रहकर आरोपण बन जाता है। हाँ, विद्यार्थी हार मानकर आपके आरोपण को भी स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन फिर यह एक प्रभुत्व और अधिकार का कृत्य हो जाएगा और आपके बीच एक कष्ट देने में खुशी पाने वाला विकृत रिश्ता बनेगा। मैं तो वही तरीका पसन्द करूँगा जिसमें हम मित्रों की तरह मिलकर सीखें। मुझे तानाशाही शिक्षक कभी अच्छे नहीं लगे और मैं खुद भी ऐसा नहीं बनना चाहता।
अमन मदान: बेंगलुरु में अपनी माता, पत्नी और पुत्र के साथ रहते हैं। वहाँ के लोग उन्हें बहुत पसन्द हैं और वहाँ की भाषा बहुत मधुर लगती है, मगर उसे सीखने की उनकी कोशिशें ज़्यादातर नाकामयाब रही हैं। समाज शास्त्र और मानव विज्ञान के अलावा उन्हें साइकल चलाना और बाँसुरी बजाना भी पसन्द है। उनके परिवार और पड़ोसियों को उनका बाँसुरी वादन कितना पसन्द है, इस पर विवाद है। अपनी साइकल, कंप्यूटर इत्यादी को खोलकर खुद ठीक करते हैं और इसमें भी उन्हें बहुत आनन्द आता है। वर्तमान में, अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु में पढ़ाते हैं और उन्हें ऐसे छात्रों के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है जो कि समाज के प्रति संवेदनशील और प्रतिबद्ध हैं। पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ से एंथ्रोपोलॉजी में स्नातकोत्तर और जवाहर लाल नेह डिग्री विश्वविद्यालय, दिल्ली से डॉक्टरेट की पढ़ाई की है। सन् 2000 से 2003 तक एकलव्य के होशंगाबाद केन्द्र से जुड़े रहे हैं। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन (मुम्बई), टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (मुम्बई) और आई.आई.टी. (कानपुर) में कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया है।
अँग्रेज़ी से अनुवाद: भरत त्रिपाठी: पत्रकारिता की पढ़ाई। स्वतंत्र लेखन और द्विभाषिक अनुवाद करते हैं। होशंगाबाद में निवास।
सभी चित्र: प्रज्ञा शंकरन: सृष्टि इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, बैंगलोर से स्नातक की पढ़ाई कर रही हैं।
यह इंटरव्यु द न्यू लीम के नवम्बर-दिसम्बर, 2016 अंक (वर्ष 2, अंक 16-17) में प्रकाशित हुआ था। और मुद्रित रूप में उपलब्ध है।


