हिमांशु श्रीवास्तव
 हर साल गर्मियों में एकलव्य 8-10 दिनों का आवासीय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस प्रशिक्षण में माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के स्तर पर विज्ञान और गणित के चुनिन्दा विषयों पर काम होता है। पाठ्यचर्या और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सत्र होते हैं। विषय विशेषज्ञ, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं से कोई 40-50 लोग इस प्रशिक्षण में शामिल होते हैं।|
हर साल गर्मियों में एकलव्य 8-10 दिनों का आवासीय विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। इस प्रशिक्षण में माध्यमिक और उच्च विद्यालयों के स्तर पर विज्ञान और गणित के चुनिन्दा विषयों पर काम होता है। पाठ्यचर्या और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सत्र होते हैं। विषय विशेषज्ञ, सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी संस्थाओं से कोई 40-50 लोग इस प्रशिक्षण में शामिल होते हैं।|
इस प्रशिक्षण का एक मुख्य अंग होता है प्रोजेक्ट्स का, जिसमें शिक्षकों द्वारा चुने सवालों की जाँच-पड़ताल की जाती है। सवाल कुछ भी हो सकते हैं - आपकी कोई भी जिज्ञासा, किसी बच्चे का सवाल, सालों से दिमाग में घूम रही कोई शंका इत्यादि। 6-7 दिनों में जितना हो सके, इस पर काम होता है। समस्या का हल निकालने के लिए शुरुआत कैसे की जाए और किन तरीकों का इस्तेमाल हो, बहुत खर्च किए बिना काम कैसे करें, जुगाड़ कैसे जमाएँ, इन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है।
प्रोजेक्ट्स के पीछे प्रमुख विचार यह है कि सीखने की शुरुआत असली सवाल से हो, और ये सवाल खुद के हों तो और भी बेहतर। आम तौर पर शिक्षा का पूरा कारोबार पाठ्य पुस्तकों के भरोसे चलता है। छात्रों को कभी मालूम नहीं पड़ता कि ये पाठ्य पुस्तकें किन सवालों का जवाब देती हैं। प्रोजेक्ट्स का विचार ही यह है कि सीखने की प्रेरणा उन सवालों से मिले जो आपको उकसाते हैं। विज्ञान में भी खोज की शुरुआत सवालों से ही तो होती है।
सोच-विचार कर, समूह में काम करने का मज़ा ही अलग है। इस प्रक्रिया में किसी एक सही नतीजे पर पहुँचने की अपेक्षा नहीं होती है। मुख्य उद्देश्य है विज्ञान की प्रक्रिया का अनुभव प्राप्त करना और यह विश्वास जगाना कि कई समस्याओं के हल, कुछ हद तक तो हम अक्सर खुद या समूहों में काम करके निकाल सकते हैं। और जवाब तक न पहुँचें तो भी सवाल को समझना और जवाब खोजने की कठिनाइयों को समझना भी कम प्रेरक नहीं होता।
यह लेख, ऐसे ही एक सवाल पर किए प्रोजेक्ट पर आधारित है।
यूँ तो सवाल पूछना, सवाल खड़े करना, किसी बात को तर्क और अनुभव की कसौटी पर कसे बिना न मानना वगैरह विज्ञान करने-कराने की प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं और इसलिए विज्ञान की कक्षा में भी इसके लिए जगह बनाए जाने की ज़रूरत है। पर सवाल-जवाब का सिलसिला जब एक बार शु डिग्री होता है तो विषयगत सीमाएँ बहुत बनावटी हो जाती हैं। चाहे विज्ञान की कक्षा में हो या उसके बाहर, सवाल न तो विषय की सीमाओं में बँधे होते हैं और न ही उम्र का लिहाज़ करते हैं। जैसे कई बच्चे यह जानने में रुचि रखते हैं कि बच्चे आते कहाँ से हैं और बड़ों को यह समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस सवाल का जवाब अभी क्यों नहीं दिया जा सकता। और बच्चे ही क्यों, बड़े भी तो ऐसे असहज कर देने वाले सवालों से जूझते रहते हैं। इस लेख में मैं ऐसे ही एक सवाल पर बात करने जा रहा हूँ जो मुझे काफी समय से परेशान करता रहा है और जो कई लोगों को दुविधा में डालने की क्षमता रखता है।
आपने दुकानों, गाड़ियों वगैरह में नींबू और मिर्च को एक धागे में पिरोकर टाँगते हुए तो ज़रूर देखा होगा। शायद आपके घर, दुकान या गाड़ी में आपने भी टाँग रखा हो। खैर, मैं तो एक सामान्य बात कर रहा हूँ। दरअसल मुझे यह कभी भी समझ में नहीं आया कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने जब-जब भी इस बारे में किसी से बात करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि ऐसा बुरी बला या बुरी नज़र से बचने के लिए किया जाता है तो फिर सवाल उठता है कि भला ये नज़र लगने का मामला है क्या। कुछ लोग मानते हैं कि जिनके पास अमुक चीज़ नहीं होती वे दूसरों की चीज़ पर नज़र रखते हैं और उनकी बुरी नज़र का खामियाज़ा दूसरों को उठाना पड़ता है। टी.वी. पर भी कुछ विज्ञापन बुरी नज़र को लाल किरणों के रूप में दिखाते हैं मानो सचमुच में कोई किरण आँख से निकलकर चीज़ों तक जाती हो और फिर किसी जन्तर या किसी ताबीज़ को खरीदने-बेचने के लिए फोन नम्बर दिया रहता है। कुछ लोग इन सब बातों पर बिलकुल विश्वास नहीं करते और इन्हें अन्धविश्वास या झाँसे का नाम देकर सिरे से खारिज कर देते हैं। कोई कह सकता है कि यह श्रद्धा और विश्वास का मामला है, कोई माने या न माने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वगैरह-वगैरह। आपको इस बारे में क्या लगता है?
कुछ लोग मानते हैं कि जिनके पास अमुक चीज़ नहीं होती वे दूसरों की चीज़ पर नज़र रखते हैं और उनकी बुरी नज़र का खामियाज़ा दूसरों को उठाना पड़ता है। टी.वी. पर भी कुछ विज्ञापन बुरी नज़र को लाल किरणों के रूप में दिखाते हैं मानो सचमुच में कोई किरण आँख से निकलकर चीज़ों तक जाती हो और फिर किसी जन्तर या किसी ताबीज़ को खरीदने-बेचने के लिए फोन नम्बर दिया रहता है। कुछ लोग इन सब बातों पर बिलकुल विश्वास नहीं करते और इन्हें अन्धविश्वास या झाँसे का नाम देकर सिरे से खारिज कर देते हैं। कोई कह सकता है कि यह श्रद्धा और विश्वास का मामला है, कोई माने या न माने इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वगैरह-वगैरह। आपको इस बारे में क्या लगता है?
क्या इस तरह के सवालों पर स्कूल में बात होनी चाहिए? अगर नहीं तो क्यों नहीं और अगर हाँ तो क्यों और क्या बात होनी चाहिए?
खैर, आगे बढ़ने से पहले यहाँ मैं एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के अनुभव का भी ज़िक्र कर देना चाहता हूँ जिसमें कुछ लोगों ने नज़र लगने से सम्बन्धित विश्वासों की जाँच-पड़ताल करने का काम चुना और 2-3 दिन लगाकर जो भी प्रयोग किए या लोगों से बातचीत की, उसे अन्य शिक्षकों के सामने प्रस्तुत किया। गौरतलब हो कि ये सभी शिक्षक विज्ञान पढ़ाने वाले थे तो ज़ाहिर है इन विश्वासों को अन्धविश्वास कहने का एक दबाव तो वे महसूस कर ही रहे थे। पर फिर भी कुछ शिक्षकों ने व्यक्तिगत अनुभवों से जोड़कर अपनी बात रखी और मन के अन्तर्द्वन्द्व को सबसे साझा भी किया। इस दौरान एक सवाल यह भी निकल कर आया कि क्या नज़र लगने जैसे विश्वासों की जाँच-पड़ताल विज्ञान की कक्षा या विज्ञान के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में की जानी चाहिए या इन्हें विज्ञान की कक्षा से बाहर ही रखना उचित है? आखिर ये भी तो एक तरह के विश्वास ही हैं तो क्या इनकी जाँच-पड़ताल विज्ञान के दायरे में रहकर नहीं की जा सकती?
शिक्षकों की धारणाएँ, शिक्षकों की ज़ुबानी
जून 2013 के इस प्रशिक्षण में जिन साथियों ने नज़र लगने की जाँच-पड़ताल की ज़िम्मेदारी उठाई, उन्होंने जल्द ही यह एहसास कर लिया कि नज़र लगने से सम्बन्धित कई मान्यताएँ और धारणाएँ प्रचलन में हैं। तो सबसे पहली बात तो यह तय हुई कि इन मान्यताओं और धारणाओं को थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझ लिया जाए जिसके लिए कुछ सवाल तय किए गए, मसलन नज़र लगने से आप क्या समझते हैं, कैसे पता चलता है कि नज़र लगी है, नज़र कौन लगा सकता है, नज़र किस-किसको लगती है, नज़र से बचने के क्या तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, अगर लोग मानते हैं कि किसी को नज़र लगी है तो उसे उतारने के लिए वे क्या-क्या करते हैं और आपको क्या लगता है - नज़र लगती है कि नहीं? ज़ाहिर है कि इस सर्वे की कुछ सीमाएँ हैं जैसे जाँच-पड़ताल के हर-एक तरीके की होती हैं। मसलन, जवाब पढ़कर यह पता लगाना मुश्किल है कि सर्वे में पूछे गए सवालों को जवाब देने वालों ने ठीक से समझा भी था या नहीं। इसी तरह अगर सर्वे में पूछे गए प्रश्न का किसी ने कोई जवाब एक बार लिखकर दे दिया है तो उस पर आगे पूछताछ की गुंजाइश काफी कम रहती है। यह पता लगाना भी मुश्किल है कि जवाब देने वाले ने क्या सोचकर वह जवाब दिया है। पर फिर भी किसी चीज़ की जाँच करने के एक तरीके के तौर पर इसमें काफी सम्भावनाएँ हैं और नज़र लगने के सन्दर्भ में जहाँ शुरुआत प्रचलित मान्यताओं और विश्वासों को व्यवस्थित तरीके से समझने से करने का तय किया गया था, वहाँ इसका उपयोग इतना भी अटपटा नहीं है।
मोटे तौर पर जो बातें इस सर्वे से निकल कर आईं, वे कुछ इस प्रकार हैं-
* आम तौर पर ऐसा माना जाता है कि बच्चों, जानवरों, रिश्तों, पौधों, सम्पत्ति जैसे - नई गाड़ी, घर, दुकान, खेत आदि को नज़र लगने की सम्भावना ज़्यादा होती है। खाने पर भी नज़र लगती है और नज़र कोई भी लगा सकता है।
* लोगों का यह भी मानना था कि नज़र कुछ परिस्थितियों में ज़्यादा लगती है, जैसे - घर में नया सामान आने पर, बहुत सज-सँवर कर बाहर निकलने पर, सबके सामने खूब सारा खाना खाने पर, सफेद चीज़ (जैसे- दूध या दही) खाने पर, सबके सामने बहुत तारीफ मिलने पर, मर्दानगी का दिखावा करने पर (जैसे नंगे बदन बाहर घूमने पर), लड़कियों द्वारा लम्बे बालों का दिखावा करने पर आदि। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग औरों की सफलता, यश या सम्पत्ति से ईर्ष्या करते हैं। इसी बात को कुछ लोगों ने समाज में गैर-बराबरी को ज़िम्मेदार ठहराते हुए कहा। अब चूँकि महज़ किसी शब्द के इस्तेमाल से यह नहीं कहा जा सकता कि उसके पीछे की समझ क्या है, ऐसा लगता है कि इस पर उनके साथ थोड़ी और बातचीत की जानी चाहिए थी जो कई कारणों से नहीं हो पाई। आगे कभी अगर इस तरह का अध्ययन किसी और समूह के साथ हो तो उस समय यह किया जा सकता है।
* यह पूछे जाने पर कि नज़र लगने का पता कैसे चलता है, कई तरह के जवाब सामने आए। व्यक्ति के व्यवहार में अचानक बदलाव आने को कई लोगों ने नज़र लगने का प्रमुख लक्षण बताया। नज़र लगने पर न केवल शारीरिक समस्याएँ जैसे - लम्बी बीमारी, नींद के झटके, दुबलापन, पेट में दर्द आदि पैदा होती हैं बल्कि तमाम भावुक समस्याएँ जैसे- गम्भीर उदासी, निराशा (depressionù), चिड़चिड़ाहट, गुस्सा आदि भी व्यक्ति को घेर लेती हैं। सम्बन्धों में भी अक्सर समस्या आने लगती है और इन्हीं सबसे पता चलता है कि नज़र लगी है या नहीं।
* ऐसा पता चला कि नज़र से बचने के लिए तमाम टोटके अपनाए जाते हैं, जैसे ताबीज़ पहनना, बच्चों को काजल या काला टीका लगाना, काला धागा पहनाना, गाड़ी के पीछे जूते-चप्पल टाँगना, अँगूठी पहनना आदि।
* नज़र उतारने के लिए भी कई लोक-प्रचलित उपाय सुझाए गए। इसमें झाड़-फूँक, भभूति, मंत्रजाप, बलि, सिलबट्टे को सिर से घुमाकर घर की देहरी पर पटकना, राई-नमक-खड़ी मिर्च को एक साथ लेकर तथाकथित नज़र लगे हुए व्यक्ति के सिर से घुमाकर आग में झोंकना, अंगार में हल्दी और तेल डालकर नज़र उतारना वगैरह कुछ प्रचलित मान्यताएँ हैं। इसी तरह किसी ने बताया कि मिर्ची, नमक, राई, हल्दी, आटा, झाड़ू की सींक, रेत और बाल को एक कागज़ में बाँधकर एक लोटे में रख लो और तथाकथित नज़र लगे हुए व्यक्ति के सिर से घुमाकर लोटे को एक ताज़ा गोबर भरी थाली में कुछ समय के लिए रखो तो पता चल जाएगा है कि नज़र लगी है या नहीं। अगर लोटा थाली से चिपक गया तो इसका मतलब है कि नज़र लगी है, वरना नहीं। उन्हीं ने बताया कि एक बार मालूम चल जाए कि नज़र लगी है तो फिर उसी कागज़ की पुड़िया को आग में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से अगर बदबू आती है तो इसका मतलब है नज़र नहीं उतरी, वरना समझो काम बन गया।
सर्वे से मिली इस जानकारी से ऐसा लगता है कि नज़र लगने की बात काफी गहराई से हमारे समाज में बैठी है और इसके बारे में कुछ भी पुख्ता कहने से पहले इसे और खंगालने की ज़रूरत है। चूँकि यह सर्वे विज्ञान प्रशिक्षण में आए कुछ 20-25 शिक्षकों के साथ ही किया गया था, वैसे भी इससे कोई सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता।
यहाँ यह भी सावधान कर देना ज़रूरी है कि ये कुछ मान्यताएँ और धारणाएँ हैं जो अलग-अलग लोगों ने एक शिक्षक प्रशिक्षण के दौरान साझा कीं, कौन कितनी सही है, यह ठीक-ठीक पता किए बगैर इन्हें अपनाने की भूल ना करें। कई बार तबियत खराब होने पर अगर मरीज़ को अलग-अलग टोटकों में उलझाए रखा जाए तो आसानी से ठीक हो सकने वाली बीमारी भी गम्भीर रूप धारण कर लेती है।
कुछ सफल तो कुछ असफल प्रयास
समूह के अन्दर उत्साहित कुछ लोगों ने नज़र उतारने के लिए आए आखिरी सुझाव को जाँचने का सोचा। हालाँकि समूह के ही कुछ और लोगों ने यह भी कहा कि जब तक नज़र लगने के बारे में कुछ स्पष्ट दावा न हो यानी कि पक्के से पता न हो कि नज़र लगी भी है या नहीं, तब तक प्रयोग से किस बात की जाँच की जाएगी, यह कहा नहीं जा सकता और इसलिए इससे जुड़ी बातों को प्रयोग करके जाँचने का कोई मतलब ही नहीं है। पर कुछ लोगों का मानना था कि नज़र लगने से जुड़े सुझाव बनावटी बातें मात्र हैं, ऐसा कुछ नहीं होता और प्रयोग करके हम इस बात का पता लगा सकते हैं। इसलिए समूह के दो हिस्से हो गए। जहाँ एक उप-समूह ने इस बात पर समझ बनाने की कोशिश जारी रखी कि विज्ञान किस तरह के प्रश्नों के जवाब दे सकता है और किस तरह के प्रश्न विज्ञान के दायरे में नहीं आते, वहीं दूसरे उप-समूह ने प्रयोग करने का फैसला किया। हालाँकि उन्हें भी यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि प्रयोग में क्या जाँचकर देखना चाहते हैं। खैर, सुझाव के अनुसार उन्होंने एक थाली में ताज़ा गोबर लेकर एक लोटे में सभी ज़रूरी सामान भरकर लोटे को थाली में कुछ समय के लिए उल्टा रखा (चित्र-1) और कुछ घण्टे चिपकने का इन्तज़ार भी किया। उनका ऐसा अनुमान था कि लोटा आराम से थाली में चिपक जाएगा और पता चल जाएगा कि लोटे के चिपकने का नज़र लगने से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि नज़र लगे हुए व्यक्ति के बगैर भी लोटा थाली में चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी खुली मानसिकता से इस प्रयोग को नहीं कर रहे थे। अब उनके दिमाग में जो भी रहा हो, फिलहाल लम्बे इन्तज़ार के बाद भी लोटे ने चिपकने का नाम नहीं लिया। ज़ाहिर है कि इसके आधार पर नज़र लगने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
इसलिए समूह के दो हिस्से हो गए। जहाँ एक उप-समूह ने इस बात पर समझ बनाने की कोशिश जारी रखी कि विज्ञान किस तरह के प्रश्नों के जवाब दे सकता है और किस तरह के प्रश्न विज्ञान के दायरे में नहीं आते, वहीं दूसरे उप-समूह ने प्रयोग करने का फैसला किया। हालाँकि उन्हें भी यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि प्रयोग में क्या जाँचकर देखना चाहते हैं। खैर, सुझाव के अनुसार उन्होंने एक थाली में ताज़ा गोबर लेकर एक लोटे में सभी ज़रूरी सामान भरकर लोटे को थाली में कुछ समय के लिए उल्टा रखा (चित्र-1) और कुछ घण्टे चिपकने का इन्तज़ार भी किया। उनका ऐसा अनुमान था कि लोटा आराम से थाली में चिपक जाएगा और पता चल जाएगा कि लोटे के चिपकने का नज़र लगने से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि नज़र लगे हुए व्यक्ति के बगैर भी लोटा थाली में चिपक जाता है। ऐसा लगता है कि वे भी खुली मानसिकता से इस प्रयोग को नहीं कर रहे थे। अब उनके दिमाग में जो भी रहा हो, फिलहाल लम्बे इन्तज़ार के बाद भी लोटे ने चिपकने का नाम नहीं लिया। ज़ाहिर है कि इसके आधार पर नज़र लगने के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।
अगर लोटा सच में चिपक जाता तो भी नज़र लगने वाला दावा खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि दावे में नज़र लगे हुए व्यक्ति के सिर के चारों ओर घुमाने का भी ज़िक्र था और प्रयोग में तो ऐसा किया ही नहीं गया था। मतलब यह कि प्रयोग के डिज़ाइन में ही गलती थी। अगर इस प्रयोग को नज़र लगने का पता लगाने के परीक्षण के रूप में देखें तो टेस्ट की जाँच के लिए हमें कम-से-कम दो ऐसे समूह चाहिए होंगे जिनमें से एक समूह के लोगों को पक्के तौर पर नज़र लगी हो और दूसरे समूह के लोगों को पक्के तौर पर नज़र न लगी हो, और दोनों समूहों के साथ टेस्ट करके देखा जाए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि टेस्ट करने वाले को पता न हो कि वे किस समूह के व्यक्ति का टेस्ट कर रहे हैं। फिर किसी को पक्के तौर पर नज़र लगी भी है या नहीं, इसका पता किसी और तरीके से करना होगा, वरना तो बात गोल-गोल घूमती रह जाएगी।
खैर, इस पहली असफलता के बाद भी इस उप-समूह का मनोबल कम नहीं हुआ। उन्होंने नज़र उतारने के लिए दिए गए सुझाव को भी जाँचने का फैसला किया। इस बार भी दूसरे उप-समूह के लोगों ने समझाने की कोशिश की कि जब तक यह तय नहीं हो कि पक्के से नज़र लगी है या नहीं, तब तक नज़र उतरी या नहीं, इसका पता कैसे चल सकता है और चूँकि नज़र लगने के बारे में साफ-साफ कुछ कहा ही नहीं जा रहा है तो किस बात की जाँच होगी, यह स्पष्ट नहीं है। पर इस समूह के लोगों ने सोचा कि सुझाई गई सभी चीज़ों (मिर्ची, नमक, राई, हल्दी, आटा, झाड़ू की सींक, रेत और बाल) को मिलाकर एक बार जलाकर तो देखना ही चाहिए कि बदबू आती भी है या नहीं। तो भले ही यह बहुत स्पष्ट नहीं था कि इससे क्या पता चलेगा, उन्होंने इन सभी चीज़ों को एक साथ बाँधकर जलाया और पाया कि कोई खास बदबू नहीं आती है (चित्र-2)। जहाँ मन में एक ओर यह सन्तोष था कि चलो जो चाहते थे, वह करके देख लिया, वहीं नज़र लगने के बारे में कुछ खास समझ नहीं बन पाने का मलाल भी।  तर्कों के दाँव-पेंच समझना शायद इतना आसान मामला भी नहीं है। कई बार हम जोश में बहुत कुछ कह जाते हैं और उसी धुन में कुछ-का-कुछ कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि वह कितना तर्कसंगत है, इस उप-समूह में कुछ ऐसा ही चल रहा था। खैर, बाद में लम्बी बातचीत के दौरान दूसरा उप-समूह कुछ हद तक इस समूह को समझा पाने में सफल रहा कि नज़र लगने का मामला काफी पेचीदा है। यह कुछ ऐसी मान्यताओं का पुलिन्दा है जो एक खास तरह के विश्वास पर आधारित हैं, और इनकी जाँच वैज्ञानिक तरीकों से नहीं की जा सकती। पर क्यों नहीं, इस सवाल पर आगे की चर्चा में थोड़ी बातचीत की जाएगी, पर फिलहाल विज्ञान शिक्षण के लिए इस सबके क्या मायने हैं, वह भी थोड़ा सोच लेते हैं, खास तौर पर विज्ञान की कक्षा में इन सवालों पर बात करने या न करने का क्या मतलब है।
तर्कों के दाँव-पेंच समझना शायद इतना आसान मामला भी नहीं है। कई बार हम जोश में बहुत कुछ कह जाते हैं और उसी धुन में कुछ-का-कुछ कर जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि वह कितना तर्कसंगत है, इस उप-समूह में कुछ ऐसा ही चल रहा था। खैर, बाद में लम्बी बातचीत के दौरान दूसरा उप-समूह कुछ हद तक इस समूह को समझा पाने में सफल रहा कि नज़र लगने का मामला काफी पेचीदा है। यह कुछ ऐसी मान्यताओं का पुलिन्दा है जो एक खास तरह के विश्वास पर आधारित हैं, और इनकी जाँच वैज्ञानिक तरीकों से नहीं की जा सकती। पर क्यों नहीं, इस सवाल पर आगे की चर्चा में थोड़ी बातचीत की जाएगी, पर फिलहाल विज्ञान शिक्षण के लिए इस सबके क्या मायने हैं, वह भी थोड़ा सोच लेते हैं, खास तौर पर विज्ञान की कक्षा में इन सवालों पर बात करने या न करने का क्या मतलब है।
नज़र का फेर और विज्ञान शिक्षण
विज्ञान की कक्षा में इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए या नहीं, यह एक विवादित मुद्दा है। जैसे कोई कह सकता है कि विज्ञान की कक्षा में सिर्फ उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिनके जवाब विज्ञान में उपयोग किए जाने वाले तरीकों का इस्तेमाल करके ढूँढ़े जा सकते हैं - मसलन चीज़ों के ज़मीन पर गिरने की घटना को समझना हो या पदार्थ की प्रकृति को, जीवों के व्यवहार से जुड़ी बातें हों या पौधों के। पर जिन बातों के जवाब विज्ञान के तरीकों का इस्तेमाल करके नहीं दिए जा सकते, जैसे 3 अ 2 उ 5 होता है कि नहीं, या पानीपत की दूसरी लड़ाई में फलाँ राजा ने फलाँ राजा को हराया था कि नहीं, जीवन क्या है, या हमारे अस्तित्व का क्या अर्थ है जैसे सवालों की जाँच गणित, इतिहास या दर्शन शास्त्र जैसे विषयों पर छोड़ देनी चाहिए और वहीं तक सीमित रहनी चाहिए।
पर मेरा मानना है कि इस तरह के सवालों पर भी विज्ञान की कक्षा में ज़रूर बात होनी चाहिए क्योंकि इन बातों से ही पता चलता है कि विज्ञान किस तरह के सवालों के जवाब हमें दे सकता है और किस तरह के सवाल विज्ञान के दायरे में नहीं आते। आखिर विज्ञान सीखना मतलब सिर्फ परिभाषाएँ, सूत्र, समीकरण सीखना या कुछ अवधारणाओं की मदद से प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या कर पाना भर नहीं है। यह भी सीखना उतना ही ज़रूरी है कि विज्ञान (और अन्य विषयों) की सीमाएँ क्या हैं, ये सीमाएँ कितनी जायज़ हैं, विज्ञान (और अन्य विषयों) में किसी बात को जाँचने के तरीके क्या हैं, क्या विज्ञान हमारे हर सवाल का जवाब दे सकता है, विज्ञान इतने विश्वास के साथ कोई बात कैसे कहता है, उसमें गलती की कितनी सम्भावनाएँ हैं आदि-आदि।
नज़र लगने से जुड़ी धारणाएँ एवं मान्यताएँ भी इस बात का एक जीता-जागता उदाहरण हैं कि हर बात की जाँच विज्ञान के तरीकों का इस्तेमाल करके नहीं की जा सकती। पर इसका मतलब यह भी नहीं कि नज़र लगना, गणित की बुनियादी समस्याएँ और दर्शन की बातें एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं। जहाँ गणित, इतिहास या दर्शन में किसी बात की प्रामाणिकता को जाँचने के अलग आधार तय हैं, नज़र लगने से जुड़ी धारणाओं को जाँचना सम्भव ही नहीं है, कम-से-कम विज्ञान के तरीकों से तो नहीं क्योंकि कोई स्पष्ट बात कभी कही ही नहीं जाती।
विज्ञान के एक प्रमुख दर्शनशास्त्री कार्ल पॉपर (1902-1994) का मानना था कि सिर्फ उन्हीं कथनों और सिद्धान्तों को विज्ञान के दायरे में माना जाएगा जो उनकी जाँच के लिए एक अनूठा (distinctive) प्रयोग सुझाते हों और स्पष्ट दावा करते हों कि जाँच करने पर फलाँ नतीजा आएगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कथन/सिद्धान्त गलत साबित हो जाएगा। यानी कि विज्ञान में दो ही तरह की बातें सम्भव हैं। या तो कथन/सिद्धान्त पहले ही खण्डित किया जा चुका है या अभी तक खण्डित नहीं हुआ है, पर खण्डन योग्य है।
अगर ऐसा स्पष्ट दावा किया ही न जाए या और किए गए दावे के गलत साबित होने पर अपनी बात को किसी-न-किसी तरह से मनवाने की कोशिश जारी रहे या बच निकलने के रास्ते ढूँढ़े जाते रहें, तो उस बात को अवैज्ञानिक या विज्ञान के दायरे के बाहर की बात ही माना जाएगा। पर अगर दावा ऐसा है कि उसे जाँचा ही नहीं जा सकता तो वह अवैज्ञानिक तो है ही, निरर्थक भी है।
किसी कथन/सिद्धान्त को वैज्ञानिक करार दिए जाने की यह शर्त काफी कड़ी तो है पर वैज्ञानिकों के बीच काफी लोकप्रिय भी। हालाँकि बाद के दर्शनशास्त्रियों ने इस पर कई सवाल उठाए हैं, पर वह चर्चा फिर कभी। आप चाहें तो नैशनल बुक ट्रस्ट द्वारा सम्पादित सुन्दर सरूकाई की किताब ‘What is Science’ के पहले अध्याय में इस चर्चा की और बारीकियों को देख सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए हम नज़र लगने के सवाल पर थोड़ा और ध्यान देते हैं।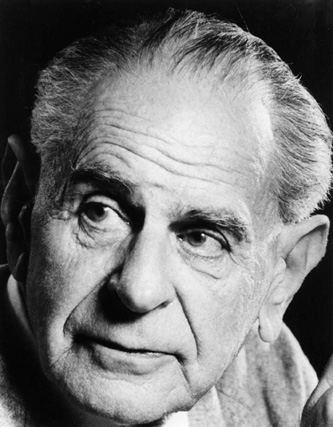 दरअसल, पॉपर की मानें तो दुकान के दरवाज़े पर बुरी बला से बचने के लिए नींबू-मिर्ची टाँगना और फिर भी बुरा हो जाने पर इस प्रचलन पर सवाल उठाने की बजाय दोष किसी और के मत्थे मढ़ देना, ऐसी एक धारणा है जिसे आसानी से अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। बड़े-बड़े मकानों की छत पर बुरी बला से बचने के लिए उल्टा मटका टाँगना, काली बिल्ली का रास्ता काटने पर अशुभ की आशंका से रुक जाना, किसी काम की शुरुआत से पहले छींक आ जाने पर काम रोक देना, या बुरी बलाओं से बचने के लिए तमाम तरह के मोती-माला, अँगूठियाँ वगैरह पहन कर रखना, ऐसे ही कुछ अवैज्ञानिक विश्वास हैं। अगर इन विश्वासों के विरुद्ध कुछ घटित होता है तो बहुत सारे किन्तु-परन्तु जाग उठते हैं। इन मूलभूत धारणाओं पर सवाल उठाने की बजाय लोग अक्सर कुछ और कारकों को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं और ये धारणाएँ जस-की-तस समाज में चलती रहती हैं। जैसे किसी विद्वान ज्योतिषी की बात मानकर एक खास तरह की अँगूठी पहनने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए तो भी लोग ज्योतिष पर सवाल उठाने की बजाय ज्योतिषी के पास फिर से पहुँच जाते हैं और ज्योतिषी अपनी गलत हुई भविष्यवाणी को ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति में आए अचानक फेर-बदल के रूप में समझा देते हैं। जहाँ कई लोगों को इससे उनकी ज़िन्दगी में होने वाली घटनाओं-दुर्घटनाओं को एक तरह से समझने और उनसे उबरने में मदद मिलती है और वे रोज़मर्रा की उबाऊ ज़िन्दगी और उसकी अनिश्चितताओं को कहीं आसानी से झेल पाते हैं, वहीं कई लोग इन विश्वासों को अपने फायदे और दूसरों का नुकसान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन सभी मान्यताओं को किसी-न-किसी कसौटी पर परखने की खासी ज़रूरत है।
दरअसल, पॉपर की मानें तो दुकान के दरवाज़े पर बुरी बला से बचने के लिए नींबू-मिर्ची टाँगना और फिर भी बुरा हो जाने पर इस प्रचलन पर सवाल उठाने की बजाय दोष किसी और के मत्थे मढ़ देना, ऐसी एक धारणा है जिसे आसानी से अवैज्ञानिक कहा जा सकता है। बड़े-बड़े मकानों की छत पर बुरी बला से बचने के लिए उल्टा मटका टाँगना, काली बिल्ली का रास्ता काटने पर अशुभ की आशंका से रुक जाना, किसी काम की शुरुआत से पहले छींक आ जाने पर काम रोक देना, या बुरी बलाओं से बचने के लिए तमाम तरह के मोती-माला, अँगूठियाँ वगैरह पहन कर रखना, ऐसे ही कुछ अवैज्ञानिक विश्वास हैं। अगर इन विश्वासों के विरुद्ध कुछ घटित होता है तो बहुत सारे किन्तु-परन्तु जाग उठते हैं। इन मूलभूत धारणाओं पर सवाल उठाने की बजाय लोग अक्सर कुछ और कारकों को ज़िम्मेदार ठहराने लगते हैं और ये धारणाएँ जस-की-तस समाज में चलती रहती हैं। जैसे किसी विद्वान ज्योतिषी की बात मानकर एक खास तरह की अँगूठी पहनने के बाद भी अगर कुछ गलत हो जाए तो भी लोग ज्योतिष पर सवाल उठाने की बजाय ज्योतिषी के पास फिर से पहुँच जाते हैं और ज्योतिषी अपनी गलत हुई भविष्यवाणी को ग्रहों-नक्षत्रों की स्थिति में आए अचानक फेर-बदल के रूप में समझा देते हैं। जहाँ कई लोगों को इससे उनकी ज़िन्दगी में होने वाली घटनाओं-दुर्घटनाओं को एक तरह से समझने और उनसे उबरने में मदद मिलती है और वे रोज़मर्रा की उबाऊ ज़िन्दगी और उसकी अनिश्चितताओं को कहीं आसानी से झेल पाते हैं, वहीं कई लोग इन विश्वासों को अपने फायदे और दूसरों का नुकसान करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसलिए इन सभी मान्यताओं को किसी-न-किसी कसौटी पर परखने की खासी ज़रूरत है।
यहाँ जो एक और महत्वपूर्ण बात है, वह यह कि जहाँ एक ओर इन मान्यताओं, विश्वासों और प्रचलनों को अवैज्ञानिक कहकर हाशिए पर धकेला जा सकता है, सिरे से नकारा जा सकता है, वहीं पर सवाल यह भी उठता है कि तेज़ी से बदलती इस बिलकुल असम्भावित-सी दुनिया में होने वाली घटनाओं को समझने के लिए विज्ञान किस सीमा तक हमारा साथ दे सकता है। क्या वैज्ञानिक तर्क भी एक सीमा के बाद इन अनिश्चितताओं को समझा पाते हैं? ऐसे में वैकल्पिक प्रयासों के लिए हमारे समाज में क्या जगह है?
जैसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान (modern medicine) या ऐलोपैथी के बदले में आज ढेरों विकल्प मौजूद हैं पर सभी कहीं-न-कहीं अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या सभी बातों को विज्ञान द्वारा प्रमाणित तर्कों की कसौटी पर ही खरा उतरना ज़रूरी है? भावनाओं, सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विश्वासों को वैज्ञानिक तर्कों के सापेक्ष कैसे देखा जाना चाहिए? वैज्ञानिक तर्क को सामाजिक मान्यताओं और सांस्कृतिक विश्वासों से ऊँचा स्थान देना कितना जायज़ है? पर इसका मतलब क्या यह हुआ कि सभी विश्वास और मान्यताएँ वैज्ञानिक तर्क के समतुल्य समझी जानी चाहिए? हरगिज़ नहीं।
उदाहरण के तौर पर, कुछ खास तरह के सांस्कृतिक विश्वासों को ही ले लीजिए जो आर्थिक और राजनैतिक हित की भावनाओं से ओत-प्रोत होते हैं और अक्सर समाज में काफी कट्टरपन्थी रूप धारण कर लेते हैं, जैसे जाति, धर्म या लिंग आधारित भेदभाव और उससे जुड़ी हिंसा का मामला। निश्चित ही ऐसे विश्वासों, धारणाओं और प्रचलनों पर हम सभी को सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है पर इसके चलते हम सभी सांस्कृतिक विश्वासों और प्रचलनों को तो एक ही कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। कई और विश्वास भले ही वे अवैज्ञानिक हों, पर किसी को सीधा नुकसान नहीं पहुँचाते बल्कि कई स्तर पर लोगों को ज़िन्दगी से जूझने में मदद ही करते हैं, ऐसे विश्वासों और प्रचलनों के प्रति शायद थोड़ा नरम रवैया अपनाया जा सकता है। जैसे काफी समय तक बारिश न होने पर किसानों का किसी देवी-देवता की पूजा करना, बलि देना और यह उम्मीद करना कि जल्द ही बारिश होगी और उनके दुख-दर्द मिट जाएँगे, अस्पताल में किसी निकट सम्बन्धी के भर्ती होने पर भगवान से प्रार्थना करना कि सब जल्दी ठीक हो जाए वगैरह।
फिर वैज्ञानिक तर्क एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण इनमें से कुछ मुद्दों पर सवाल उठाने, उन पर समझ बनाने और प्रतिक्रिया करने में मददगार तो हो सकता है पर चँूकि इन सभी चीज़ों का एक संरचनात्मक आधार है, तो उन संरचनाओं और सामाजिक ढाँचों पर समझ बनाए बगैर किए गए प्रयास किसी ठोस बदलाव की ओर नहीं ले जा सकते। जैसे लड़का या लड़की पैदा करना गर्भवती महिला के हाथ में ना होने के बावजूद अक्सर महिला को ही उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाता है और इसके चलते उसे कई लांछन और प्रताड़नाएँ सहनी पड़ती हैं। हालाँकि विज्ञान की दृष्टि से देखें तो लिंग निर्धारण एक प्राकृतिक घटना है और उसमें पुरुष या महिला का कोई नियंत्रण नहीं है, पर समाज में इस बात की इतनी गहरी पैठ को समझने और उसे झकझोरने के लिए समाज के पितृसत्तात्मक ढाँचे को समझे बगैर कोई बात नहीं हो सकती।
ऐसे में मुझे लगता है कि विज्ञान और ज्ञान के अन्य रूपों को कहीं अधिक संवेदनशील तरीके से आपस में संवाद करने की ज़रूरत है। एक-दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोलने की बजाय एक-दूसरे के साथ मिलकर मानवता के हित में काम करने की ज़रूरत है।
इसलिए वैज्ञानिकों को, और सिर्फ वैज्ञानिकों को ही क्यों, हम सभी को विकल्पों को सिरे से खारिज करने की बजाय उन पर गौर फरमाने और उनके जाँच के तरीकों को धैर्य के साथ समझने की ज़रूरत है। हो सकता है इन प्रयासों से कोई और कड़ी हमारे हाथ लग जाए और हम अलग-अलग समुदायों में प्रचलित मान्यताओं और विश्वासों के प्रति थोड़ा संवेदनशील दृष्टिकोण रखते हुए कहीं बेहतर विज्ञान कर सकें।
इस लेख में मैंने यह चर्चा करने की कोशिश की है कि कुछ शिक्षकों ने एक प्रशिक्षण के दौरान नज़र लगने से जुड़े अपने सवाल की जाँच-पड़ताल कैसे की और उसके चलते विज्ञान के दायरे के बारे में क्या समझ बनाई। आगे कुछ चर्चा इस बात पर हुई कि विज्ञान शिक्षा के लिए इसके क्या मायने हैं। आप इस चर्चा से कितना सहमत हैं? क्या इस तरह के सवालों पर भी विज्ञान की कक्षा में बात होनी चाहिए? अगर हाँ, तो बताइए कि दी हुई पाठ्यचर्या में इस तरह की बातचीत के लिए कहाँ-कहाँ गुंजाइश है? और अगर आपको लगता है कि इसे विज्ञान की कक्षा से बाहर ही रखना चाहिए तो अपना जवाब अपने तर्क के साथ हमें ‘संदर्भ’ के पते पर भेजिए।
हिमांशु श्रीवास्तव: होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, मुम्बई में शोध छात्र। एकलव्य के विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से भी जुड़े हैं।
आभार: उन सभी शिक्षकों का जिन्होंने सर्वे में अपनी राय व्यक्त की और अपने अनुभव साझा किए और समूह के उन सभी साथियों का जिन्होंने प्रशिक्षण के दौरान इस काम का बीड़ा उठाया और उसे एक अंजाम तक पहुँचाया - खास तौर पर मोना, सीमा, श्रेया और आलोका का, जिन्होंने इस काम की प्रमुख ज़िम्मेदारी वहन की। इनके अलावा भी कई साथी बीच-बीच में समूह में आते-जाते रहे और काम को आगे बढ़ाने में उनके सुझाव भी काफी महत्वपूर्ण रहे। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में विज्ञान शिक्षण पर शोध कर रही अश्वति रवीन्द्रन ने इस लेख पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए और लेख को आकार देने में भी काफी योगदान दिया। एकलव्य के प्रकाशन समूह ने काफी बारीकी से लेख को पढ़ा और इसे कसने में उनका बहुत सहयोग रहा।


