संजय खाती
कहानी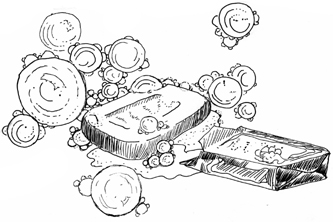 हमारे गाँव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साबुन का नाम हमने और दूसरे लोगों ने सुना ज़रूर था लेकिन दो-चार ही लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उसे सचमुच में देखा हो। साबण का नाम भी लोगों को मालूम था तो सिर्फ कुछ फौजियों की बदौलत। और थोड़ा इसलिए भी कि जब एक बार डिप्टी साहब की बिटिया पिण्टी गाँव आई थी तो उसके पास कुछ औरतों ने यह चीज़ देखी थी। कहते हैं कि पिण्टी जहाँ खड़ी हो उससे एक कोस दूर तक फूलों की-सी बास महकती थी। दस-पन्द्रह साल बाद भी लोगों को वह पिण्टी याद रही तो इसी वजह से। लोग साबुन का ज़िक्र इतर और फुलेल के बाद करते थे।
हमारे गाँव में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। साबुन का नाम हमने और दूसरे लोगों ने सुना ज़रूर था लेकिन दो-चार ही लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उसे सचमुच में देखा हो। साबण का नाम भी लोगों को मालूम था तो सिर्फ कुछ फौजियों की बदौलत। और थोड़ा इसलिए भी कि जब एक बार डिप्टी साहब की बिटिया पिण्टी गाँव आई थी तो उसके पास कुछ औरतों ने यह चीज़ देखी थी। कहते हैं कि पिण्टी जहाँ खड़ी हो उससे एक कोस दूर तक फूलों की-सी बास महकती थी। दस-पन्द्रह साल बाद भी लोगों को वह पिण्टी याद रही तो इसी वजह से। लोग साबुन का ज़िक्र इतर और फुलेल के बाद करते थे।
पिण्टी तो खैर जैसे किसी दूसरी दुनिया से आई जीव थी। गाँव के किसी आदमी के पास कभी साबुन नहीं देखा गया। सच्चे अर्थों में गाँव में पहला साबुन आया मेरे पास। और वह भी अचानक, अप्रत्याशित रूप से।
उस दिन पन्द्रह अगस्त था ऐसा ही कुछ खास दिन रहा होगा क्योंकि स्कूल बन्द था। मैं और काका आलू बेचने के लिए कई कोस चलकर कस्बे में आए थे। काका मुझसे पाँच-सात साल ही बड़ा होगा। हम दोनों लगभग दोस्त जैसे ही थे। हालाँकि कभी-कभी वह बड़प्पन जताने को उत्सुक हो जाता था, लेकिन उसका कोई दबदबा मुझ पर नहीं बन पाया।
तो कस्बे की रौनक से विभोर हम लोग लेमनचूस चाटते भटक रहे थे कि एक भीड़-भरे मैदान में जा पहुँचे। वहाँ बिलकुल मेला-सा लगा था। खूब शोर हो रहा था। सीटियाँ बज रही थीं। एक भोंपे से किसी आदमी की ज़ोरदार आवाज़ आ रही थी जैसे डाँट रहा हो।
हम अचकचाए...से और बिलकुल बेध्यानी में उस भीड़ में घुसे जा रहे थे कि अचानक मैंने पाया, मैं अपने जैसे लड़कों की एक कतार में खड़ा हूँ। किसी ने बाँह पकड़कर जल्दी में मुझे वहाँ खड़ा कर दिया था। एक आदमी सबको सफेद लाइन पर खड़ा कर रहा था। मेरे दोनों ओर लड़के चिल्ला रहे थे। झपटने की मुद्रा में बार-बार एक टाँग पर झुक रहे थे।
पहले तो मैं घबरा ही गया। इधर-उधर देखा तो काका का कहीं पता ही नहीं। लाठी वालों ने बाकी भीड़ के साथ उसे भी धकिया दिया होगा। अब भोंपे पर गिनती गिनी जा रही थी। एक...दो... और तीन! भूखे जानवरों की तरह सब भागे। साथ में मैं भी। पहले तो कुछ सूझा ही नहीं, पर जब देखा कि बगल वाला छोकरा अपनी सींकिया टाँगें पटकता आगे निकला जा रहा है तो मैं भी भाग लिया दम तोड़कर। ऐसा कि मैदान के दूसरे छोर पर बँधी रस्सी से उलझकर गिर पड़ा। घुटने में लगी सो अलग। झाड़कर खड़ा हुआ तो तालियाँ। चमचमाती डिबिया थमा दी।
भीड़ में जाने कहाँ से काका हँसता हुआ प्रकट हो गया। अब हम दोनों साथ-साथ हँसे जा रहे थे। मेरा मन हो रहा था कि अभी खूब दौड़ूँ। दौड़ता ही जाऊँ। आगे-आगे कुलाँचें मारता मैं भागा तो काका भी हाँफता हुआ आया पीछे-पीछे। कस्बा पीछे छूट गया। मैं गाँव की ओर सरपट भागा जा रहा था। काका आवाज़ देने लगा। आखिर में नदी के पास मैं रुका तो उसने मुझे पकड़ लिया।
काका ने कहा, “क्या है रे?”
तब जाकर मुझे ख्याल आया कि वह लाल चमकती डिबिया मेरे हाथ में है। काका ने झट उसे छीन लिया और उलट-पलटकर देखने लगा। उसी को सबसे पहले सूझा कि ये तो साबण है। उसका चेहरा उत्तेजना से चमकने लगा था। वह बार-बार उसे सूँघता। माँगने पर भी नहीं देता। चिढ़कर बोलता, “खा नहीं रहा हूँ।” उसकी नीयत में खोट लगती थी।
मैं भड़क गया। आखिर वह मेरी चीज़ थी। मैंने काका से उसे छीनने की कोशिश की। उसे गिराने के लिए संघर्ष किया। लेकिन उस लम्बे खड़ूस से जीतना मेरे लिए नामुमकिन ही था। अब तक उसने बाहर की चमकीली पन्नी भी खोल दी थी और अन्दर की गुलाबी नाज़ुक टिकिया निकाल ली थी।
अन्तिम हथियार के तौर पर मैं धप से नदी के पत्थरों पर गिर गया। दहाड़ मारकर सचमुच रोने लगा, “मैं इजा से कह दूँगा हा...।”
हमेशा की तरह इस बार भी मेरी चाल कामयाब हुई। काका कुछ देर मुझे लाल आँखों से घूरता रहा, फिर ‘जा मर’ कहकर टिकिया फेंक दी। मैंने उसे लपक लिया। “पन्नी भी दे।” काका ने पन्नी भी फेंक दी। मैंने नाज़ुक टिकिया को फिर पन्नी में जतन से लपेटा और उसे सूँघता, हँसता हुआ घर की ओर चला।
 काका से पहली बार गहरी दुश्मनी की यह शुरुआत थी। उस वक्त तो मैं साबुन की उस भीनी खुशबू में इतना मगन था कि काका की ओर ध्यान देने का वक्त नहीं था मेरे पास, लेकिन आगे चलकर हम दोनों की दुश्मनी स्थाई हो गई।
काका से पहली बार गहरी दुश्मनी की यह शुरुआत थी। उस वक्त तो मैं साबुन की उस भीनी खुशबू में इतना मगन था कि काका की ओर ध्यान देने का वक्त नहीं था मेरे पास, लेकिन आगे चलकर हम दोनों की दुश्मनी स्थाई हो गई।
बहरहाल उस शाम काका पीछे-पीछे, पत्थरों को ठोकर मारता हुआ चला। घर पहुँचते ही मुँह टेढ़ा कर उसने ऐलानिया अन्दाज़ में कहा, “गोपिए को एक साबण क्या मिल गया, नीचे ही नहीं देख रहा आज।”
इजा गोबर समेट रही थी। खड़ी होकर बोली, “साबण! कहाँ से लाया रे? कैसा है? दिखा तो।”
“मेरा है।” मैंने तुनककर कहा।
इजा हाथ खूब साफ से धोकर आई, “दिखा तो। मैं भी देखूँ कैसा साबण है।”
मुझे अब किसी पर एतबार नहीं रह गया था। बहुत नखरे के साथ उँगलियाँ खोलीं इजा ने, बड़े शौक के साथ साबुन लिया। ढिबरी के पास ले जाकर गौर से देखा। दो-तीन बार सूँघा। बोली, “मैं नहाउँगी इससे।”
मैं चील की तरह झपटा। साबुन झपटकर अन्दर की जेब में ठूँसा। भागकर खड़ा हुआ बीस कदम दूर। इजा देखती रह गई। “मर तू। आग लगे तेरे साबण को।” उसने चिचियाकर कहा और आँखें तरेरती हुई वहाँ से चली गई।
इस तरह माँ मेरी दूसरी दुश्मन बनी। असल में साबुन की इस महत्ता को मैं पहले समझ ही नहीं पाया। शायद समझने की उम्र थी भी नहीं। लेकिन जल्द ही मुझे लगने लगा मानो मैं चारों ओर से दुश्मनों से घिर गया हूँ। मुझे मालूम था काका मेरी हर चीज़ को उलट-पलटकर देखता है। घर में जितने भी कनस्तर-डिब्बे हैं, सबको उसने टटोला है। यहाँ तक कि गोशाला के घास-पुआल को भी वह छान आया है। लेकिन साबुन कहाँ है यह मेरे अलावा कोई नहीं जान सका था।
हारकर काका ने मेरी चापलूसी करने की भी कोशिश की। लेकिन अब मैं उतना भोला नहीं रह गया था।
बापू को तो साबुन देखना नसीब ही नहीं हुआ। इजा और काका ने हर वक्त साबुन का ज़िक्र करके उनको इतना उकसा दिया था कि वे मारपीट पर उतर आए। पर अब तक मैंने जान लिया था कि जो भी साबुन देख लेगा, उसकी नीयत में खोट आ जाएगा। सो मैं भी टस-से-मस नहीं हुआ। हारकर बापू ने यह कहते हुए कि “बहुत इतर-फुलेल का शौक चढ़ा है, भेज दो साले को गाय चराने,” मुझे कसकर दो लातें मारीं।
मैं रोया नहीं और इस अपमान को पी लिया। लेकिन इस घड़ी से मुझे सन्देह होने लगा कि मैं उनका असली बेटा हूँ भी या नहीं।
कुन्ती को अलबत्ता एक दिन मेरी सख्त पहरेदारी में साबुन को छू-सूँघकर देखने का मौका मिला। कुन्ती तब से आँखें बड़ी-बड़ी किए मेरे पीछे-पीछे डोलती रहती है। उसे भगाने के लिए झापड़ों के अलावा कोई रास्ता नहीं होता।
इतने लोगों के बीच साबुन को बार-बार देख पाना मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा था। मेरी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी। हर दिन पहाड़-सा लगता। आखिरकार इतवार को जी कड़ा कर मैंने साबुन निकाल ही लिया और गर्म पानी लेकर नहाने बैठा।
यह साबुन से मेरा पहला स्नान होने जा रहा था। मैंने बड़े प्यार से पन्नी अलग की। एहतियात से धूप में रखी। साबुन को नरमी से दाएँ हाथ में पकड़ा और भीगे बालों को हौले-हौले छुआ।  गुलाबी टिकिया पर उभरे हुए अक्षर बने थे। मुझे अँग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन यह जो कुछ भी लिखा था, इससे साबुन की खूबसूरती बढ़ रही थी। वे मिटे नहीं, इसका ख्याल रखना था।
गुलाबी टिकिया पर उभरे हुए अक्षर बने थे। मुझे अँग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती थी, लेकिन यह जो कुछ भी लिखा था, इससे साबुन की खूबसूरती बढ़ रही थी। वे मिटे नहीं, इसका ख्याल रखना था।
काका कहने को तो चाख में बैठा पढ़ाई कर रहा था, लेकिन बार-बार उसका सिर खिड़की से दिखाई दे जाता। फिर ज़ोर-ज़ोर से किताब पढ़ने की आवाज़ आती। इजा घास की ओर जाती-जाती बीच आँगन में रुक गई। कुछ देर देखती रही। फिर मुँह बिचकाकर चली गई। कुन्ती दो कदम दूर आकर खड़ी हो गई और मेरे बालों पर फिसलते साबुन को, उससे बनते सफेद झाग को और धूप में चमकते कई रंगों के बुलबुलों को एकटक देखती रही। “भाग-भाग,” मैं चिल्लाया।
कुन्ती चिरौरी करने लगी, “दादा मुझे भी दे दो थोड़ा-सा।”
कुन्ती को मैं अच्छी तरह जानता था, बिल्ली की तरह धूर्त। उसे भगाने में ही भलाई थी। पहले तो मैंने उस पर पानी फेंका। नहीं हटी तो भीगे हाथ से दिया एक झापड़। इधर चिल्लाती हुई कुन्ती भागी, उधर सीढ़ियों पर धड़धड़ाता हुआ आया काका, “उस पर हाथ चलाया तूने? आज तेरी खैर नहीं!” पर मुँडेर से आगे नहीं बढ़ा। वहीं रुककर घूरने लगा। मैं बहुत दूर था वहाँ से। मज़े से हँसता झाग उठाता रहा। काका गालियाँ देता रहा लेकिन वहाँ से हटा भी नहीं।
बड़ी देर लगाकर पानी डाला बदन पर। साबुन को सुखाया। नामालूम-सा घिसा था। पन्नी में सम्हालकर रखा। इतराता हुआ काका के बगल से निकला। काका ने हवा को सूँघा।
कैसी तो ताज़गी आ गई थी बदन में। कैसी खुशबू! और बाल कैसे नरम! खुशबू कहीं उड़ न जाए यह सोचकर फटाफट कपड़े पहने।
अपने आँगन की मुँडेर से मैं छलाँग लगाता और कई बार ऐसा होता कि मैं उड़ने लगता। ऊँचे और ऊँचे पहाड़ों, जंगलों के ऊपर मैं कबूतरों की तरह तैरता जाता। दूर-दूर तक जाने कितने देस, कितने गाँव एक साथ मेरे नीचे सरकते जाते। बदन में सनसनी-सी होने लगती। नीचे देखता तो अपना घर छोटा-सा दिखई देता - खिलौने जैसा। और इजा, बापू, काका, कुन्ती - सारे लोग कैसे दिखाई देते, जैसे चींटी जितने हो गए हों। मैं सारी दुनिया के ऊपर तैरता। सब कुछ मेरे नीचे। कोई मुझ तक नहीं पहुँच सकता था।
यह सपनों की बात थी, कहते हैं कि बढ़वार के दिनों में बच्चों को उड़ने के सपने दिखाई देते हैं लेकिन सपने सच नहीं होते, ये किसने कहा!
साबुन से नहाकर उस दिन मुझे लगा था कि किसी भी क्षण मैं उड़ने लगूँगा।
स्कूल का दिन था। सुबह-सुबह खूब झाग उठाकर, खुद को चमकाया। महकते बदन पर सबसे अच्छे कपड़े डाले। टेढ़ी करके माँग निकाली और रास्ते भर कुहनी उठाकर सूँघता रहा कि कहीं खुशबू उड़ तो नहीं गई। नहीं, खुशबू उड़ती नहीं थी। घण्टों आती रहती। अगर धूप नहीं होती, पसीना नहीं होता, धूल नहीं उड़ती और हवा नहीं चलती तो शायद बदन हमेशा महकता रहता।
क्लास में तो सनसनी ही फैल गई। थोड़ी ही देर में सब लड़के नाक उठाए बौराये-से हवा को सूँघ रहे थे। मैं कुछ देर मन्द मुस्कुराता इसका आनन्द लेता रहा, फिर पास वाले लड़के के मुँह पर अपनी बाँह अड़ा दी।
“ओ बबा हो। क्या लगा के आया है?” लड़का तो उछल ही पड़ा। क्लास में ऐसी रेलपेल मची कि तौबा। लड़के एक-दूसरे को धकियाते लपके और जहाँ-तहाँ नाक गड़ाकर लगे सूँघने। जो सूँघ चुके वे आँखें कपाल पर चढ़ाकर कहने लगे, “बता तो, बता दो।”
और जब मैंने मज़े ले-लेकर सारी कहानी सुनाई तो क्लास में शोर मच गया, “सच? कैसा है? साथ में पन्नी भी है? एक दिन तो खत्म हो जाएगा, फिर? फिर क्या, और दौड़ेगा तो नया जीत लाएगा। एक साल तो चलेगा ही। दिखा यार, दिखा ना।”
मास्साब आए तो हंगामा था। लेकिन किसी का ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं था। सब कनखियों से मुझे देख रहे थे। मैं तो आकाश में खूब ऊँचा उड़ रहा था। उस पल अगर मैं कह देता कि आज से मॉनीटर मैं हुआ तो वे सब कहते, “हाँ हुआ।” उन्होंने अपने बाप-दादों से इतना कुछ सुना था पिण्टी के बारे में, उसके साबुन के बारे में। आज वे सब सपने जैसी कथाएँ सच होती देख लगभग पागल-से हो उठे थे।
हाफ टाइम की घण्टी बजी। हमेशा की तरह भाग पड़ने को लड़के उठे। अचानक सब-के-सब ठिठक गए। मैं वहीं बैठा जो था, अपनी जगह। “चल रे चल।” आज सब मेरे करीब आना चाहते थे। वे भी जो मेरे दुश्मन थे और मेरे दुबले-पतलेपन की वजह से मुझे पीटा करते थे।
मैं उठा तो, लेकिन एक अनजानी झिझक ने मुझे घेर लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पहले तो सबसे पहले भाग छूटने वालों में मैं अव्वल रहता था। लेकिन पहले कभी सारे लड़कों ने मुझे घेरकर ऐसे ‘चल-चल’ भी नहीं कहा था।
“तू हमारी तरफ हुआ।” “नहीं हमारी तरफ।” कबड्डी में मैं किस टीम के साथ खेलूँ इसे लेकर भारी झगड़ा चल पड़ा था।
मैं तो संकोच से मरा जा रहा था। कबड्डी में रगेदे जाने का, मिट्टी में लिपटने का डर मुझ पर हावी हो गया। “नहीं, मेरा मन नहीं है खेलने का।” मैंने कहा। “क्यों? क्यों?” हर तरफ से पुकार मच गई। फिर अपने आप जैसे सब लड़के समझ गए, “अच्छा, तू रेफरी हुआ। तू बैठकर देख।” वे एक-एक कर खिसकने लगे। खिसियाए हुए।
“क्यों? क्यों?” हर तरफ से पुकार मच गई। फिर अपने आप जैसे सब लड़के समझ गए, “अच्छा, तू रेफरी हुआ। तू बैठकर देख।” वे एक-एक कर खिसकने लगे। खिसियाए हुए।
हर कोई साबुन देखने को बेकल था। सारे गाँव में जंगल की आग की तरह यह बात फैल गई थी। लोग मुझे रोक लेते। कोई बहाना खोजकर घर चले आते। वे चाहते कि मैं उनको साबुन दिखा दूँ। जब मैं इन्कार कर देता तो वे नाराज़ हो जाते। डाँट-डपट करते। अलबत्ता वे मुझे सूँघ ज़रूर लेते। साबुन न दिखाने की मेरी इस ज़िद से घर वालों को शर्मिन्दगी का सामना करना पड़ता होगा। बाद में मुझे अपनी गालियों का निशाना बनाते। काका जब भी सामने आता, धमकी भरे इशारे करता। दो-एक बार तो उसने अकेले में मेरा गला भी दबाया। कुन्ती हमेशा मुँह फुलाए रहती। उससे मेरी झड़प हो जाए तो बापू मुझे अपने ढाई किलो के हाथ से झापड़ मारने में ज़रा भी देर नहीं करते। इजा मुझसे हमेशा चिड़चिड़ाते हुए बात करती।
सारी दुनिया गिद्धों की तरह मेरे उस छोटे-से सुख को नोचने के लिए बेताब थी। मैंने देखा कि पहले तो लोग मेरी इज़्ज़त करने लगते, लेकिन जब मैं उनको साबुन नहीं दिखाता तो वे फौरन मेरे खिलाफ लामबन्दी कर लेते। लगभग सभी मेरे दुश्मन हो चुके थे।
लोगों ने मेरा नाम ही पिण्टी रख दिया था। यह सिर्फ मज़ाक नहीं था। इस तरह वे अपनी नफरत जता रहे होते। लड़के मुझे पिण्टी-पिण्टी कहकर पुकारते। और हैरानी की बात तो यह कि इस बात से मुझे तकलीफ होने के बावजूद मैं अक्सर उस पिण्टी के बारे में सोचने लगा था। मैं अक्सर सोचता था कि वह कैसी और कहाँ होगी। मैंने मन में उसका एक खाका भी खींच लिया था, जिस पर मैं अपने खाली वक्त में रंग भरा करता था। मेरे ख्याल से वह हमारे कैलेण्डर की लक्ष्मी जैसी थी। वह इतनी गोरी थी और उसके कपड़े इतने चमकीले थे कि रात में भी उसके आसपास उजाला रहता था। उस पर धूल का एक कण भी नहीं बैठ सकता था। वह इतनी हल्की थी मानो उसे सफेद कोरे कागज़ से बनाया गया हो।
और खेलना तो मैंने छोड़ ही दिया था। कुछ लड़के मेरे करीब होना चाहते, लेकिन जल्दी ही धमाचौकड़ी का आकर्षण उनको खींच ले जाता। जब लड़के हुड़दंग मचा रहे होते तब मैं दीवार पर बैठा टाँगें हिलाता रहता। वे कबड्डी में एक-दूसरे को रगेदते, गीले खेतों में घुसकर ककड़ियाँ खोजते, चोरी से नींबू तोड़ लाते, नदी में नंगे होकर नहाते, पिरूल में फिसलते थे। वे हमेशा की तरह चीखते-चिल्लाते, गुत्थमगुत्था होते, कपड़े फाड़ लेते या बदन छिला लेते। मैं बैठे-बैठे उनको देखता उँगलियाँ चटखाता।
सच कहूँ तो कई बार मेरी इच्छा हुई कि मैं उनके बीच कूद पड़ूँ। लेकिन जब भी मैं ऐसा करने को हुआ जाने किस बात ने मेरे शरीर को जड़ कर दिया। तब मैंने चाहा कि कोई लड़का मुझे जबरन घसीटकर कबड्डी के मैदान में धकेल दे, लेकिन शायद यह नहीं हो सकता था। वे तो अब मुझसे खेलने को कहते भी नहीं थे। उन्होंने मान लिया था कि पिण्टी का काम बैठकर उनको देखते रहना है। वे मेरा अस्तित्व ही भूलने लगे थे।
अब फिर काका बाज़ार जा रहा था। सामान लाने के लिए थैले-झोले समेट रहा था। मुझसे रहा नहीं गया, कहा, “मैं भी चलूँगा।”
काका एकदम भड़क गया, “तू नहीं जाएगा मेरे साथ।”
“मैं जाऊँगा।”
“भाभी!” काका ने ऐलान किया, “इसी से मँगा ले अपना सामान। मैं नहीं जा रहा।”
इजा बाघिन की तरह झपटती आई। मेरा कान पकड़कर पटक दिया ज़मीन पर, “आज करती हूँ मैं इसका इलाज। ज्यों-ज्यों बढ़ रहा है, त्यों-त्यों सड़ रहा है।” मेरी पीठ पर दो लातें मारीं और घसीटती हुई ले चली बाहर। पीछे से काका उल्लास में चिल्लाया, “ज़रा अच्छे-से कर दो मरम्मत पिण्टी की।”
इजा मुझे मरे चूहे की तरह घसीटती मुँडेर पर ले गई और धकेल दिया बिच्छू के झाड़ पर-- “ओ इजा वे...।”
मोह का एक पतला-सा धागा-भर बचा था। टूट गया वह उस क्षण। हाफ टाइम में दीवार पर बैठे मेरी आँखें बार-बार भर आतीं। कूदते-फाँदते लड़के नज़र में काँपने लगते। बिच्छू के काँटों से बदन अभी भी चिलचिला रहा था। कोहनियाँ छिली हुईं, बालों में धूल। नहाया था उस सुबह भी। लेकिन बदन में कोई खुशबू बाकी नहीं।
मन खुलकर रो पड़ने को हो रहा था। जाऊँ, चला जाऊँ वहाँ से। हमेशा के लिए वहाँ, जहाँ पिण्टी रहती है। वहाँ लोग ऐसे नहीं हैं। वहाँ नफरत नहीं है। बिना बात के ऐसा ज़ुल्म नहीं है।
और मैंने फैसला किया कि एक दिन मौका मिलते ही बाज़ार भाग जाऊँगा। कहते हैं वहाँ से दूर-दूर को बस जाती हैं। किसी में बैठ जाऊँगा। फिर कभी नहीं लौटूँगा यहाँ। कभी नहीं। उस वक्त से यह इरादा मेरे मन में हर पल पक्का होता गया। मैंने कपड़े चुन लिए जो साथ ले जाने थे। एक झोला भी उनके लिए छिपा लिया। कुछ अखरोट भी रख लिए और देख लिया कि रुपए कहाँ से निकाले जा सकते हैं। मुझे बस मौके का इन्तज़ार था।
उस वक्त से यह इरादा मेरे मन में हर पल पक्का होता गया। मैंने कपड़े चुन लिए जो साथ ले जाने थे। एक झोला भी उनके लिए छिपा लिया। कुछ अखरोट भी रख लिए और देख लिया कि रुपए कहाँ से निकाले जा सकते हैं। मुझे बस मौके का इन्तज़ार था।
और ऐसे में वह काण्ड हो गया। मैं नहा रहा था। कैसी भी ठण्ड हो मैं नहाए बिना नहीं रहता। मुझे मालूम नहीं था कि काका घात में है। मैंने साबुन अलग रखा कि वह बिल्ली की तरह झपटा। मैं सकते में। काका का हाथ साबुन पर पड़ा। उठा भी लेता कि साबुन फिसलकर दूर जा गिरा और तब तक मैंने आँख भींचकर पीतल का भारी लोटा खींचकर दे मारा।
काका ‘हाय’ कहता चकराकर बैठ गया और सिर पकड़े वैसे ही रह गया।
तब तक मैंने साबुन उठा लिया और लोटा पकड़कर फिर से तैयार हो गया। पर काका तो उठा ही नहीं। तब मेरी टाँगें काँपने लगीं। काका को हिलाकर पुकारा, “काका, काका!”
कराहकर काका ने सिर उठाया तो देखा माथे से एकदम लाल-लाल खून बह रहा था। “मार दी साले!” काका जाने क्या-क्या बड़बड़ाने लगा। फिर हाथों से माथा दबाए लड़खड़ाता हुआ बाहर को चला। देहरी के पास रुककर मुड़ा। रुआँसा चेहरा। गालों पर खून और आँसुओं के धारे। सिसकता हुआ बोला, “साले एक दिन तो खत्म हो जाएगा तेरा साबण।”
काका चला गया। मैं सन्न खड़ा था। हथेली खोलकर देखा। गुलाबी खूबसूरत टिकिया। पर अब कितनी पतली लग रही थी। और खुशबू भी तो शायद उड़ चली थी।
मेरा मन डूबा गया।
रोने का वक्त नहीं था। फटाफट कपड़े पहन भागता हुआ गया ऊपर। झोला निकाला। कुछ कपड़े ठूँसे। अखरोट रखने का वक्त नहीं। बस्ता? नहीं बस्ते का क्या काम? पैसे?
तभी सुना, बाहर काका घबराई हुई इजा को बता रहा था कि कैसे वह गोबर पर फिसलकर गिर पड़ा और कैसे गोशाले की देहरी से उसका सिर टकराया।
मुझसे फिर खड़ा नहीं रहा गया था। औंधे मुँह चारपाई पर गिर पड़ा। बड़ी देर बाद इस काबिल हुआ कि जाकर साबुन को उसी जगह छिपा आऊँ। लौटकर एक अँधेरे कोने में सो रहा। शाम हो गई तो भी नहीं उठा। कहा कि पेट में दर्द है।
सुबह उठा तो देखा अजीब-सा उजाला सब ओर फैला था। रातोंरात बर्फ गिर गई थी। पता ही नहीं चला। आशंका में मेरा दिल बैठ गया।
ताज़ी बर्फ पर नंगे पाँव भागता गया। ठण्ड की परवाह किसे थी। पुआल के ढेर पर चार-चार अंगुल बर्फ जमी थी। यहीं कहीं थी वह सेंध। हाथों से बर्फ खोदी तो नीचे कीचड़ ही कीचड़। हाथ सन गए। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं? यहाँ भी नहीं!
कोई लिसलिसी-सी चीज़ उँगलियों में आई। गुलाबी कीचड़ का एक लौंदा। खुशबूदार। उस लौंदे को हथेली में भरे मैं वहीं बर्फ पर धप से बैठ गया। शीत से काँपता हुआ।
“हरिया!” यह इजा थी। दूध लगाने आई थी। मैंने सिर उठाकर देखा। उसी उपहास के लिए सिकुड़ते हुए उसके होंठ। मेरे हाथ से लौंदा गिर गया। माँ के होंठों से एक सिसकी-सी निकली, “हरिया...।”
पाँवों से सिर तक एक थरथराहट के साथ मैं बिखर गया। पूरे प्राण से अपने को फूट पड़ने की छूट देता हुआ, कीचड़ सनी उँगलियों से माँ को जकड़ता हुआ ज़ोर से रो पड़ा।
माँ भी वहीं मेरे पास बैठ गई। मुझे कौली में भरकर। और मैं कोख की गरमाहट में मुँह छिपाकर रोता रहा। बहुत दिनों बाद। पहले की तरह।
और सहसा मुझे लगा बर्फ का एक विशाल ढेर पिघल रहा है। मेरा मन रूई की तरह हल्का और हल्का होने लगा। उस क्षण हवा का कोई झोंका आता तो मैं सचमुच ही उड़ने लगा होता।
संजय खाती: पेशे से पत्रकार हैं। दो कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। पिण्टी का साबुन कहानी संग्रह की कई कहानियों का अनुवाद अलग-अलग भाषाओं में हो चुका है।दिल्ली में निवास।
सभी चित्र: कनक शशि: एकलव्य प्रकाशन मेें डिज़ाइनिंग व विज़्युलाइज़ेशन का काम करती हैं।


